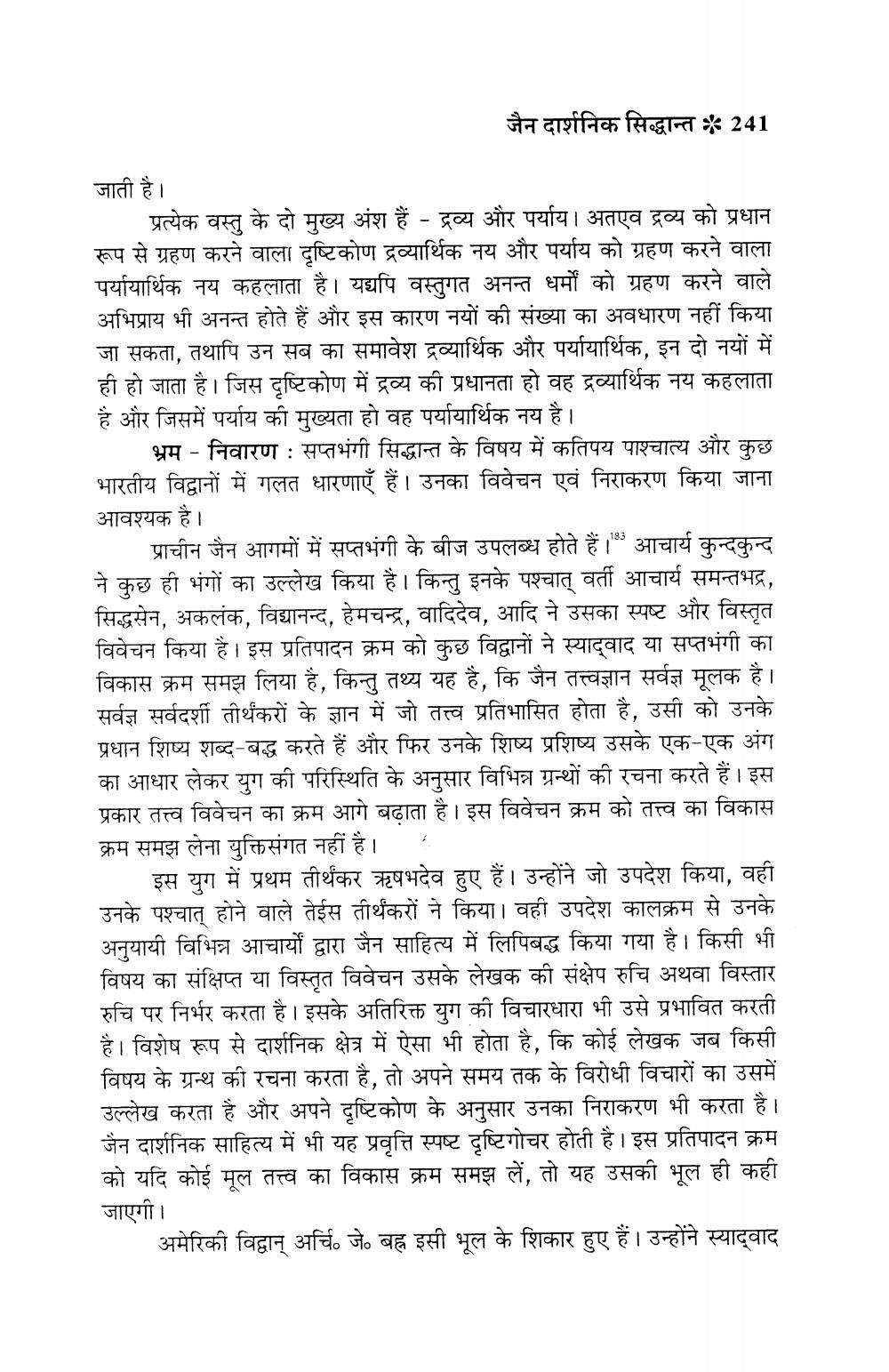________________
जैन दार्शनिक सिद्धान्त * 241
जाती है।
प्रत्येक वस्तु के दो मुख्य अंश हैं - द्रव्य और पर्याय। अतएव द्रव्य को प्रधान रूप से ग्रहण करने वाला दृष्टिकोण द्रव्यार्थिक नय और पर्याय को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिक नय कहलाता है। यद्यपि वस्तुगत अनन्त धर्मों को ग्रहण करने वाले अभिप्राय भी अनन्त होते हैं और इस कारण नयों की संख्या का अवधारण नहीं किया जा सकता, तथापि उन सब का समावेश द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दो नयों में ही हो जाता है। जिस दृष्टिकोण में द्रव्य की प्रधानता हो वह द्रव्यार्थिक नय कहलाता है और जिसमें पर्याय की मुख्यता हो वह पर्यायार्थिक नय है।
भ्रम - निवारण : सप्तभंगी सिद्धान्त के विषय में कतिपय पाश्चात्य और कुछ भारतीय विद्वानों में गलत धारणाएँ हैं। उनका विवेचन एवं निराकरण किया जाना आवश्यक है।
प्राचीन जैन आगमों में सप्तभंगी के बीज उपलब्ध होते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने कुछ ही भंगों का उल्लेख किया है। किन्तु इनके पश्चात् वर्ती आचार्य समन्तभद्र, सिद्धसेन, अकलंक, विद्यानन्द, हेमचन्द्र, वादिदेव, आदि ने उसका स्पष्ट और विस्तृत विवेचन किया है। इस प्रतिपादन क्रम को कुछ विद्वानों ने स्यावाद या सप्तभंगी का विकास क्रम समझ लिया है, किन्तु तथ्य यह है, कि जैन तत्त्वज्ञान सर्वज्ञ मूलक है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकरों के ज्ञान में जो तत्त्व प्रतिभासित होता है, उसी को उनके प्रधान शिष्य शब्द-बद्ध करते हैं और फिर उनके शिष्य प्रशिष्य उसके एक-एक अंग का आधार लेकर युग की परिस्थिति के अनुसार विभिन्न ग्रन्थों की रचना करते हैं। इस प्रकार तत्त्व विवेचन का क्रम आगे बढ़ाता है। इस विवेचन क्रम को तत्त्व का विकास क्रम समझ लेना युक्तिसंगत नहीं है।
इस युग में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए हैं। उन्होंने जो उपदेश किया, वही उनके पश्चात् होने वाले तेईस तीर्थंकरों ने किया। वही उपदेश कालक्रम से उनके अनुयायी विभिन्न आचार्यों द्वारा जैन साहित्य में लिपिबद्ध किया गया है। किसी भी विषय का संक्षिप्त या विस्तृत विवेचन उसके लेखक की संक्षेप रुचि अथवा विस्तार रुचि पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त युग की विचारधारा भी उसे प्रभावित करती है। विशेष रूप से दार्शनिक क्षेत्र में ऐसा भी होता है, कि कोई लेखक जब किसी विषय के ग्रन्थ की रचना करता है, तो अपने समय तक के विरोधी विचारों का उसमें उल्लेख करता है और अपने दृष्टिकोण के अनुसार उनका निराकरण भी करता है। जैन दार्शनिक साहित्य में भी यह प्रवृत्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस प्रतिपादन क्रम को यदि कोई मूल तत्त्व का विकास क्रम समझ लें, तो यह उसकी भूल ही कही जाएगी।
अमेरिकी विद्वान् अर्चि. जे. बह्न इसी भूल के शिकार हुए हैं। उन्होंने स्याद्वाद