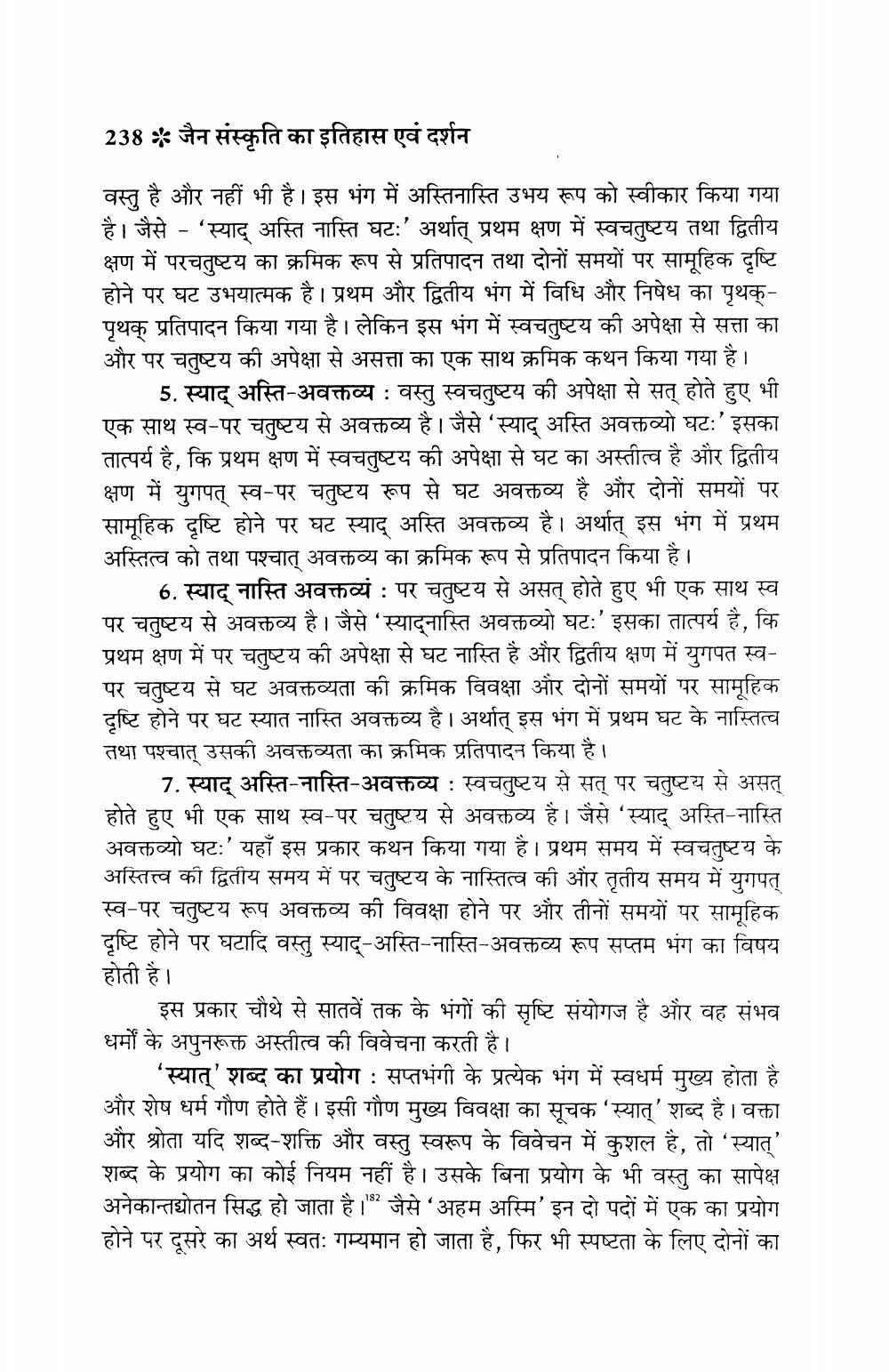________________
238 जैन संस्कृति का इतिहास एवं दर्शन
वस्तु है और नहीं भी है । इस भंग में अस्तिनास्ति उभय रूप को स्वीकार किया गया है । जैसे - 'स्याद् अस्ति नास्ति घटः' अर्थात् प्रथम क्षण में स्वचतुष्टय तथा द्वितीय क्षण में परचतुष्टय का क्रमिक रूप से प्रतिपादन तथा दोनों समयों पर सामूहिक दृष्टि होने पर घट उभयात्मक है। प्रथम और द्वितीय भंग में विधि और निषेध का पृथक्पृथक् प्रतिपादन किया गया है। लेकिन इस भंग में स्वचतुष्टय की अपेक्षा से सत्ता का और पर चतुष्टय की अपेक्षा से असत्ता का एक साथ क्रमिक कथन किया गया है। 5. स्याद् अस्ति - 3 - अवक्तव्य : वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा से सत् होते हुए भी एक साथ स्व-पर चतुष्टय से अवक्तव्य है । जैसे 'स्याद् अस्ति अवक्तव्यो घट:' इसका तात्पर्य है, कि प्रथम क्षण में स्वचतुष्टय की अपेक्षा से घट का अस्तीत्व है और द्वितीय क्षण में युगपत् स्व- पर चतुष्टय रूप से घट अवक्तव्य है और दोनों समयों पर सामूहिक दृष्टि होने पर घट स्याद् अस्ति अवक्तव्य है । अर्थात् इस भंग में प्रथम अस्तित्व को तथा पश्चात् अवक्तव्य का क्रमिक रूप से प्रतिपादन किया है।
6. स्याद् नास्ति अवक्तव्यं : पर चतुष्टय से असत् होते हुए भी एक साथ स्व पर चतुष्टय से अवक्तव्य है । जैसे 'स्याद्नास्ति अवक्तव्यो घट:' इसका तात्पर्य है, कि प्रथम क्षण में पर चतुष्टय की अपेक्षा से घट नास्ति है और द्वितीय क्षण में युगपत स्वपर चतुष्टय से घट अवक्तव्यता की क्रमिक विवक्षा और दोनों समयों पर सामूहिक दृष्टि होने पर घट स्यात नास्ति अवक्तव्य है । अर्थात् इस भंग में प्रथम घट के नास्तित्व तथा पश्चात् उसकी अवक्तव्यता का क्रमिक प्रतिपादन किया है।
7. स्याद् अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य : स्वचतुष्टय से सत् पर चतुष्टय से असत् होते हुए भी एक साथ स्व- पर चतुष्टय से अवक्तव्य है । जैसे 'स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्यो घटः' यहाँ इस प्रकार कथन किया गया है। प्रथम समय में स्वचतुष्टय के अस्तित्त्व की द्वितीय समय में पर चतुष्टय के नास्तित्व की और तृतीय समय में युगपत् स्व-पर चतुष्टय रूप अवक्तव्य की विवक्षा होने पर और तीनों समयों पर सामूहिक दृष्टि होने पर घटादि वस्तु स्याद् - अस्ति नास्ति - अवक्तव्य रूप सप्तम भंग का विषय होती हैं।
इस प्रकार चौथे से सातवें तक के भंगों की सृष्टि संयोगज है और वह संभव धर्मों के अपुनरूक्त अस्तीत्व की विवेचना करती है ।
'स्यात्' शब्द का प्रयोग : सप्तभंगी के प्रत्येक भंग में स्वधर्म मुख्य होता है और शेष धर्म गौण होते हैं । इसी गौण मुख्य विवक्षा का सूचक 'स्यात्' शब्द है। वक्ता और श्रोता यदि शब्द-शक्ति और वस्तु स्वरूप के विवेचन में कुशल है, तो 'स्यात् ' शब्द के प्रयोग का कोई नियम नहीं है। उसके बिना प्रयोग के भी वस्तु का सापेक्ष अनेकान्तद्योतन सिद्ध हो जाता है। जैसे 'अहम अस्मि' इन दो पदों में एक का प्रयोग होने पर दूसरे का अर्थ स्वतः गम्यमान हो जाता है, फिर भी स्पष्टता के लिए दोनों का
182