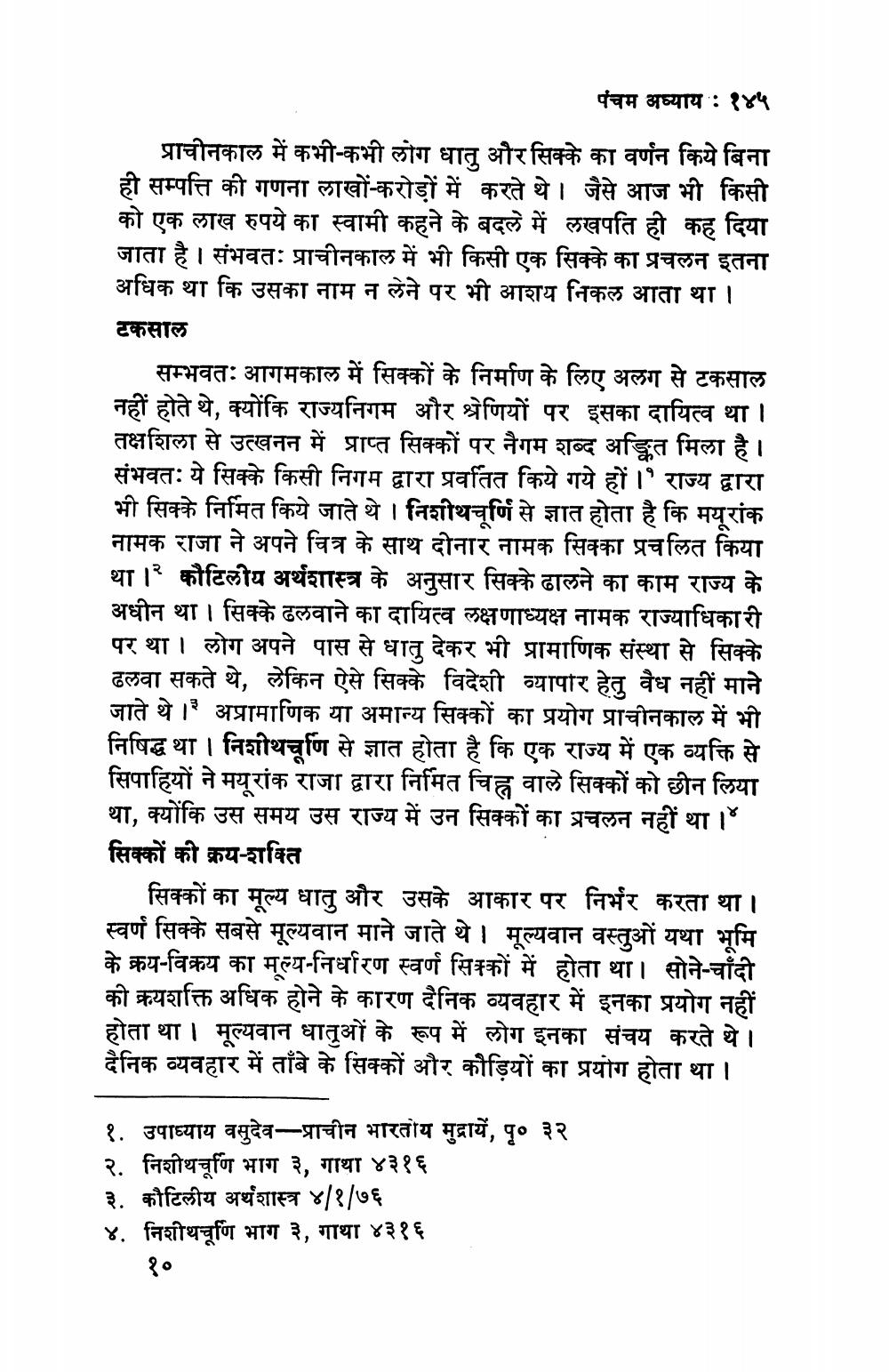________________
पंचम अध्याय : १४५ प्राचीनकाल में कभी-कभी लोग धातु और सिक्के का वर्णन किये बिना ही सम्पत्ति की गणना लाखों-करोड़ों में करते थे। जैसे आज भी किसी को एक लाख रुपये का स्वामी कहने के बदले में लखपति ही कह दिया जाता है। संभवतः प्राचीनकाल में भी किसी एक सिक्के का प्रचलन इतना अधिक था कि उसका नाम न लेने पर भी आशय निकल आता था । टकसाल
सम्भवतः आगमकाल में सिक्कों के निर्माण के लिए अलग से टकसाल नहीं होते थे, क्योंकि राज्यनिगम और श्रेणियों पर इसका दायित्व था। तक्षशिला से उत्खनन में प्राप्त सिक्कों पर नैगम शब्द अङ्कित मिला है। संभवतः ये सिक्के किसी निगम द्वारा प्रवर्तित किये गये हों।' राज्य द्वारा भी सिक्के निर्मित किये जाते थे । निशीथचूर्णि से ज्ञात होता है कि मयूरांक नामक राजा ने अपने चित्र के साथ दीनार नामक सिक्का प्रचलित किया था। कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का काम राज्य के अधीन था। सिक्के ढलवाने का दायित्व लक्षणाध्यक्ष नामक राज्याधिकारी पर था। लोग अपने पास से धातु देकर भी प्रामाणिक संस्था से सिक्के ढलवा सकते थे, लेकिन ऐसे सिक्के विदेशी व्यापार हेतु वैध नहीं माने जाते थे। अप्रामाणिक या अमान्य सिक्कों का प्रयोग प्राचीनकाल में भी निषिद्ध था । निशीथणि से ज्ञात होता है कि एक राज्य में एक व्यक्ति से सिपाहियों ने मयूरांक राजा द्वारा निर्मित चिह्न वाले सिक्कों को छीन लिया था, क्योंकि उस समय उस राज्य में उन सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिक्कों की क्रय-शक्ति
सिक्कों का मूल्य धातु और उसके आकार पर निर्भर करता था। स्वर्ण सिक्के सबसे मूल्यवान माने जाते थे। मूल्यवान वस्तुओं यथा भूमि के क्रय-विक्रय का मूल्य-निर्धारण स्वर्ण सिक्कों में होता था। सोने-चाँदी की क्रयशक्ति अधिक होने के कारण दैनिक व्यवहार में इनका प्रयोग नहीं होता था। मूल्यवान धातुओं के रूप में लोग इनका संचय करते थे। दैनिक व्यवहार में ताँबे के सिक्कों और कौड़ियों का प्रयोग होता था ।
१. उपाध्याय वसुदेव-प्राचीन भारतीय मुद्रायें, पृ० ३२ २. निशीथचूणि भाग ३, गाथा ४३१६ ३. कौटिलीय अर्थशास्त्र ४/१/७६ ४. निशीथचूणि भाग ३, गाथा ४३१६