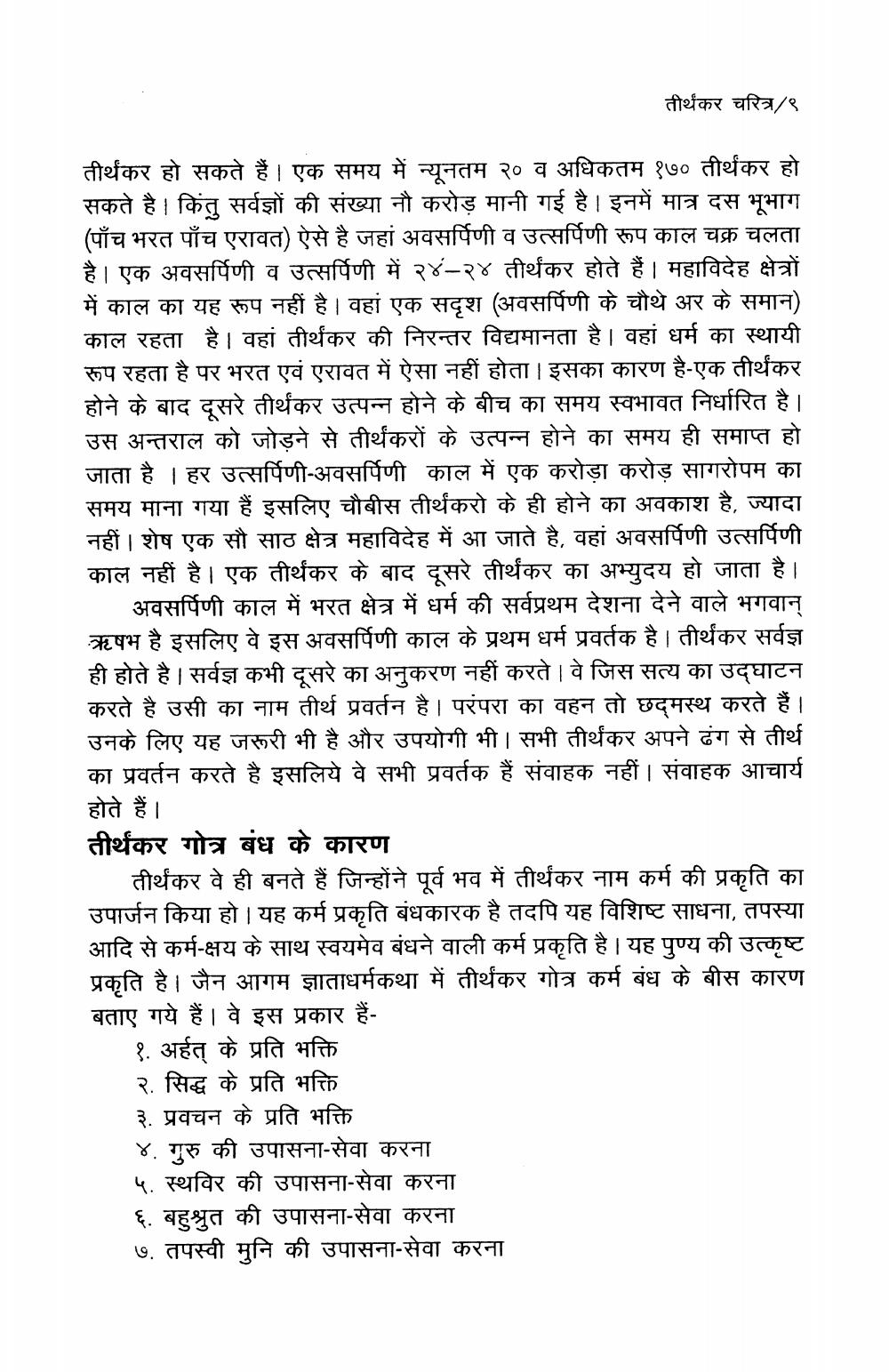________________
तीर्थंकर चरित्र/९
तीर्थंकर हो सकते हैं। एक समय में न्यूनतम २० व अधिकतम १७० तीर्थंकर हो सकते है। किंतु सर्वज्ञों की संख्या नौ करोड़ मानी गई है। इनमें मात्र दस भूभाग (पाँच भरत पाँच एरावत) ऐसे है जहां अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी रूप काल चक्र चलता है। एक अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी में २४-२४ तीर्थंकर होते हैं। महाविदेह क्षेत्रों में काल का यह रूप नहीं है। वहां एक सदृश (अवसर्पिणी के चौथे अर के समान) काल रहता है। वहां तीर्थंकर की निरन्तर विद्यमानता है। वहां धर्म का स्थायी रूप रहता है पर भरत एवं एरावत में ऐसा नहीं होता। इसका कारण है-एक तीर्थंकर होने के बाद दूसरे तीर्थंकर उत्पन्न होने के बीच का समय स्वभावत निर्धारित है। उस अन्तराल को जोड़ने से तीर्थंकरों के उत्पन्न होने का समय ही समाप्त हो जाता है । हर उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल में एक करोड़ा करोड़ सागरोपम का समय माना गया हैं इसलिए चौबीस तीर्थंकरो के ही होने का अवकाश है, ज्यादा नहीं। शेष एक सौ साठ क्षेत्र महाविदेह में आ जाते है, वहां अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल नहीं है। एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर का अभ्युदय हो जाता है। ___ अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में धर्म की सर्वप्रथम देशना देने वाले भगवान् ऋषभ है इसलिए वे इस अवसर्पिणी काल के प्रथम धर्म प्रवर्तक है। तीर्थंकर सर्वज्ञ ही होते है। सर्वज्ञ कभी दूसरे का अनुकरण नहीं करते। वे जिस सत्य का उद्घाटन करते है उसी का नाम तीर्थ प्रवर्तन है। परंपरा का वहन तो छद्मस्थ करते हैं। उनके लिए यह जरूरी भी है और उपयोगी भी। सभी तीर्थंकर अपने ढंग से तीर्थ का प्रवर्तन करते है इसलिये वे सभी प्रवर्तक हैं संवाहक नहीं। संवाहक आचार्य होते हैं। तीर्थंकर गोत्र बंध के कारण
तीर्थंकर वे ही बनते हैं जिन्होंने पूर्व भव में तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उपार्जन किया हो। यह कर्म प्रकृति बंधकारक है तदपि यह विशिष्ट साधना, तपस्या आदि से कर्म-क्षय के साथ स्वयमेव बंधने वाली कर्म प्रकृति है। यह पुण्य की उत्कृष्ट प्रकृति है। जैन आगम ज्ञाताधर्मकथा में तीर्थंकर गोत्र कर्म बंध के बीस कारण बताए गये हैं। वे इस प्रकार हैं
१. अर्हत् के प्रति भक्ति २. सिद्ध के प्रति भक्ति ३. प्रवचन के प्रति भक्ति ४. गुरु की उपासना-सेवा करना ५. स्थविर की उपासना-सेवा करना ६. बहुश्रुत की उपासना-सेवा करना ७. तपस्वी मुनि की उपासना-सेवा करना