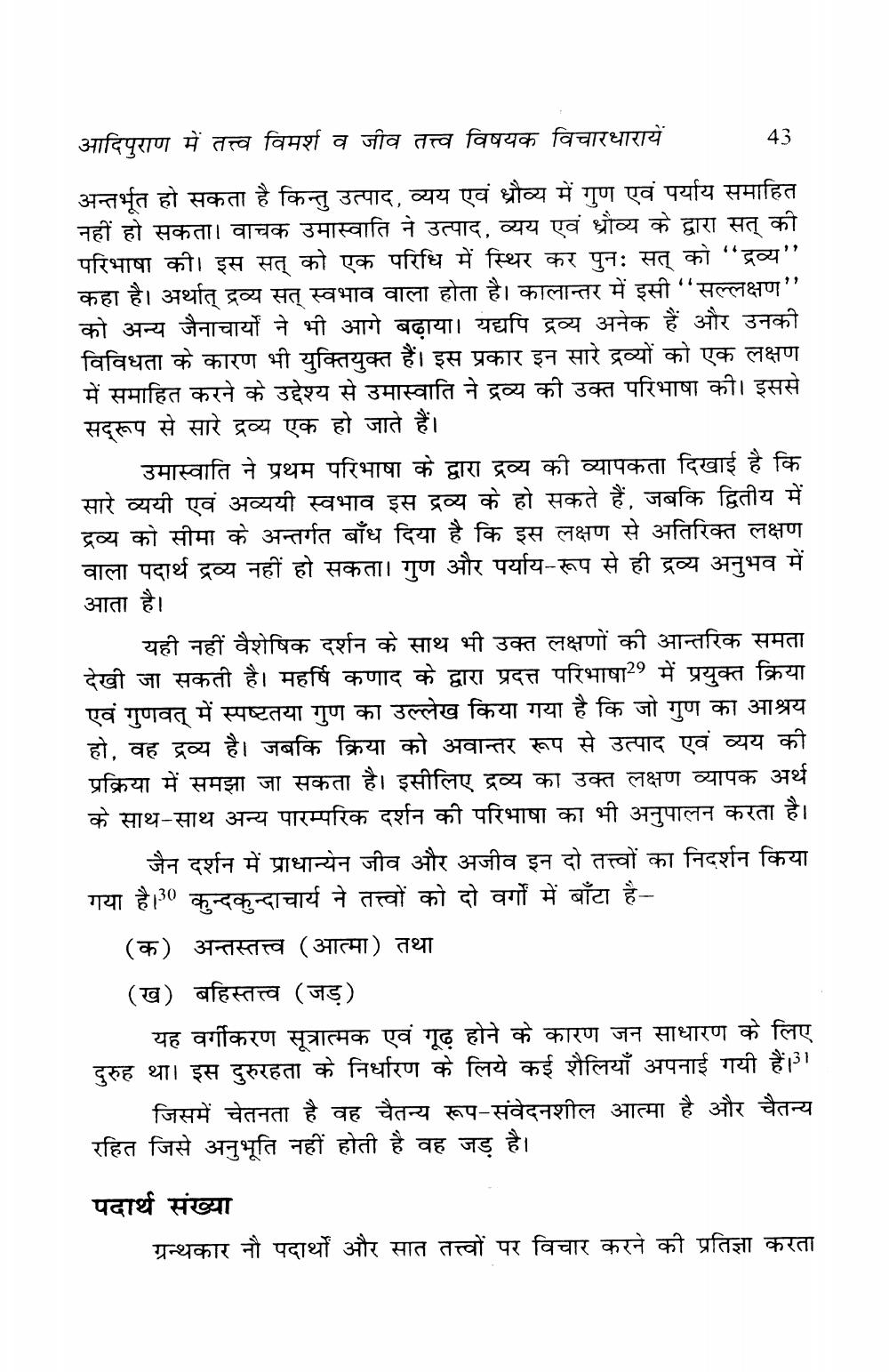________________
43
आदिपुराण में तत्त्व विमर्श व जीव तत्त्व विषयक विचारधारायें
""
अन्तर्भूत हो सकता है किन्तु उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्य में गुण एवं पर्याय समाहित नहीं हो सकता। वाचक उमास्वाति ने उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्य के द्वारा सत् की परिभाषा की। इस सत् को एक परिधि में स्थिर कर पुनः सत् को " द्रव्य " कहा है। अर्थात् द्रव्य सत् स्वभाव वाला होता है। कालान्तर में इसी " सल्लक्षण' को अन्य जैनाचार्यों ने भी आगे बढ़ाया। यद्यपि द्रव्य अनेक हैं और उनकी विविधता के कारण भी युक्तियुक्त हैं। इस प्रकार इन सारे द्रव्यों को एक लक्षण में समाहित करने के उद्देश्य से उमास्वाति ने द्रव्य की उक्त परिभाषा की। इससे सद्रूप से सारे द्रव्य एक हो जाते हैं।
उमास्वाति ने प्रथम परिभाषा के द्वारा द्रव्य की व्यापकता दिखाई है कि सारे व्ययी एवं अव्ययी स्वभाव इस द्रव्य के हो सकते हैं, जबकि द्वितीय में द्रव्य को सीमा के अन्तर्गत बाँध दिया है कि इस लक्षण से अतिरिक्त लक्षण वाला पदार्थ द्रव्य नहीं हो सकता। गुण और पर्याय- रूप से ही द्रव्य अनुभव में आता है।
यही नहीं वैशेषिक दर्शन के साथ भी उक्त लक्षणों की आन्तरिक समता देखी जा सकती है। महर्षि कणाद के द्वारा प्रदत्त परिभाषा 29 में प्रयुक्त क्रिया एवं गुणवत् में स्पष्टतया गुण का उल्लेख किया गया है कि जो गुण का आश्रय हो, वह द्रव्य है। जबकि क्रिया को अवान्तर रूप से उत्पाद एवं व्यय की प्रक्रिया में समझा जा सकता है। इसीलिए द्रव्य का उक्त लक्षण व्यापक अर्थ के साथ-साथ अन्य पारम्परिक दर्शन की परिभाषा का भी अनुपालन करता है।
जैन दर्शन में प्राधान्येन जीव और अजीव इन दो तत्त्वों का निदर्शन किया गया है।30 कुन्दकुन्दाचार्य ने तत्त्वों को दो वर्गों में बाँटा है
(क) अन्तस्तत्त्व (आत्मा) तथा
(ख) बहिस्तत्त्व (जड़)
यह वर्गीकरण सूत्रात्मक एवं गूढ़ होने के कारण जन साधारण के लिए दुरुह था । इस दुरुरहता के निर्धारण के लिये कई शैलियाँ अपनाई गयी हैं। 31
जिसमें चेतनता है वह चैतन्य रूप - संवेदनशील आत्मा है और चैतन्य रहित जिसे अनुभूति नहीं होती है वह जड़ है।
पदार्थ संख्या
ग्रन्थकार नौ पदार्थों और सात तत्त्वों पर विचार करने की प्रतिज्ञा करता