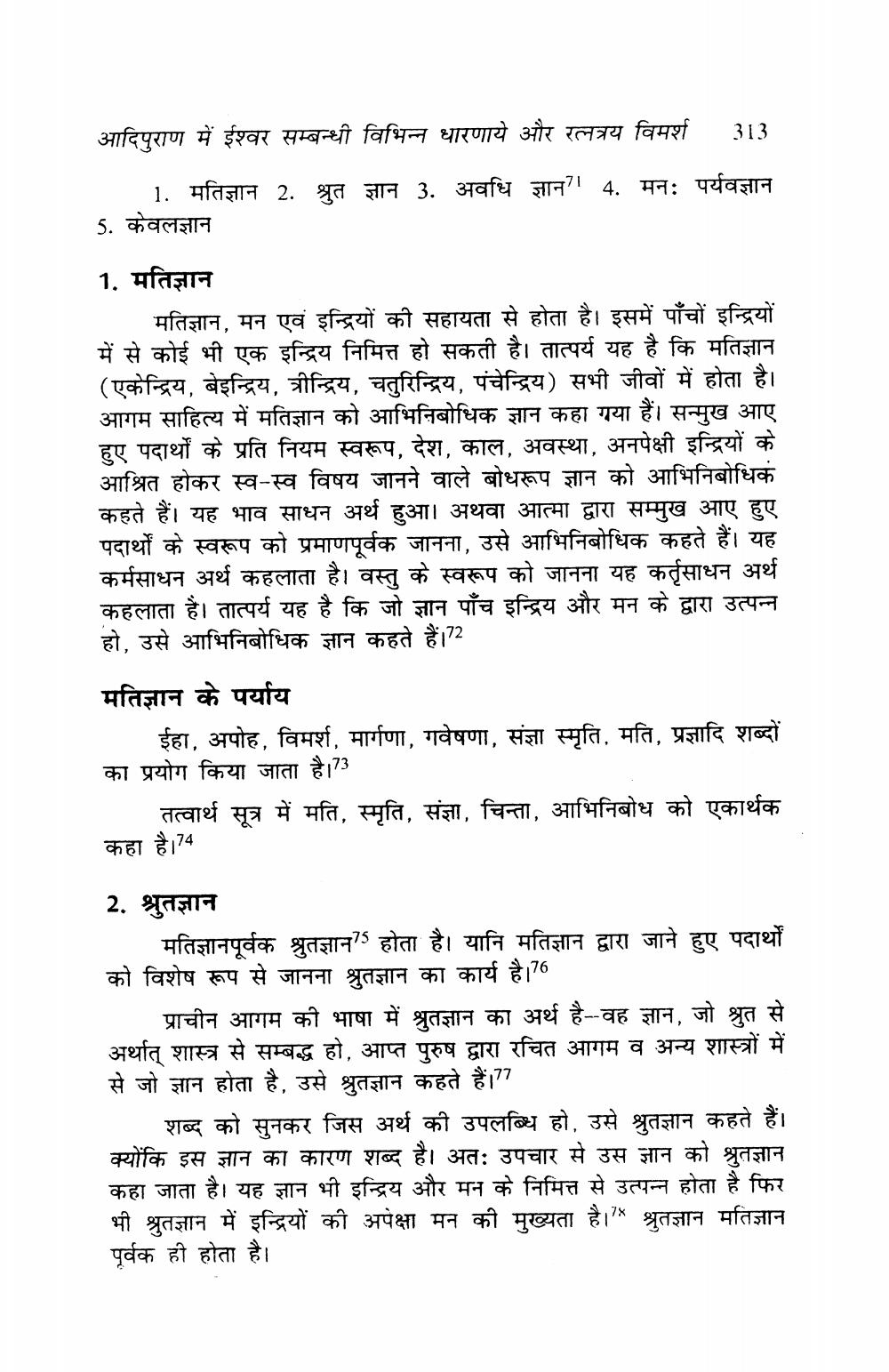________________
आदिपुराण में ईश्वर सम्बन्धी विभिन्न धारणाये और रत्नत्रय विमर्श 313
1. मतिज्ञान 2. श्रुत ज्ञान 3. अवधि ज्ञान। 4. मनः पर्यवज्ञान 5. केवलज्ञान 1. मतिज्ञान
मतिज्ञान, मन एवं इन्द्रियों की सहायता से होता है। इसमें पाँचों इन्द्रियों में से कोई भी एक इन्द्रिय निमित्त हो सकती है। तात्पर्य यह है कि मतिज्ञान (एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय) सभी जीवों में होता है। आगम साहित्य में मतिज्ञान को आभिनिबोधिक ज्ञान कहा गया हैं। सन्मुख आए हुए पदार्थों के प्रति नियम स्वरूप, देश, काल, अवस्था, अनपेक्षी इन्द्रियों के आश्रित होकर स्व-स्व विषय जानने वाले बोधरूप ज्ञान को आभिनिबोधिक कहते हैं। यह भाव साधन अर्थ हुआ। अथवा आत्मा द्वारा सम्मुख आए हुए पदार्थों के स्वरूप को प्रमाणपूर्वक जानना, उसे आभिनिबोधिक कहते हैं। यह कर्मसाधन अर्थ कहलाता है। वस्तु के स्वरूप को जानना यह कर्तृसाधन अर्थ कहलाता है। तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान पाँच इन्द्रिय और मन के द्वारा उत्पन्न हो, उसे आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं।2 मतिज्ञान के पर्याय
ईहा, अपोह, विमर्श, मार्गणा, गवेषणा, संज्ञा स्मृति, मति, प्रज्ञादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।73
तत्वार्थ सूत्र में मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, आभिनिबोध को एकार्थक कहा है।
2. श्रुतज्ञान
मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है। यानि मतिज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से जानना श्रुतज्ञान का कार्य है।76
प्राचीन आगम की भाषा में श्रुतज्ञान का अर्थ है--वह ज्ञान, जो श्रुत से अर्थात् शास्त्र से सम्बद्ध हो, आप्त पुरुष द्वारा रचित आगम व अन्य शास्त्रों में से जो ज्ञान होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं।7
__ शब्द को सुनकर जिस अर्थ की उपलब्धि हो, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। क्योंकि इस ज्ञान का कारण शब्द है। अतः उपचार से उस ज्ञान को श्रुतज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान भी इन्द्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है फिर भी श्रुतज्ञान में इन्द्रियों की अपेक्षा मन की मुख्यता है। श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक ही होता है।