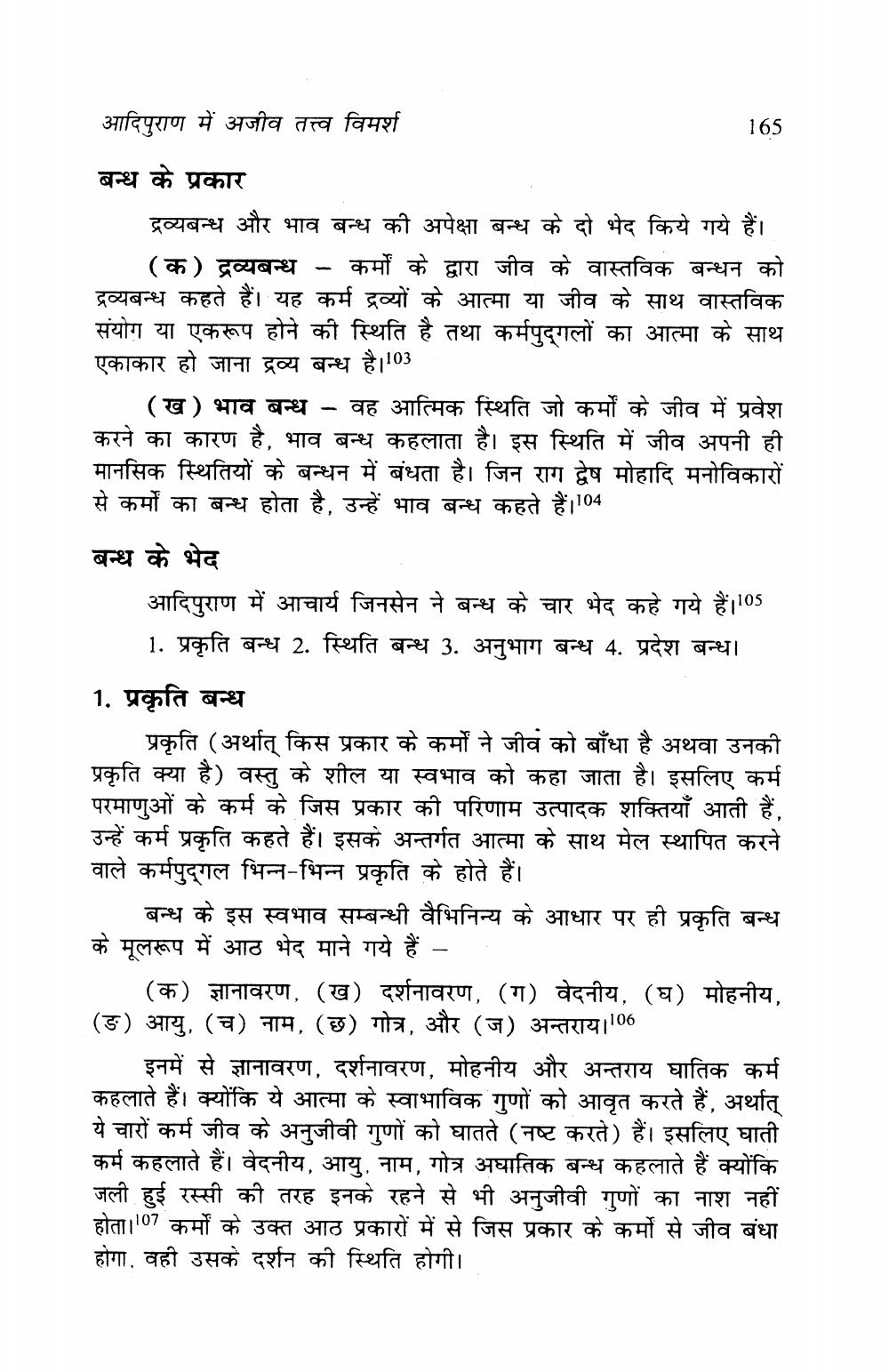________________
आदिपुराण में अजीव तत्त्व विमर्श
165
बन्ध के प्रकार
द्रव्यबन्ध और भाव बन्ध की अपेक्षा बन्ध के दो भेद किये गये हैं।
(क) द्रव्यबन्ध - कर्मों के द्वारा जीव के वास्तविक बन्धन को द्रव्यबन्ध कहते हैं। यह कर्म द्रव्यों के आत्मा या जीव के साथ वास्तविक संयोग या एकरूप होने की स्थिति है तथा कर्मपुद्गलों का आत्मा के साथ एकाकार हो जाना द्रव्य बन्ध है।103
(ख) भाव बन्ध - वह आत्मिक स्थिति जो कर्मों के जीव में प्रवेश करने का कारण है, भाव बन्ध कहलाता है। इस स्थिति में जीव अपनी ही मानसिक स्थितियों के बन्धन में बंधता है। जिन राग द्वेष मोहादि मनोविकारों से कर्मों का बन्ध होता है, उन्हें भाव बन्ध कहते हैं।104 बन्ध के भेद
आदिपुराण में आचार्य जिनसेन ने बन्ध के चार भेद कहे गये हैं।105
1. प्रकृति बन्ध 2. स्थिति बन्ध 3. अनुभाग बन्ध 4. प्रदेश बन्ध। 1. प्रकृति बन्ध
प्रकृति (अर्थात् किस प्रकार के कर्मों ने जीव को बाँधा है अथवा उनकी प्रकृति क्या है) वस्तु के शील या स्वभाव को कहा जाता है। इसलिए कर्म परमाणुओं के कर्म के जिस प्रकार की परिणाम उत्पादक शक्तियाँ आती हैं, उन्हें कर्म प्रकृति कहते हैं। इसके अन्तर्गत आत्मा के साथ मेल स्थापित करने वाले कर्मपुद्गल भिन्न-भिन्न प्रकृति के होते हैं।
बन्ध के इस स्वभाव सम्बन्धी वैभिनिन्य के आधार पर ही प्रकृति बन्ध के मूलरूप में आठ भेद माने गये हैं -
(क) ज्ञानावरण, (ख) दर्शनावरण, (ग) वेदनीय, (घ) मोहनीय, (ङ) आयु, (च) नाम, (छ) गोत्र, और (ज) अन्तराय।106
इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय घातिक कर्म कहलाते हैं। क्योंकि ये आत्मा के स्वाभाविक गुणों को आवृत करते हैं, अर्थात् ये चारों कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को घातते (नष्ट करते) हैं। इसलिए घाती कर्म कहलाते हैं। वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र अघातिक बन्ध कहलाते हैं क्योंकि जली हुई रस्सी की तरह इनके रहने से भी अनुजीवी गुणों का नाश नहीं होता।107 कर्मों के उक्त आठ प्रकारों में से जिस प्रकार के कर्मो से जीव बंधा होगा. वही उसके दर्शन की स्थिति होगी।