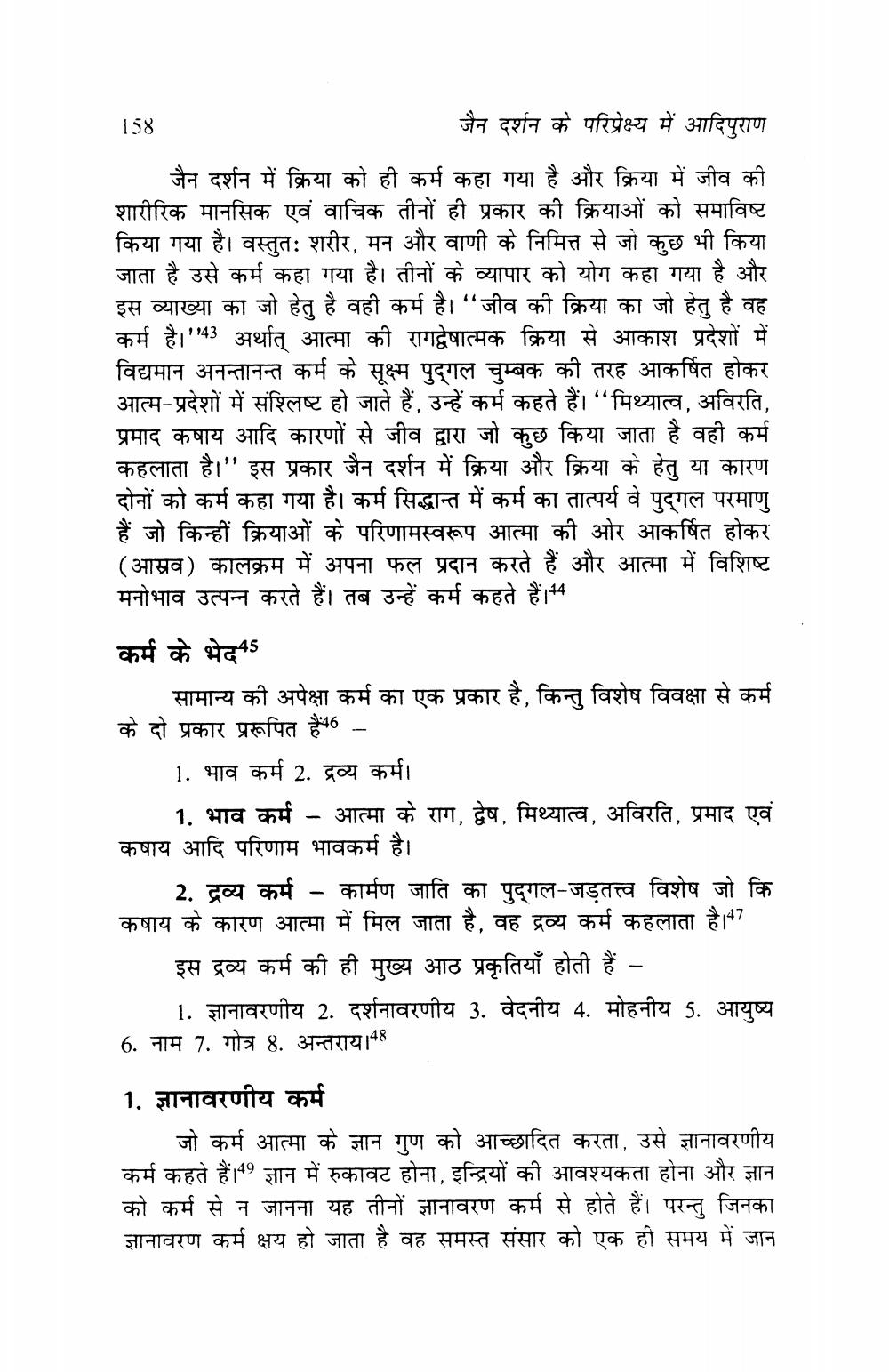________________
158
जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आदिपुराण जैन दर्शन में क्रिया को ही कर्म कहा गया है और क्रिया में जीव की शारीरिक मानसिक एवं वाचिक तीनों ही प्रकार की क्रियाओं को समाविष्ट किया गया है। वस्तुतः शरीर, मन और वाणी के निमित्त से जो कुछ भी किया जाता है उसे कर्म कहा गया है। तीनों के व्यापार को योग कहा गया है और इस व्याख्या का जो हेतु है वही कर्म है। "जीव की क्रिया का जो हेतु है वह कर्म है।''43 अर्थात् आत्मा की रागद्वेषात्मक क्रिया से आकाश प्रदेशों में विद्यमान अनन्तानन्त कर्म के सूक्ष्म पुद्गल चुम्बक की तरह आकर्षित होकर आत्म-प्रदेशों में संश्लिष्ट हो जाते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। “मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद कषाय आदि कारणों से जीव द्वारा जो कुछ किया जाता है वही कर्म कहलाता है।" इस प्रकार जैन दर्शन में क्रिया और क्रिया के हेतु या कारण दोनों को कर्म कहा गया है। कर्म सिद्धान्त में कर्म का तात्पर्य वे पुद्गल परमाणु हैं जो किन्हीं क्रियाओं के परिणामस्वरूप आत्मा की ओर आकर्षित होकर (आस्रव) कालक्रम में अपना फल प्रदान करते हैं और आत्मा में विशिष्ट मनोभाव उत्पन्न करते हैं। तब उन्हें कर्म कहते हैं।14 कर्म के भेद45 ___सामान्य की अपेक्षा कर्म का एक प्रकार है, किन्तु विशेष विवक्षा से कर्म के दो प्रकार प्ररूपित हैं16 -
1. भाव कर्म 2. द्रव्य कर्म।
1. भाव कर्म - आत्मा के राग, द्वेष, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद एवं कषाय आदि परिणाम भावकर्म है।
2. द्रव्य कर्म - कार्मण जाति का पुद्गल-जड़तत्त्व विशेष जो कि कषाय के कारण आत्मा में मिल जाता है, वह द्रव्य कर्म कहलाता है।47
इस द्रव्य कर्म की ही मुख्य आठ प्रकृतियाँ होती हैं -
1. ज्ञानावरणीय 2. दर्शनावरणीय 3. वेदनीय 4. मोहनीय 5. आयुष्य 6. नाम 7. गोत्र 8. अन्तराय।48
1. ज्ञानावरणीय कर्म
जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को आच्छादित करता, उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।49 ज्ञान में रुकावट होना, इन्द्रियों की आवश्यकता होना और ज्ञान को कर्म से न जानना यह तीनों ज्ञानावरण कर्म से होते हैं। परन्तु जिनका ज्ञानावरण कर्म क्षय हो जाता है वह समस्त संसार को एक ही समय में जान