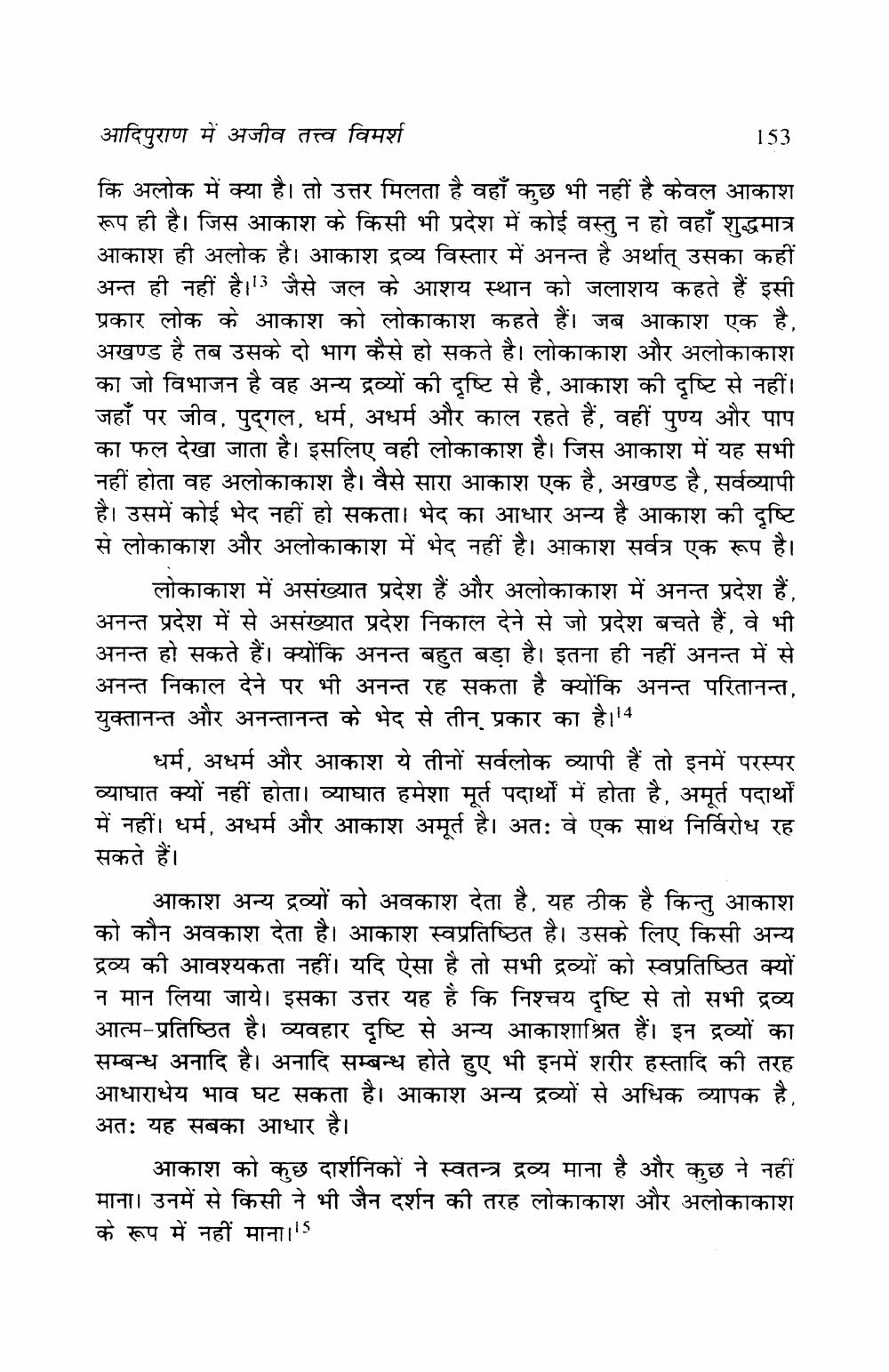________________
आदिपुराण में अजीव तत्त्व विमर्श
153
कि अलोक में क्या है। तो उत्तर मिलता है वहाँ कुछ भी नहीं है केवल आकाश रूप ही है। जिस आकाश के किसी भी प्रदेश में कोई वस्तु न हो वहाँ शुद्धमात्र आकाश ही अलोक है। आकाश द्रव्य विस्तार में अनन्त है अर्थात् उसका कहीं अन्त ही नहीं है।13 जैसे जल के आशय स्थान को जलाशय कहते हैं इसी प्रकार लोक के आकाश को लोकाकाश कहते हैं। जब आकाश एक है, अखण्ड है तब उसके दो भाग कैसे हो सकते है। लोकाकाश और अलोकाकाश का जो विभाजन है वह अन्य द्रव्यों की दृष्टि से है, आकाश की दृष्टि से नहीं। जहाँ पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल रहते हैं, वहीं पुण्य और पाप का फल देखा जाता है। इसलिए वही लोकाकाश है। जिस आकाश में यह सभी नहीं होता वह अलोकाकाश है। वैसे सारा आकाश एक है, अखण्ड है, सर्वव्यापी है। उसमें कोई भेद नहीं हो सकता। भेद का आधार अन्य है आकाश की दृष्टि से लोकाकाश और अलोकाकाश में भेद नहीं है। आकाश सर्वत्र एक रूप है।
लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं और अलोकाकाश में अनन्त प्रदेश हैं, अनन्त प्रदेश में से असंख्यात प्रदेश निकाल देने से जो प्रदेश बचते हैं, वे भी अनन्त हो सकते हैं। क्योंकि अनन्त बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं अनन्त में से अनन्त निकाल देने पर भी अनन्त रह सकता है क्योंकि अनन्त परितानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त के भेद से तीन प्रकार का है।।4
धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों सर्वलोक व्यापी हैं तो इनमें परस्पर व्याघात क्यों नहीं होता। व्याघात हमेशा मूर्त पदार्थों में होता है, अमूर्त पदार्थों में नहीं। धर्म, अधर्म और आकाश अमूर्त है। अतः वे एक साथ निर्विरोध रह सकते हैं।
आकाश अन्य द्रव्यों को अवकाश देता है, यह ठीक है किन्तु आकाश को कौन अवकाश देता है। आकाश स्वप्रतिष्ठित है। उसके लिए किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा है तो सभी द्रव्यों को स्वप्रतिष्ठित क्यों न मान लिया जाये। इसका उत्तर यह है कि निश्चय दृष्टि से तो सभी द्रव्य आत्म-प्रतिष्ठित है। व्यवहार दृष्टि से अन्य आकाशाश्रित हैं। इन द्रव्यों का सम्बन्ध अनादि है। अनादि सम्बन्ध होते हुए भी इनमें शरीर हस्तादि की तरह आधाराधेय भाव घट सकता है। आकाश अन्य द्रव्यों से अधिक व्यापक है, अतः यह सबका आधार है।
आकाश को कुछ दार्शनिकों ने स्वतन्त्र द्रव्य माना है और कुछ ने नहीं माना। उनमें से किसी ने भी जैन दर्शन की तरह लोकाकाश और अलोकाकाश के रूप में नहीं माना।