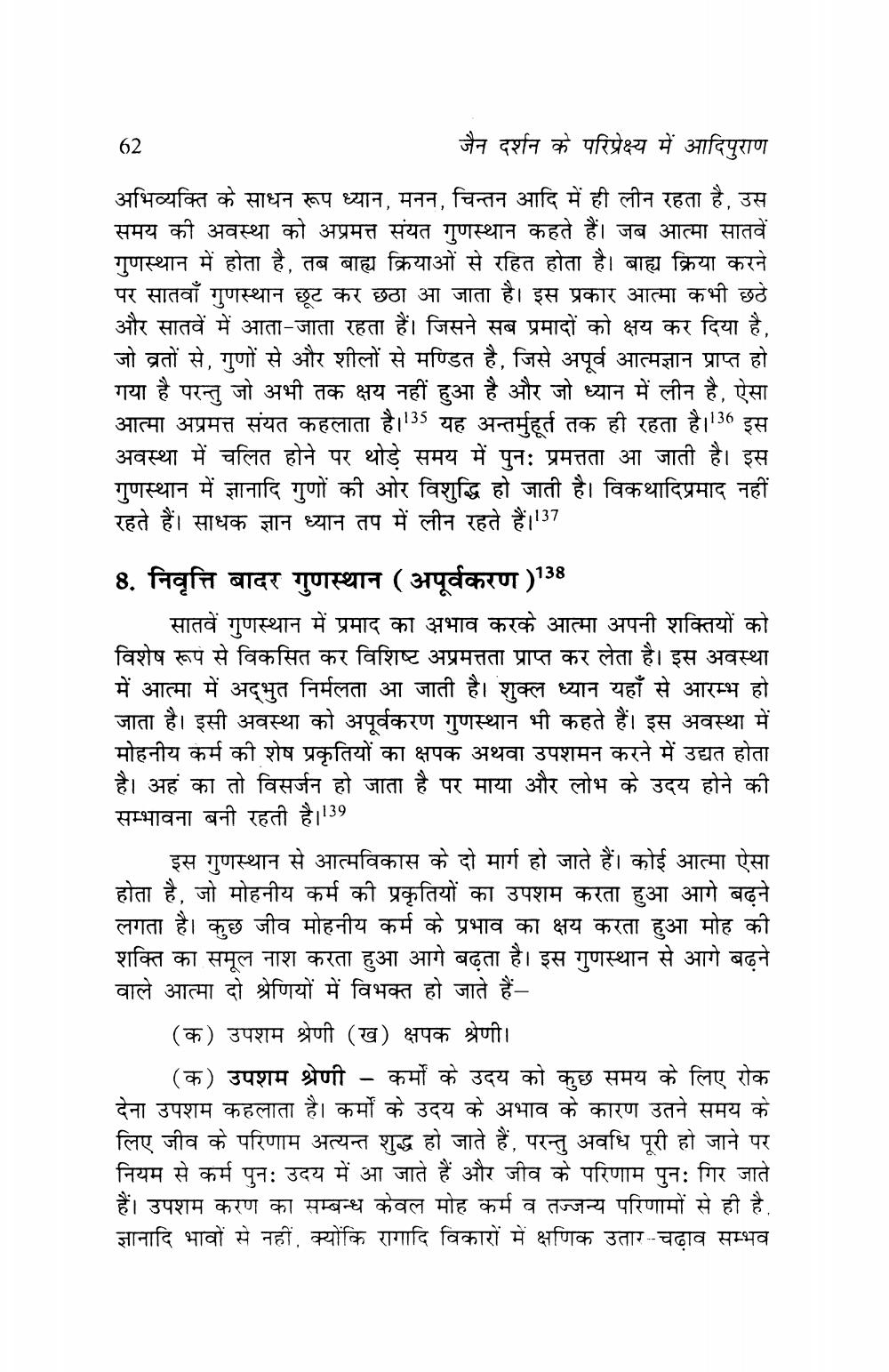________________
जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आदिपुराण
अभिव्यक्ति के साधन रूप ध्यान, मनन, चिन्तन आदि में ही लीन रहता है, उस समय की अवस्था को अप्रमत्त संयत गुणस्थान कहते हैं। जब आत्मा सातवें गुणस्थान में होता है, तब बाह्य क्रियाओं से रहित होता है। बाह्य क्रिया करने पर सातवाँ गुणस्थान छूट कर छठा आ जाता है। इस प्रकार आत्मा कभी छठे और सातवें में आता जाता रहता हैं। जिसने सब प्रमादों को क्षय कर दिया है, जो व्रतों से, गुणों से और शीलों से मण्डित है, जिसे अपूर्व आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है परन्तु जो अभी तक क्षय नहीं हुआ है और जो ध्यान में लीन है, ऐसा आत्मा अप्रमत्त संयत कहलाता है। 135 यह अन्तर्मुहूर्त तक ही रहता है। 136 इस अवस्था में चलित होने पर थोड़े समय में पुनः प्रमत्तता आ जाती है। इस गुणस्थान में ज्ञानादि गुणों की ओर विशुद्धि हो जाती है। विकथादिप्रमाद नहीं रहते हैं। साधक ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। 137
62
8. निवृत्ति बादर गुणस्थान ( अपूर्वकरण ) 138
सातवें गुणस्थान में प्रमाद का अभाव करके आत्मा अपनी शक्तियों को विशेष रूप से विकसित कर विशिष्ट अप्रमत्तता प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में आत्मा में अद्भुत निर्मलता आ जाती है। शुक्ल ध्यान यहाँ से आरम्भ हो जाता है। इसी अवस्था को अपूर्वकरण गुणस्थान भी कहते हैं। इस अवस्था में मोहनीय कर्म की शेष प्रकृतियों का क्षपक अथवा उपशमन करने में उद्यत होता है। अहं का तो विसर्जन हो जाता है पर माया और लोभ के उदय होने की सम्भावना बनी रहती है। 139
इस गुणस्थान से आत्मविकास के दो मार्ग हो जाते हैं। कोई आत्मा ऐसा होता है, जो मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। कुछ जीव मोहनीय कर्म के प्रभाव का क्षय करता हुआ मोह की शक्ति का समूल नाश करता हुआ आगे बढ़ता है। इस गुणस्थान से आगे बढ़ने वाले आत्मा दो श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं
(क) उपशम श्रेणी (ख) क्षपक श्रेणी ।
(क) उपशम श्रेणी
कर्मों के उदय को कुछ समय के लिए रोक देना उपशम कहलाता है। कर्मों के उदय के अभाव के कारण उतने समय के लिए जीव के परिणाम अत्यन्त शुद्ध हो जाते हैं, परन्तु अवधि पूरी हो जाने पर नियम से कर्म पुनः उदय में आ जाते हैं और जीव के परिणाम पुनः गिर जाते हैं। उपशम करण का सम्बन्ध केवल मोह कर्म व तज्जन्य परिणामों से ही है. ज्ञानादि भावों से नहीं, क्योंकि रागादि विकारों में क्षणिक उतार-चढ़ाव सम्भव