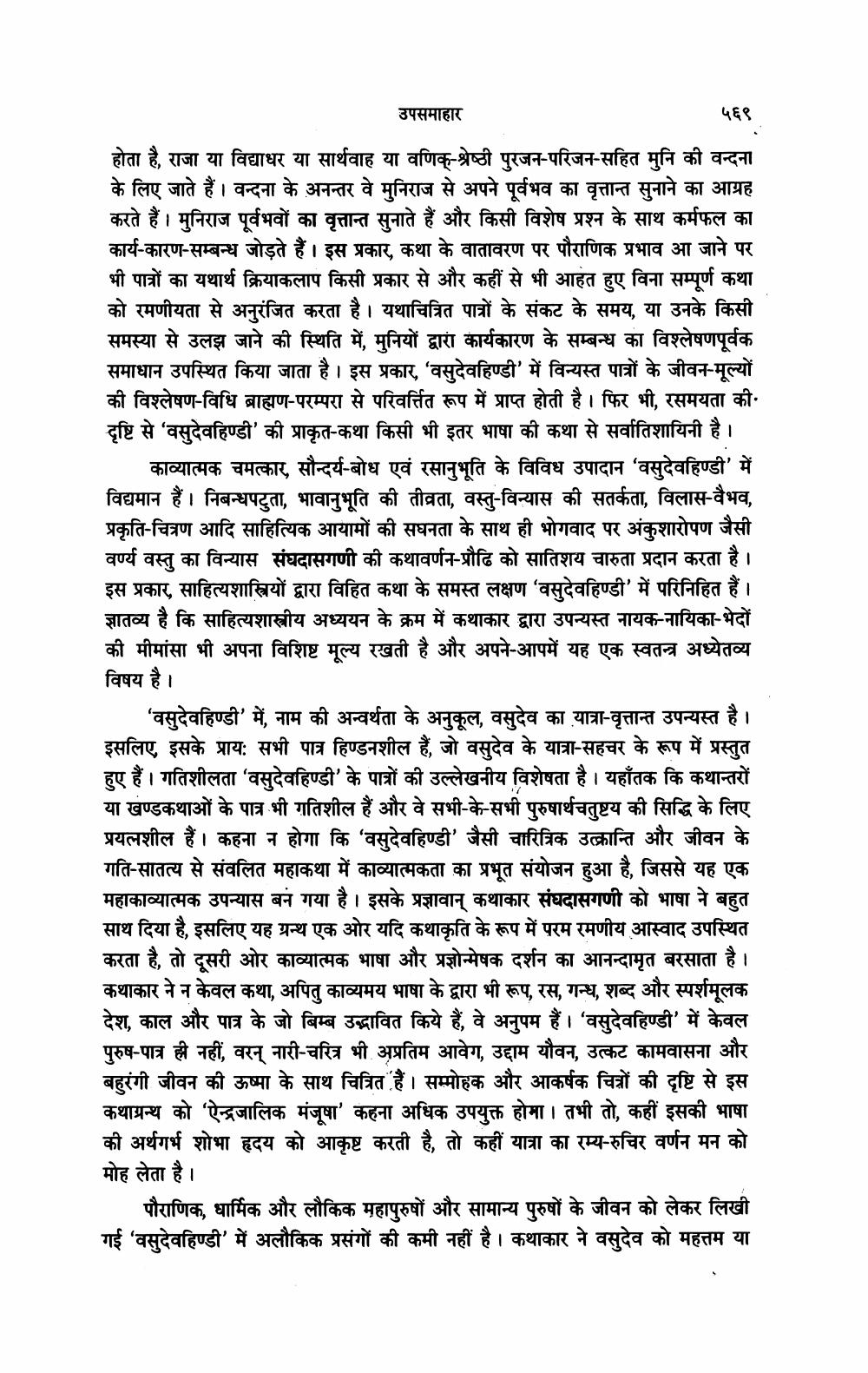________________
५६९
उपसमाहार
होता है, राजा या विद्याधर या सार्थवाह या वणिक् श्रेष्ठी पुरजन- परिजन सहित मुनि की वन्दना के लिए जाते हैं । वन्दना के अनन्तर वे मुनिराज से अपने पूर्वभव का वृत्तान्त सुनाने का आग्रह करते हैं । मुनिराज पूर्वभवों का वृत्तान्त सुनाते हैं और किसी विशेष प्रश्न के साथ कर्मफल का कार्य-कारण-सम्बन्ध जोड़ते हैं। इस प्रकार, कथा के वातावरण पर पौराणिक प्रभाव आ जाने पर भी पात्रों का यथार्थ क्रियाकलाप किसी प्रकार से और कहीं से भी आहत हुए विना सम्पूर्ण कथा को रमणीयता से अनुरंजित करता है । यथाचित्रित पात्रों के संकट के समय, या उनके किसी समस्या से उलझ जाने की स्थिति में, मुनियों द्वारा कार्यकारण के सम्बन्ध का विश्लेषणपूर्वक समाधान उपस्थित किया जाता है। इस प्रकार, 'वसुदेवहिण्डी' में विन्यस्त पात्रों के जीवन-मूल्यों की विश्लेषण - विधि ब्राह्मण-परम्परा से परिवर्तित रूप में प्राप्त होती है । फिर भी, रसमयता की. दृष्टि से 'वसुदेवहिण्डी' की प्राकृत-कथा किसी भी इतर भाषा की कथा से सर्वातिशायिनी है ।
काव्यात्मक चमत्कार, सौन्दर्य-बोध एवं रसानुभूति के विविध उपादान 'वसुदेवहिण्डी' में विद्यमान हैं। निबन्धपटुता, भावानुभूति की तीव्रता, वस्तु-विन्यास की सतर्कता, विलास-वैभव, प्रकृति-चित्रण आदि साहित्यिक आयामों की सघनता के साथ ही भोगवाद पर अंकुशारोपण जैसी वर्ण्य वस्तु का विन्यास संघदासगणी की कथावर्णन - प्रौढि को सातिशय चारुता प्रदान करता है । इस प्रकार, साहित्यशास्त्रियों द्वारा विहित कथा के समस्त लक्षण 'वसुदेवहिण्डी' में परिनिहित हैं । ज्ञातव्य है कि साहित्यशास्त्रीय अध्ययन के क्रम में कथाकार द्वारा उपन्यस्त नायक-नायिका - भेदों की मीमांसा भी अपना विशिष्ट मूल्य रखती है और अपने-आपमें यह एक स्वतन्त्र अध्येतव्य विषय है 1
'वसुदेवहिण्डी' में, नाम की अन्वर्थता के अनुकूल, वसुदेव का यात्रा- वृत्तान्त उपन्यस्त है । इसलिए, इसके प्राय: सभी पात्र हिण्डनशील हैं, जो वसुदेव के यात्रा - सहचर के रूप में प्रस्तुत हुए हैं । गतिशीलता 'वसुदेवहिण्डी' के पात्रों की उल्लेखनीय विशेषता है । यहाँतक कि कथान्तरों या खण्डकथाओं के पात्र भी गतिशील हैं और वे सभी के सभी पुरुषार्थचतुष्टय की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं। कहना न होगा कि 'वसुदेवहिण्डी' जैसी चारित्रिक उत्क्रान्ति और जीवन के गति-सातत्य से संवलित महाकथा में काव्यात्मकता का प्रभूत संयोजन हुआ है, जिससे यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास बन गया है। इसके प्रज्ञावान् कथाकार संघदासगणी को भाषा ने बहुत साथ दिया है, इसलिए यह ग्रन्थ एक ओर यदि कथाकृति के रूप में परम रमणीय आस्वाद उपस्थित करता है, तो दूसरी ओर काव्यात्मक भाषा और प्रज्ञोन्मेषक दर्शन का आनन्दामृत बरसाता है । कथाकार ने न केवल कथा, अपितु काव्यमय भाषा के द्वारा भी रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्शमूलक देश, काल और पात्र के जो बिम्ब उद्भावित किये हैं, वे अनुपम हैं। 'वसुदेवहिण्डी' में केवल पुरुष - पात्र ही नहीं, वरन् नारी- चरित्र भी अप्रतिम आवेग, उद्दाम यौवन, उत्कट कामवासना और बहुरंगी जीवन की ऊष्मा के साथ चित्रित हैं। सम्मोहक और आकर्षक चित्रों की दृष्टि से इस कथाग्रन्थ को 'ऐन्द्रजालिक मंजूषा' कहना अधिक उपयुक्त होमा। तभी तो, कहीं इसकी भाषा की अर्थगर्भ शोभा हृदय को आकृष्ट करती है, तो कहीं यात्रा का रम्य रुचिर वर्णन मन को मोह लेता है ।
पौराणिक, धार्मिक और लौकिक महापुरुषों और सामान्य पुरुषों के जीवन को लेकर लिखी गई ‘वसुदेवहिण्डी' में अलौकिक प्रसंगों की कमी नहीं है । कथाकार ने वसुदेव को महत्तम या