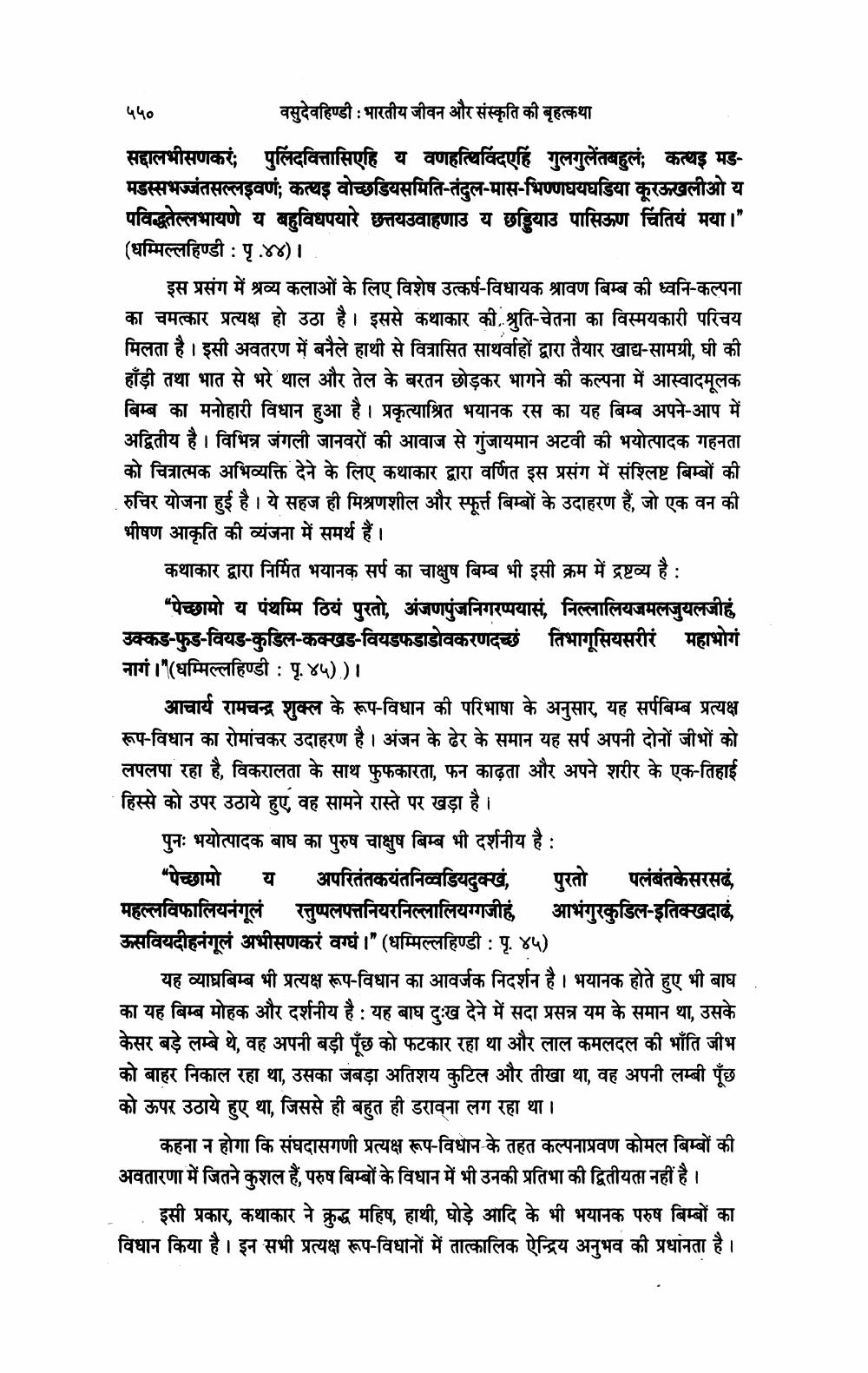________________
५५०
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा सद्दालभीसणकरं; पुलिंदवित्तासिएहि य वणहत्थिविंदएहिं गुलगुलेंतबहुलं; कत्यइ मडमडस्सभज्जंतसल्लइवणं; कत्यइ वोच्छडियसमिति-तंदुल-मास-भिण्णघयघडिया कूरऊखलीओ य पविद्धतेल्लभायणे य बहुविधपयारे छत्तयउवाहणाउ य छड्डियाउ पासिऊण चिंतियं मया।" (धम्मिल्लहिण्डी : पृ.४४)।
इस प्रसंग में श्रव्य कलाओं के लिए विशेष उत्कर्ष-विधायक श्रावण बिम्ब की ध्वनि-कल्पना का चमत्कार प्रत्यक्ष हो उठा है। इससे कथाकार की श्रुति-चेतना का विस्मयकारी परिचय मिलता है। इसी अवतरण में बनैले हाथी से वित्रासित साथर्वाहों द्वारा तैयार खाद्य-सामग्री, घी की हाँड़ी तथा भात से भरे थाल और तेल के बरतन छोड़कर भागने की कल्पना में आस्वादमूलक बिम्ब का मनोहारी विधान हआ है। प्रकत्याश्रित भयानक रस का यह बिम्ब अपने-आप में अद्वितीय है। विभिन्न जंगली जानवरों की आवाज से गुंजायमान अटवी की भयोत्पादक गहनता को चित्रात्मक अभिव्यक्ति देने के लिए कथाकार द्वारा वर्णित इस प्रसंग में संश्लिष्ट बिम्बों की रुचिर योजना हुई है। ये सहज ही मिश्रणशील और स्फूर्त बिम्बों के उदाहरण हैं, जो एक वन की भीषण आकृति की व्यंजना में समर्थ हैं।
कथाकार द्वारा निर्मित भयानक सर्प का चाक्षुष बिम्ब भी इसी क्रम में द्रष्टव्य है :
“पेच्छामो य पंथम्मि ठियं पुरतो, अंजणपुंजनिगरप्पयासं, निल्लालियजमलजुयलजीह उक्कड़-फुड-वियड-कुडिल-कक्खङ-वियडफडाडोवकरणदच्छं तिभागूसियसरीरं महाभोगं नाग। (धम्मिल्लहिण्डी : पृ. ४५) )।
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के रूप-विधान की परिभाषा के अनुसार, यह सर्पबिम्ब प्रत्यक्ष रूप-विधान का रोमांचकर उदाहरण है। अंजन के ढेर के समान यह सर्प अपनी दोनों जीभों को लपलपा रहा है, विकरालता के साथ फुफकारता, फन काढ़ता और अपने शरीर के एक-तिहाई हिस्से को उपर उठाये हुए, वह सामने रास्ते पर खड़ा है।
पुनः भयोत्पादक बाघ का पुरुष चाक्षुष बिम्ब भी दर्शनीय है :
“पेच्छामो य अपरितंतकयंतनिव्वडियदुक्खं, पुरतो पलंबतकेसरसढं महल्लविफालियनंगूलं रतुष्पलपत्तनियरनिल्लालियग्गजीहं आभंगुरकुडिल-इतिक्खदाढं ऊसवियदीहनंगूलं अभीसणकरं वग्धं ।" (धम्मिल्लहिण्डी : पृ. ४५)
यह व्याघबिम्ब भी प्रत्यक्ष रूप-विधान का आवर्जक निदर्शन है। भयानक होते हुए भी बाघ का यह बिम्ब मोहक और दर्शनीय है : यह बाघ दुःख देने में सदा प्रसन्न यम के समान था, उसके केसर बड़े लम्बे थे, वह अपनी बड़ी पूँछ को फटकार रहा था और लाल कमलदल की भाँति जीभ को बाहर निकाल रहा था, उसका जबड़ा अतिशय कुटिल और तीखा था, वह अपनी लम्बी पूँछ को ऊपर उठाये हुए था, जिससे ही बहुत ही डरावना लग रहा था।
कहना न होगा कि संघदासगणी प्रत्यक्ष रूप-विधान के तहत कल्पनाप्रवण कोमल बिम्बों की अवतारणा में जितने कुशल हैं, परुष बिम्बों के विधान में भी उनकी प्रतिभा की द्वितीयता नहीं है।
. इसी प्रकार, कथाकार ने क्रुद्ध महिष, हाथी, घोड़े आदि के भी भयानक परुष बिम्बों का विधान किया है। इन सभी प्रत्यक्ष रूप-विधानों में तात्कालिक ऐन्द्रिय अनुभव की प्रधानता है।