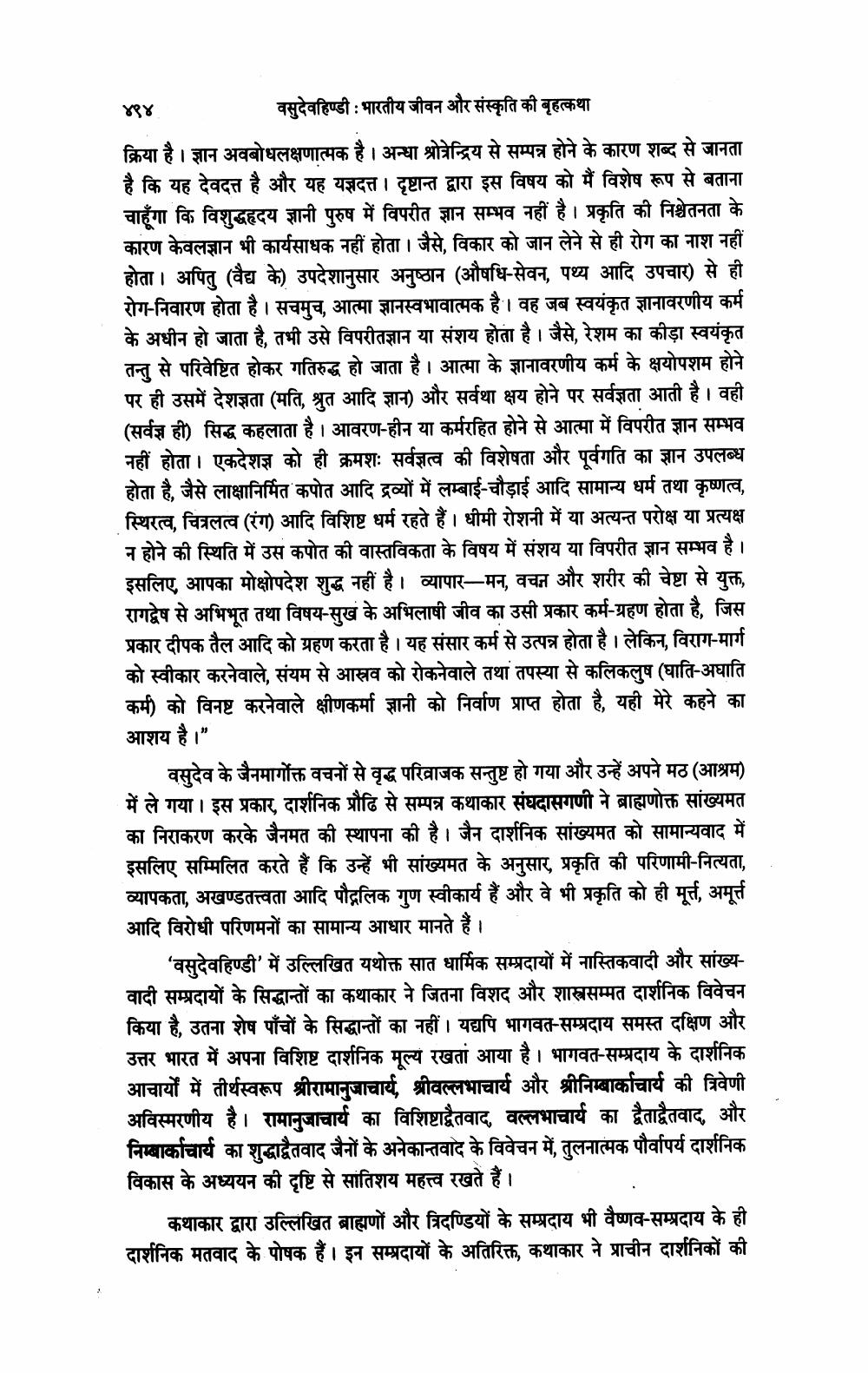________________
४९४
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा क्रिया है । ज्ञान अवबोधलक्षणात्मक है । अन्धा श्रोत्रेन्द्रिय से सम्पन्न होने के कारण शब्द से जानता है कि यह देवदत्त है और यह यज्ञदत्त । दृष्टान्त द्वारा इस विषय को मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि विशुद्धहृदय ज्ञानी पुरुष में विपरीत ज्ञान सम्भव नहीं है। प्रकृति की निश्चेतनता के कारण केवलज्ञान भी कार्यसाधक नहीं होता। जैसे, विकार को जान लेने से ही रोग का नाश नहीं होता। अपितु (वैद्य के) उपदेशानुसार अनुष्ठान (औषधि सेवन, पथ्य आदि उपचार) से ही रोग-निवारण होता है। सचमुच, आत्मा ज्ञानस्वभावात्मक है। वह जब स्वयंकृत ज्ञानावरणीय कर्म के अधीन हो जाता है, तभी उसे विपरीतज्ञान या संशय होता है। जैसे, रेशम का कीड़ा स्वयंकृत तन्तु से परिवेष्टित होकर गतिरुद्ध हो जाता है। आत्मा के ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने पर ही उसमें देशज्ञता (मति, श्रुत आदि ज्ञान) और सर्वथा क्षय होने पर सर्वज्ञता आती है। वही (सर्वज्ञ ही) सिद्ध कहलाता है। आवरण-हीन या कर्मरहित होने से आत्मा में विपरीत ज्ञान सम्भव नहीं होता। एकदेशज्ञ को ही क्रमशः सर्वज्ञत्व की विशेषता और पूर्वगति का ज्ञान उपलब्ध होता है, जैसे लाक्षानिर्मित कपोत आदि द्रव्यों में लम्बाई-चौड़ाई आदि सामान्य धर्म तथा कृष्णत्व, स्थिरत्व, चित्रलत्व (रंग) आदि विशिष्ट धर्म रहते हैं। धीमी रोशनी में या अत्यन्त परोक्ष या प्रत्यक्ष न होने की स्थिति में उस कपोत की वास्तविकता के विषय में संशय या विपरीत ज्ञान सम्भव है। इसलिए, आपका मोक्षोपदेश शुद्ध नहीं है। व्यापार–मन, वचन और शरीर की चेष्टा से युक्त, रागद्वेष से अभिभूत तथा विषय-सुख के अभिलाषी जीव का उसी प्रकार कर्म-ग्रहण होता है, जिस प्रकार दीपक तैल आदि को ग्रहण करता है। यह संसार कर्म से उत्पन्न होता है। लेकिन, विराग-मार्ग को स्वीकार करनेवाले, संयम से आस्रव को रोकनेवाले तथा तपस्या से कलिकलुष (घाति-अघाति कम) को विनष्ट करनेवाले क्षीणकर्मा ज्ञानी को निर्वाण प्राप्त होता है, यही मेरे कहने का आशय है।"
वसुदेव के जैनमागोंक्त वचनों से वृद्ध परिव्राजक सन्तुष्ट हो गया और उन्हें अपने मठ (आश्रम) में ले गया। इस प्रकार, दार्शनिक प्रौढि से सम्पन्न कथाकार संघदासगणी ने ब्राह्मणोक्त सांख्यमत का निराकरण करके जैनमत की स्थापना की है। जैन दार्शनिक सांख्यमत को सामान्यवाद में इसलिए सम्मिलित करते हैं कि उन्हें भी सांख्यमत के अनुसार, प्रकृति की परिणामी-नित्यता, व्यापकता, अखण्डतत्त्वता आदि पौद्गलिक गुण स्वीकार्य हैं और वे भी प्रकृति को ही मूर्त, अमूर्त आदि विरोधी परिणमनों का सामान्य आधार मानते हैं।
'वसुदेवहिण्डी' में उल्लिखित यथोक्त सात धार्मिक सम्प्रदायों में नास्तिकवादी और सांख्यवादी सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का कथाकार ने जितना विशद और शास्त्रसम्मत दार्शनिक विवेचन किया है, उतना शेष पाँचों के सिद्धान्तों का नहीं। यद्यपि भागवत-सम्प्रदाय समस्त दक्षिण और उत्तर भारत में अपना विशिष्ट दार्शनिक मूल्य रखता आया है। भागवत-सम्प्रदाय के दार्शनिक आचार्यों में तीर्थस्वरूप श्रीरामानुजाचार्य, श्रीवल्लभाचार्य और श्रीनिम्बार्काचार्य की त्रिवेणी अविस्मरणीय है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, और निम्बार्काचार्य का शुद्धाद्वैतवाद जैनों के अनेकान्तवाद के विवेचन में, तुलनात्मक पौर्वापर्य दार्शनिक विकास के अध्ययन की दृष्टि से सातिशय महत्त्व रखते हैं।
कथाकार द्वारा उल्लिखित ब्राह्मणों और त्रिदण्डियों के सम्प्रदाय भी वैष्णव-सम्प्रदाय के ही दार्शनिक मतवाद के पोषक हैं। इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त, कथाकार ने प्राचीन दार्शनिकों की