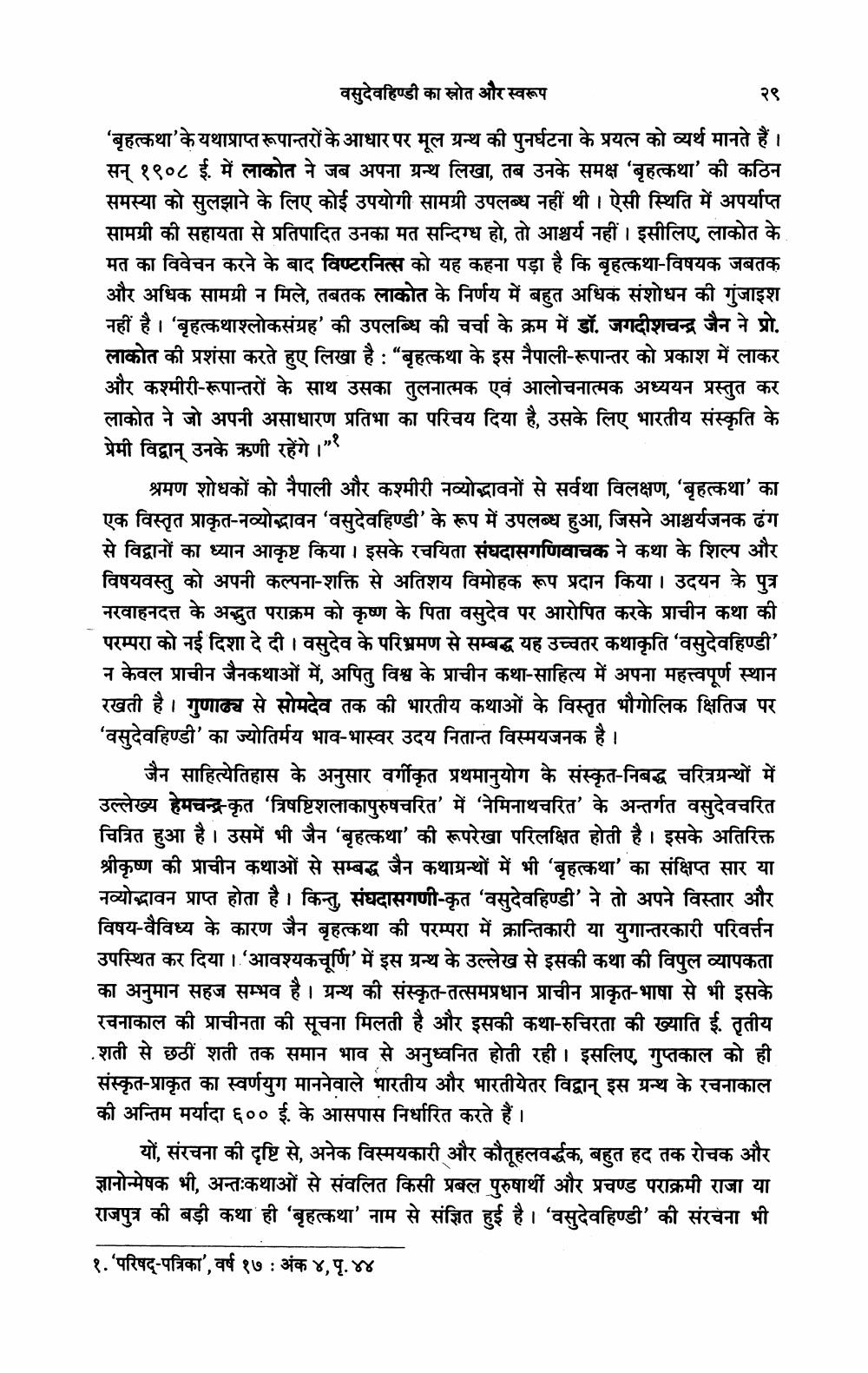________________
वसुदेवहिण्डी का स्रोत और स्वरूप
२९
‘बृहत्कथा’के यथाप्राप्त रूपान्तरों के आधार पर मूल ग्रन्थ की पुनर्घटना के प्रयत्न को व्यर्थ मानते हैं । सन् १९०८ ई. में लाकोत ने जब अपना ग्रन्थ लिखा, तब उनके समक्ष 'बृहत्कथा' की कठिन समस्या को सुलझाने के लिए कोई उपयोगी सामग्री उपलब्ध नहीं थी । ऐसी स्थिति में अपर्याप्त सामग्री की सहायता से प्रतिपादित उनका मत सन्दिग्ध हो, तो आश्चर्य नहीं। इसीलिए, लाकोत के. मत का विवेचन करने के बाद विण्टरनित्स को यह कहना पड़ा है कि बृहत्कथा-विषयक जबतक और अधिक सामग्री न मिले, तबतक लाकोत के निर्णय में बहुत अधिक संशोधन की गुंजाइश नहीं है। ‘बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' की उपलब्धि की चर्चा के क्रम में डॉ. जगदीशचन्द्र जैन ने प्रो. लाकोत की प्रशंसा करते हुए लिखा है: “बृहत्कथा के इस नैपाली - रूपान्तर को प्रकाश में लाकर और कश्मीरी - रूपान्तरों के साथ उसका तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर लाकोत ने जो अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है, उसके लिए भारतीय संस्कृति के प्रेमी विद्वान् उनके ऋणी रहेंगे ।""
श्रमण शोधकों को नैपाली और कश्मीरी नव्योद्भावनों से सर्वथा विलक्षण, 'बृहत्कथा' का एक विस्तृत प्राकृत-नव्योद्भावन 'वसुदेवहिण्डी' के रूप में उपलब्ध हुआ, जिसने आश्चर्यजनक ढंग से विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया । इसके रचयिता संघदासगणिवाचक ने कथा के शिल्प और विषयवस्तु को अपनी कल्पना - शक्ति से अतिशय विमोहक रूप प्रदान किया । उदयन के पुत्र नरवाहनदत्त के अद्भुत पराक्रम को कृष्ण के पिता वसुदेव पर आरोपित करके प्राचीन कथा की परम्परा को नई दिशा दे दी । वसुदेव के परिभ्रमण से सम्बद्ध यह उच्चतर कथाकृति 'वसुदेवहिण्डी' न केवल प्राचीन जैनकथाओं में, अपितु विश्व के प्राचीन कथा - साहित्य में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। गुणाढ्य से सोमदेव तक की भारतीय कथाओं के विस्तृत भौगोलिक क्षितिज पर ‘वसुदेवहिण्डी' का ज्योतिर्मय भाव - भास्वर उदय नितान्त विस्मयजनक है ।
जैन साहित्येतिहास के अनुसार वर्गीकृत प्रथमानुयोग के संस्कृत - निबद्ध चरित्रग्रन्थों में उल्लेख्य हेमचन्द्र-कृत ‘त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित' में 'नेमिनाथचरित' के अन्तर्गत वसुदेवचरि चित्रित हुआ है। उसमें भी जैन 'बृहत्कथा' की रूपरेखा परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण की प्राचीन कथाओं से सम्बद्ध जैन कथाग्रन्थों में भी 'बृहत्कथा' का संक्षिप्त सार या नव्योद्भावन प्राप्त होता है । किन्तु, संघदासगणी - कृत 'वसुदेवहिण्डी' ने तो अपने विस्तार और विषय- वैविध्य के कारण जैन बृहत्कथा की परम्परा में क्रान्तिकारी या युगान्तरकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया । 'आवश्यकचूर्णि' में इस ग्रन्थ के उल्लेख से इसकी कथा की विपुल व्यापकता का अनुमान सहज सम्भव है । ग्रन्थ की संस्कृत - तत्समप्रधान प्राचीन प्राकृत भाषा से भी इसके रचनाकाल की प्राचीनता की सूचना मिलती है और इसकी कथा - रुचिरता की ख्याति ई. तृतीय . शती से छठीं शती तक समान भाव से अनुध्वनित होती रही। इसलिए, गुप्तकाल को ही संस्कृत-प्राकृत का स्वर्णयुग माननेवाले भारतीय और भारतीयेतर विद्वान् इस ग्रन्थ के रचनाकाल की अन्तिम मर्यादा ६०० ई. के आसपास निर्धारित करते हैं ।
यों, संरचना की दृष्टि से, अनेक विस्मयकारी और कौतूहलवर्द्धक, बहुत हद तक रोचक और ज्ञानोन्मेषक भी, अन्तःकथाओं से संवलित किसी प्रबल पुरुषार्थी और प्रचण्ड पराक्रमी राजा या राजपुत्र की बड़ी कथा ही 'बृहत्कथा' नाम से संज्ञित हुई है । 'वसुदेवहिण्डी' की संरचना भी १. 'परिषद् - पत्रिका', वर्ष १७ : अंक ४, पृ. ४४