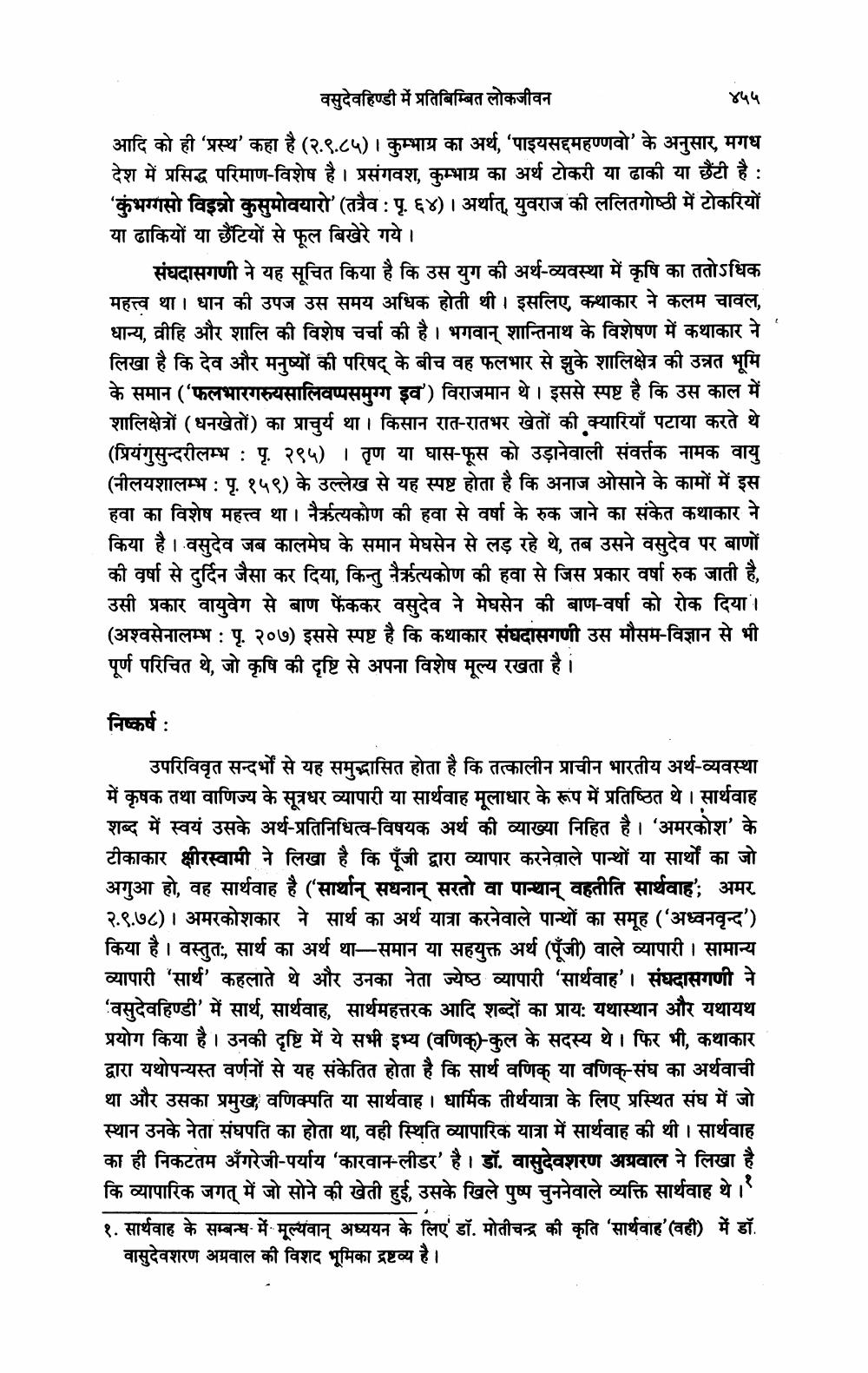________________
वसुदेवहिण्डी में प्रतिबिम्बित लोकजीवन
४५५
आदि को ही 'प्रस्थ' कहा है (२.९.८५) । कुम्भाग्र का अर्थ, 'पाइयसद्दमहण्णवो' के अनुसार, मगध देश में प्रसिद्ध परिमाण-विशेष है। प्रसंगवश, कुम्भाग्र का अर्थ टोकरी या ढाकी या छैटी है : 'कुंभग्गसो विइन्नो कुसुमोवयारो' (तत्रैव : पृ. ६४) । अर्थात्, युवराज की ललितगोष्ठी में टोकरियों या ढाकियों या छैटियों से फूल बिखेरे गये। ___संघदासगणी ने यह सूचित किया है कि उस युग की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का ततोऽधिक महत्त्व था। धान की उपज उस समय अधिक होती थी। इसलिए, कथाकार ने कलम चावल, धान्य, व्रीहि और शालि की विशेष चर्चा की है। भगवान् शान्तिनाथ के विशेषण में कथाकार ने लिखा है कि देव और मनुष्यों की परिषद् के बीच वह फलभार से झुके शालिक्षेत्र की उन्नत भूमि के समान ('फलभारगरुयसालिवप्पसमुग्ग इव') विराजमान थे। इससे स्पष्ट है कि उस काल में शालिक्षेत्रों (धनखेतों) का प्राचुर्य था। किसान रात-रातभर खेतों की क्यारियाँ पटाया करते थे (प्रियंगुसुन्दरीलम्भ : पृ. २९५) । तृण या घास-फूस को उड़ानेवाली संवर्तक नामक वायु (नीलयशालम्भ : पृ. १५९) के उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि अनाज ओसाने के कामों में इस हवा का विशेष महत्त्व था। नैर्ऋत्यकोण की हवा से वर्षा के रुक जाने का संकेत कथाकार ने किया है। वसुदेव जब कालमेघ के समान मेघसेन से लड़ रहे थे, तब उसने वसुदेव पर बाणों की वर्षा से दुर्दिन जैसा कर दिया, किन्तु नैर्ऋत्यकोण की हवा से जिस प्रकार वर्षा रुक जाती है, उसी प्रकार वायुवेग से बाण फेंककर वसुदेव ने मेघसेन की बाण-वर्षा को रोक दिया। (अश्वसेनालम्भ : पृ. २०७) इससे स्पष्ट है कि कथाकार संघदासगणी उस मौसम-विज्ञान से भी पूर्ण परिचित थे, जो कृषि की दृष्टि से अपना विशेष मूल्य रखता है।
निष्कर्ष :
उपरिविवृत सन्दर्भो से यह समुद्भासित होता है कि तत्कालीन प्राचीन भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषक तथा वाणिज्य के सूत्रधर व्यापारी या सार्थवाह मूलाधार के रूप में प्रतिष्ठित थे। सार्थवाह शब्द में स्वयं उसके अर्थ-प्रतिनिधित्व-विषयक अर्थ की व्याख्या निहित है। 'अमरकोश' के टीकाकार क्षीरस्वामी ने लिखा है कि पूँजी द्वारा व्यापार करनेवाले पान्थों या सार्थों का जो अगुआ हो, वह सार्थवाह है ('सार्थान् सधनान् सरतो वा पान्थान् वहतीति सार्थवाह'; अमर. २.९.७८)। अमरकोशकार ने सार्थ का अर्थ यात्रा करनेवाले पान्थों का समूह ('अध्वनवृन्द') किया है। वस्तुतः, सार्थ का अर्थ था-समान या सहयुक्त अर्थ (पूँजी) वाले व्यापारी । सामान्य व्यापारी 'सार्थ' कहलाते थे और उनका नेता ज्येष्ठ व्यापारी 'सार्थवाह'। संघदासगणी ने 'वसुदेवहिण्डी' में सार्थ, सार्थवाह, सार्थमहत्तरक आदि शब्दों का प्राय: यथास्थान और यथायथ प्रयोग किया है। उनकी दृष्टि में ये सभी इभ्य (वणिक्)-कुल के सदस्य थे। फिर भी, कथाकार द्वारा यथोपन्यस्त वर्णनों से यह संकेतित होता है कि सार्थ वणिक् या वणिक् संघ का अर्थवाची था और उसका प्रमुख, वणिक्पति या सार्थवाह । धार्मिक तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थित संघ में जो स्थान उनके नेता संघपति का होता था, वही स्थिति व्यापारिक यात्रा में सार्थवाह की थी। सार्थवाह का ही निकटतम अँगरेजी-पर्याय 'कारवान-लीडर' है। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है कि व्यापारिक जगत् में जो सोने की खेती हुई, उसके खिले पुष्प चुननेवाले व्यक्ति सार्थवाह थे।' १. सार्थवाह के सम्बन्ध में मूल्यवान् अध्ययन के लिए डॉ. मोतीचन्द्र की कृति 'सार्थवाह' (वही) में डॉ.
वासुदेवशरण अग्रवाल की विशद भूमिका द्रष्टव्य है।