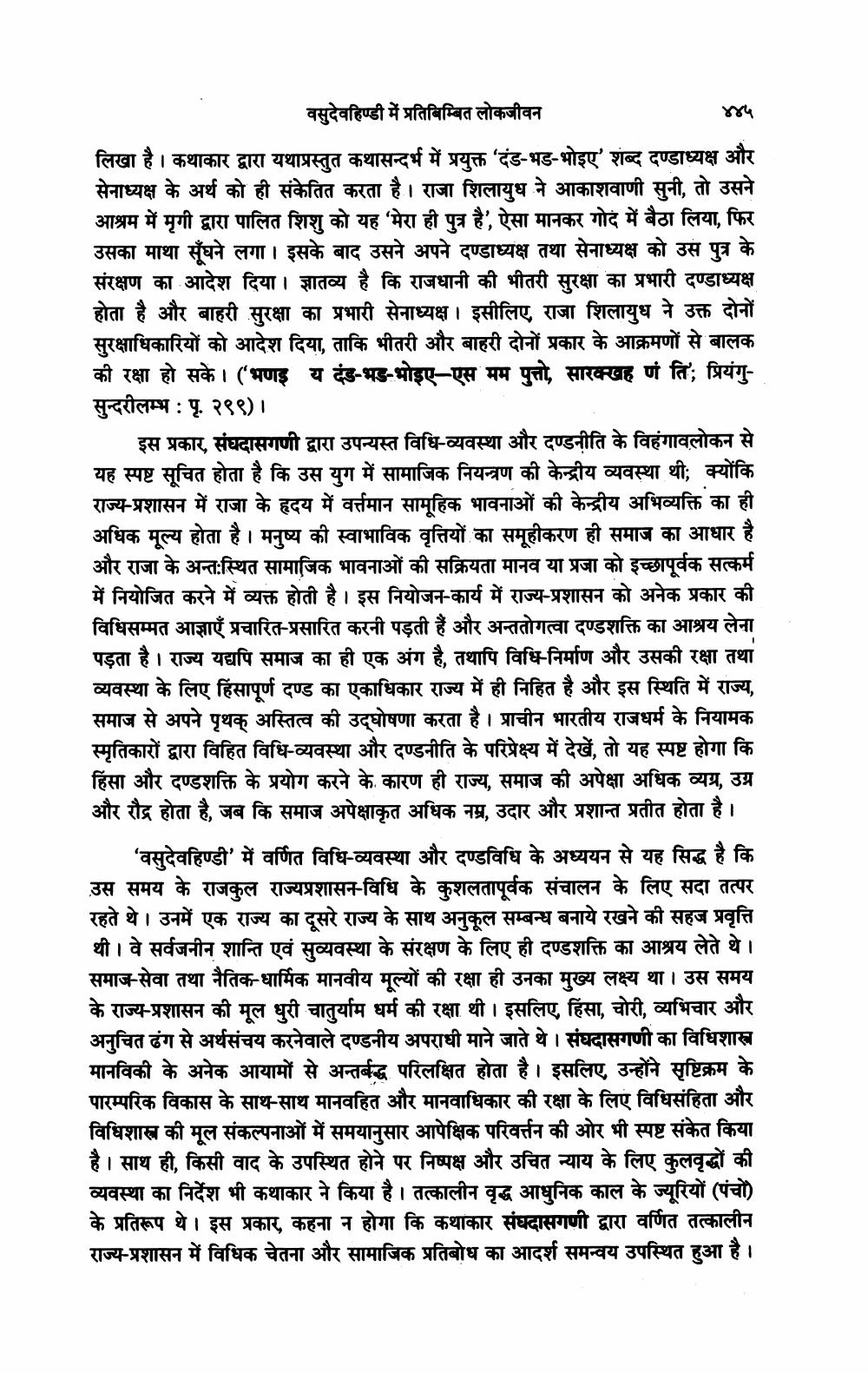________________
वसुदेवहिण्डी में प्रतिबिम्बित लोकजीवन
४४५
I
लिखा है । कथाकार द्वारा यथाप्रस्तुत कथासन्दर्भ में प्रयुक्त 'दंड-भड - भोइए' शब्द दण्डाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष के अर्थ को ही संकेतित करता है। राजा शिलायुध ने आकाशवाणी सुनी, तो उसने आश्रम में मृगी द्वारा पालित शिशु को यह 'मेरा ही पुत्र है, ऐसा मानकर गोद में बैठा लिया, फिर उसका माथा सूँघने लगा। इसके बाद उसने अपने दण्डाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष को उस पुत्र के संरक्षण का आदेश दिया। ज्ञातव्य है कि राजधानी की भीतरी सुरक्षा का प्रभारी दण्डाध्यक्ष होता है और बाहरी सुरक्षा का प्रभारी सेनाध्यक्ष । इसीलिए, राजा शिलायुध ने उक्त दोनों सुरक्षाधिकारियों को आदेश दिया, ताकि भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार के आक्रमणों से बालक की रक्षा हो सकें । ('भणइ य दंड-भड - भोइए-एस मम पुत्तो, सारक्खह णं ति; प्रियंगुसुन्दरीलम्भ: पृ. २९९) ।
इस प्रकार, संघदासगणी द्वारा उपन्यस्त विधि-व्यवस्था और दण्डनीति के विहंगावलोकन से यह स्पष्ट सूचित होता है कि उस युग में सामाजिक नियन्त्रण की केन्द्रीय व्यवस्था थी; क्योंकि राज्य- प्रशासन में राजा के हृदय में वर्त्तमान सामूहिक भावनाओं की केन्द्रीय अभिव्यक्ति का ही अधिक मूल्य होता है । मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का समूहीकरण ही समाज का आधार है और राजा के अन्तःस्थित सामाजिक भावनाओं की सक्रियता मानव या प्रजा को इच्छापूर्वक सत्कर्म में नियोजित करने में व्यक्त होती है । इस नियोजन-कार्य में राज्य - प्रशासन को अनेक प्रकार की विधिसम्मत आज्ञाएँ प्रचारित-प्रसारित करनी पड़ती हैं और अन्ततोगत्वा दण्डशक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। राज्य यद्यपि समाज का ही एक अंग है, तथापि विधि-निर्माण और उसकी रक्षा तथा व्यवस्था के लिए हिंसापूर्ण दण्ड का एकाधिकार राज्य में ही निहित है और इस स्थिति में राज्य, समाज से अपने पृथक् अस्तित्व की उद्घोषणा करता है। प्राचीन भारतीय राजधर्म के नियामक स्मृतिकारों द्वारा विहित विधि-व्यवस्था और दण्डनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यह स्पष्ट होगा कि हिंसा और दण्डशक्ति के प्रयोग करने के कारण ही राज्य, समाज की अपेक्षा अधिक व्यग्र, उग्र और रौद्र होता है, जब कि समाज अपेक्षाकृत अधिक नम्र, उदार और प्रशान्त प्रतीत होता है ।
1
'वसुदेवहिण्डी' में वर्णित विधि-व्यवस्था और दण्डविधि के अध्ययन से यह सिद्ध है कि उस समय के राजकुल राज्यप्रशासन - विधि के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए सदा तत्पर रहते थे। उनमें एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ अनुकूल सम्बन्ध बनाये रखने की सहज प्रवृत्ति थी। वे सर्वजनीन शान्ति एवं सुव्यवस्था के संरक्षण के लिए ही दण्डशक्ति का आश्रय लेते थे । समाज-सेवा तथा नैतिक-धार्मिक मानवीय मूल्यों की रक्षा ही उनका मुख्य लक्ष्य था । उस समय
राज्य - प्रशासन की मूल धुरी चातुर्याम धर्म की रक्षा थी। इसलिए, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और अनुचित ढंग से अर्थसंचय करनेवाले दण्डनीय अपराधी माने जाते थे । संघदासगणी का विधिशास्त्र मानविकी के अनेक आयामों से अन्तर्बद्ध परिलक्षित होता है । इसलिए उन्होंने सृष्टिक्रम के पारम्परिक विकास के साथ-साथ मानवहित और मानवाधिकार की रक्षा के लिए विधिसंहिता और विधिशास्त्र की मूल संकल्पनाओं में समयानुसार आपेक्षिक परिवर्तन की ओर भी स्पष्ट संकेत किया है। साथ ही, किसी वाद के उपस्थित होने पर निष्पक्ष और उचित न्याय के लिए कुलवृद्धों की व्यवस्था का निर्देश भी कथाकार ने किया है। तत्कालीन वृद्ध आधुनिक काल के ज्यूरियों (पंचों)
प्रतिरूप थे । इस प्रकार कहना न होगा कि कथाकार संघदासगणी द्वारा वर्णित तत्कालीन राज्य - प्रशासन में विधिक चेतना और सामाजिक प्रतिबोध का आदर्श समन्वय उपस्थित हुआ है ।