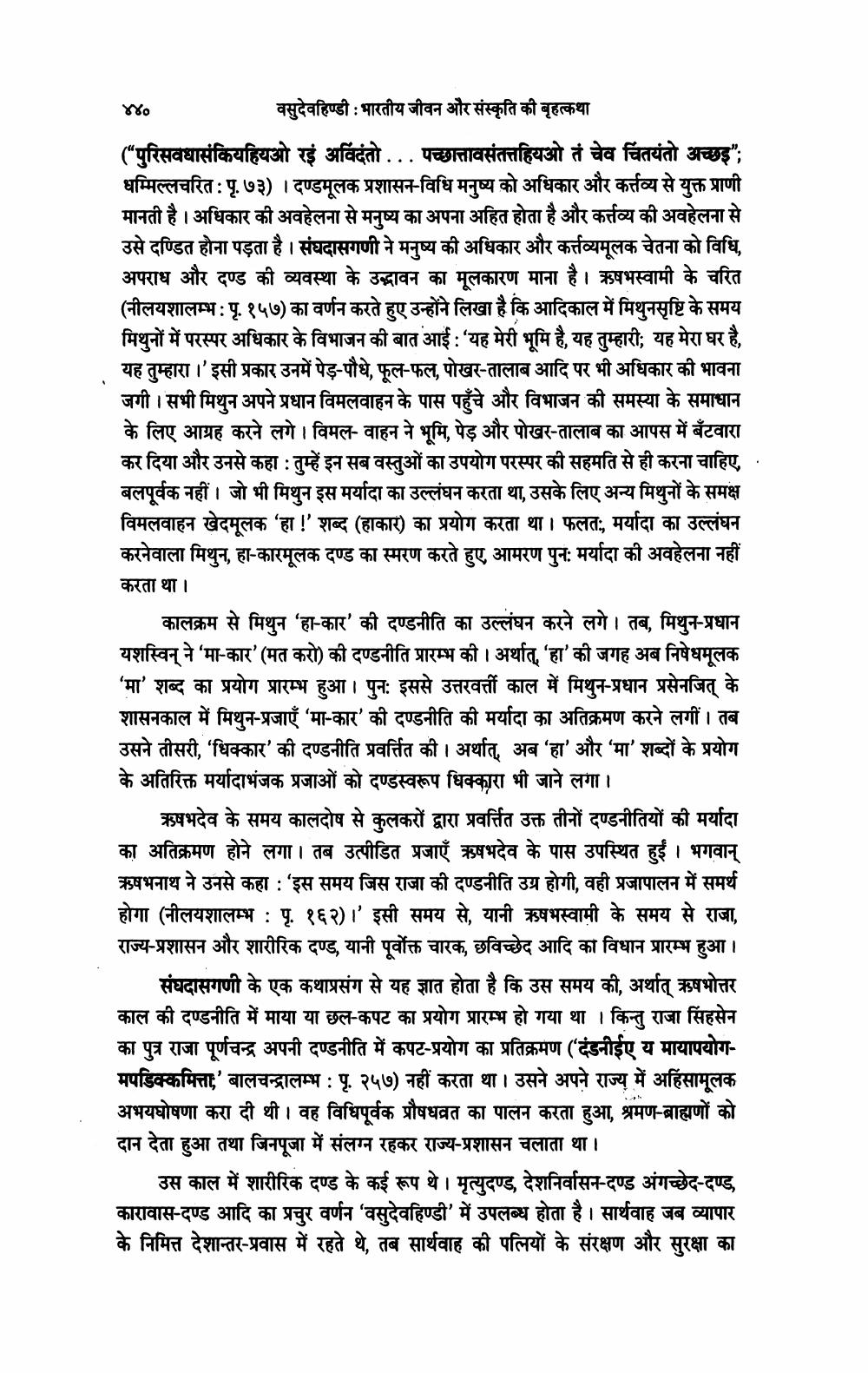________________
४४०
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
(“ पुरिसवधासंकियहियओ रई अविंदंतो
पच्छात्तावसंतत्तहियओ तं चैव चिंतयंतो अच्छइ";
1
धम्मिल्लचरित : पृ. ७३) । दण्डमूलक प्रशासन-विधि मनुष्य को अधिकार और कर्तव्य से युक्त प्राणी मानती है । अधिकार की अवहेलना से मनुष्य का अपना अहित होता है और कर्तव्य की अवहेलना से उसे दण्डित होना पड़ता है । संघदासगणी ने मनुष्य की अधिकार और कर्त्तव्यमूलक चेतना को विधि, अपराध और दण्ड की व्यवस्था के उद्भावन का मूलकारण माना है । ऋषभस्वामी के चरित (नीलयशालम्भ : पृ. १५७) का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि आदिकाल में मिथुनसृष्टि के समय मिथुनों में परस्पर अधिकार के विभाजन की बात आई : 'यह मेरी भूमि है, यह तुम्हारी; यह मेरा घर है, यह तुम्हारा।' इसी प्रकार उनमें पेड़-पौधे, फूल-फल, पोखर - तालाब आदि पर भी अधिकार की भावना जगी । सभी मिथुन अपने प्रधान विमलवाहन के पास पहुँचे और विभाजन की समस्या के समाधान के लिए आग्रह करने लगे । विमल - वाहन ने भूमि, पेड़ और पोखर - तालाब का आपस में बँटवारा कर दिया और उनसे कहा : तुम्हें इन सब वस्तुओं का उपयोग परस्पर की सहमति से ही करना चाहिए, बलपूर्वक नहीं । जो भी मिथुन इस मर्यादा का उल्लंघन करता था, उसके लिए अन्य मिथुनों के समक्ष विमलवाहन खेदमूलक 'हा !' शब्द (हाकार) का प्रयोग करता था । फलतः मर्यादा का उल्लंघन करनेवाला मिथुन, हा कारमूलक दण्ड का स्मरण करते हुए, आमरण पुनः मर्यादा की अवहेलना नहीं
करता था ।
कालक्रम से मिथुन 'हा-कार' की दण्डनीति का उल्लंघन करने लगे। तब, मिथुन - प्रधान यशस्विन् ने 'मा-कार' (मत करो) की दण्डनीति प्रारम्भ की। अर्थात्, 'हा' की जगह अब निषेधमूलक 'मा' शब्द का प्रयोग प्रारम्भ हुआ । पुनः इससे उत्तरवर्ती काल में मिथुन - प्रधान प्रसेनजित् के शासनकाल में मिथुन- प्राएँ 'मा- कार' की दण्डनीति की मर्यादा का अतिक्रमण करने लगीं। तब उसने तीसरी, 'धिक्कार' की दण्डनीति प्रवर्त्तित की । अर्थात्, अब 'हा' और 'मा' शब्दों के प्रयोग के अतिरिक्त मर्यादाभंजक प्रजाओं को दण्डस्वरूप धिक्कारा जाने लगा ।
ऋषभदेव के समय कालदोष से कुलकरों द्वारा प्रवर्त्तित उक्त तीनों दण्डनीतियों की मर्यादा का अतिक्रमण होने लगा । तब उत्पीडित प्रजाएँ ऋषभदेव के पास उपस्थित हुईं । भगवान् ऋषभनाथ ने उनसे कहा : 'इस समय जिस राजा की दण्डनीति उग्र होगी, वही प्रजापालन में समर्थ होगा (नीलयशालम्भ : पृ. १६२ ) । ' इसी समय से, यानी ऋषभस्वामी के समय से राजा, राज्य-प्रशासन और शारीरिक दण्ड, यानी पूर्वोक्त चारक, छविच्छेद आदि का विधान प्रारम्भ हुआ ।
संघदासगणी के एक कथाप्रसंग से यह ज्ञात होता है कि उस समय की, अर्थात् ऋषभोत्तर काल की दण्डनीति में माया या छल-कपट का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था । किन्तु राजा सिंहसेन का पुत्र राजा पूर्णचन्द्र अपनी दण्डनीति में कपट- प्रयोग का प्रतिक्रमण ('दंडनीईए य मायापयोगमपडिक्कमित्ता' बालचन्द्रालम्भ: पृ. २५७) नहीं करता था । उसने अपने राज्य में अहिंसामूलक अभयघोषणा करा दी थी। वह विधिपूर्वक प्रौषधव्रत का पालन करता हुआ, श्रमण-ब्राह्मणों को दान देता हुआ तथा जिनपूजा में संलग्न रहकर राज्य - प्रशासन चलाता था ।
उस काल में शारीरिक दण्ड के कई रूप थे। मृत्युदण्ड देशनिर्वासन-दण्ड अंगच्छेद-दण्ड, कारावास-दण्ड आदि का प्रचुर वर्णन 'वसुदेवहिण्डी' में उपलब्ध होता है। सार्थवाह जब व्यापार के निमित्त देशान्तर - प्रवास में रहते थे, तब सार्थवाह की पलियों के संरक्षण और सुरक्षा का