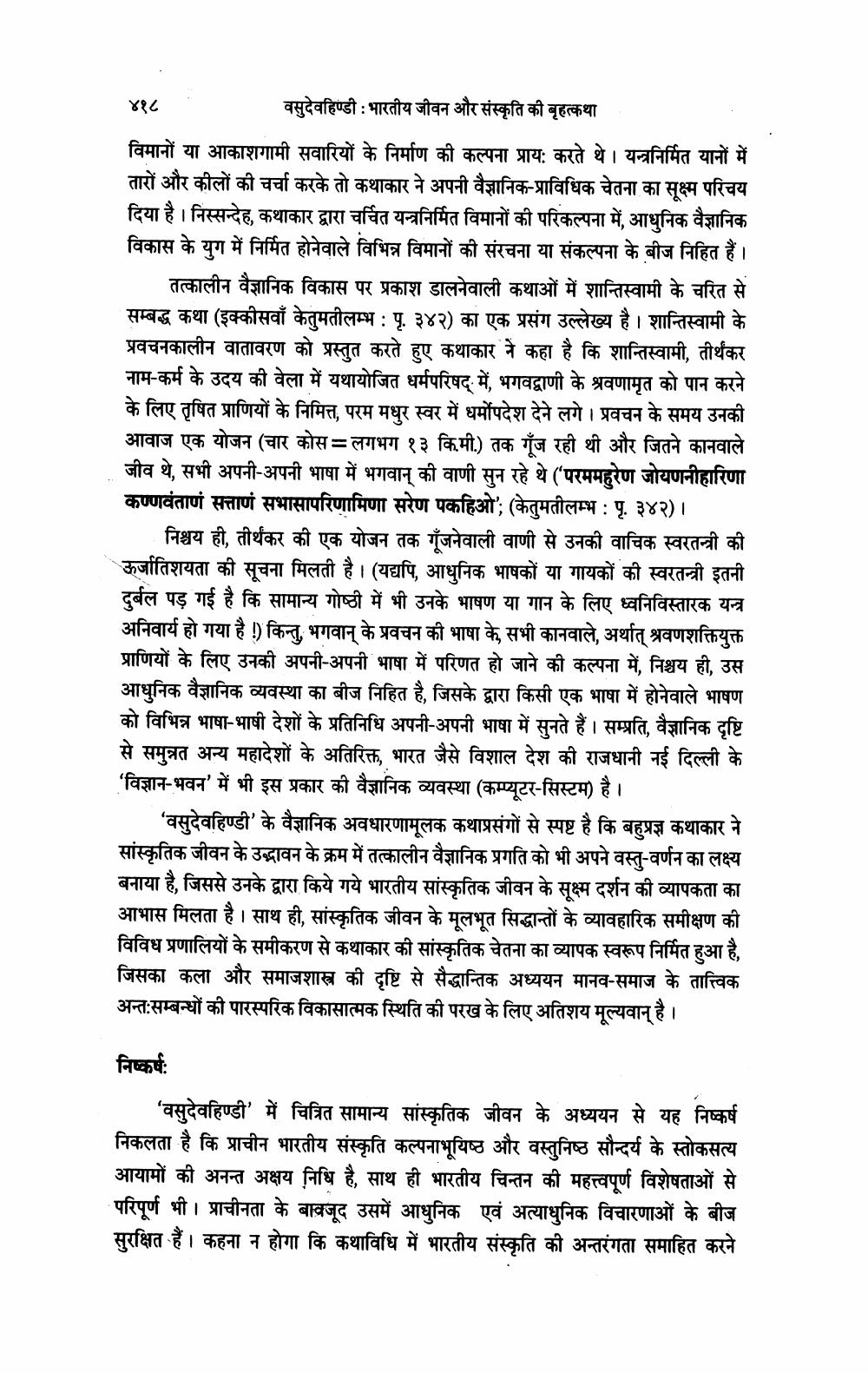________________
४१८
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा विमानों या आकाशगामी सवारियों के निर्माण की कल्पना प्राय: करते थे। यन्त्रनिर्मित यानों में तारों और कीलों की चर्चा करके तो कथाकार ने अपनी वैज्ञानिक-प्राविधिक चेतना का सूक्ष्म परिचय दिया है। निस्सन्देह, कथाकार द्वारा चर्चित यन्त्रनिर्मित विमानों की परिकल्पना में, आधुनिक वैज्ञानिक विकास के युग में निर्मित होनेवाले विभिन्न विमानों की संरचना या संकल्पना के बीज निहित हैं।
तत्कालीन वैज्ञानिक विकास पर प्रकाश डालनेवाली कथाओं में शान्तिस्वामी के चरित से सम्बद्ध कथा (इक्कीसवाँ केतुमतीलम्भ : पृ. ३४२) का एक प्रसंग उल्लेख्य है। शान्तिस्वामी के प्रवचनकालीन वातावरण को प्रस्तुत करते हुए कथाकार ने कहा है कि शान्तिस्वामी, तीर्थंकर नाम-कर्म के उदय की वेला में यथायोजित धर्मपरिषद् में, भगवद्वाणी के श्रवणामृत को पान करने के लिए तृषित प्राणियों के निमित्त, परम मधुर स्वर में धर्मोपदेश देने लगे। प्रवचन के समय उनकी आवाज एक योजन (चार कोस = लगभग १३ किमी.) तक गूंज रही थी और जितने कानवाले जीव थे, सभी अपनी-अपनी भाषा में भगवान् की वाणी सुन रहे थे ('परममहुरेण जोयणनीहारिणा कण्णवंताणं सत्ताणं सभासापरिणामिणा सरेण पकहिओ'; (केतुमतीलम्भ : पृ. ३४२) ।
निश्चय ही, तीर्थंकर की एक योजन तक गूंजनेवाली वाणी से उनकी वाचिक स्वरतन्त्री की ऊर्जातिशयता की सूचना मिलती है। (यद्यपि, आधुनिक भाषकों या गायकों की स्वरतन्त्री इतनी दुर्बल पड़ गई है कि सामान्य गोष्ठी में भी उनके भाषण या गान के लिए ध्वनिविस्तारक यन्त्र अनिवार्य हो गया है !) किन्तु, भगवान् के प्रवचन की भाषा के सभी कानवाले, अर्थात् श्रवणशक्तियुक्त प्राणियों के लिए उनकी अपनी-अपनी भाषा में परिणत हो जाने की कल्पना में, निश्चय ही, उस आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्था का बीज निहित है, जिसके द्वारा किसी एक भाषा में होनेवाले भाषण को विभिन्न भाषा-भाषी देशों के प्रतिनिधि अपनी-अपनी भाषा में सुनते हैं। सम्प्रति, वैज्ञानिक दृष्टि से समुन्नत अन्य महादेशों के अतिरिक्त, भारत जैसे विशाल देश की राजधानी नई दिल्ली के 'विज्ञान-भवन' में भी इस प्रकार की वैज्ञानिक व्यवस्था (कम्प्यूटर-सिस्टम) है।
'वसुदेवहिण्डी' के वैज्ञानिक अवधारणामूलक कथाप्रसंगों से स्पष्ट है कि बहुप्रज्ञ कथाकार ने सांस्कृतिक जीवन के उद्भावन के क्रम में तत्कालीन वैज्ञानिक प्रगति को भी अपने वस्तु-वर्णन का लक्ष्य बनाया है, जिससे उनके द्वारा किये गये भारतीय सांस्कृतिक जीवन के सूक्ष्म दर्शन की व्यापकता का आभास मिलता है। साथ ही, सांस्कृतिक जीवन के मूलभूत सिद्धान्तों के व्यावहारिक समीक्षण की विविध प्रणालियों के समीकरण से कथाकार की सांस्कृतिक चेतना का व्यापक स्वरूप निर्मित हुआ है, जिसका कला और समाजशास्त्र की दृष्टि से सैद्धान्तिक अध्ययन मानव-समाज के तात्त्विक अन्त:सम्बन्धों की पारस्परिक विकासात्मक स्थिति की परख के लिए अतिशय मूल्यवान् है ।
निष्कर्षः
'वसुदेवहिण्डी' में चित्रित सामान्य सांस्कृतिक जीवन के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति कल्पनाभूयिष्ठ और वस्तुनिष्ठ सौन्दर्य के स्तोकसत्य आयामों की अनन्त अक्षय निधि है, साथ ही भारतीय चिन्तन की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं से परिपूर्ण भी। प्राचीनता के बावजूद उसमें आधुनिक एवं अत्याधुनिक विचारणाओं के बीज सुरक्षित हैं। कहना न होगा कि कथाविधि में भारतीय संस्कृति की अन्तरंगता समाहित करने