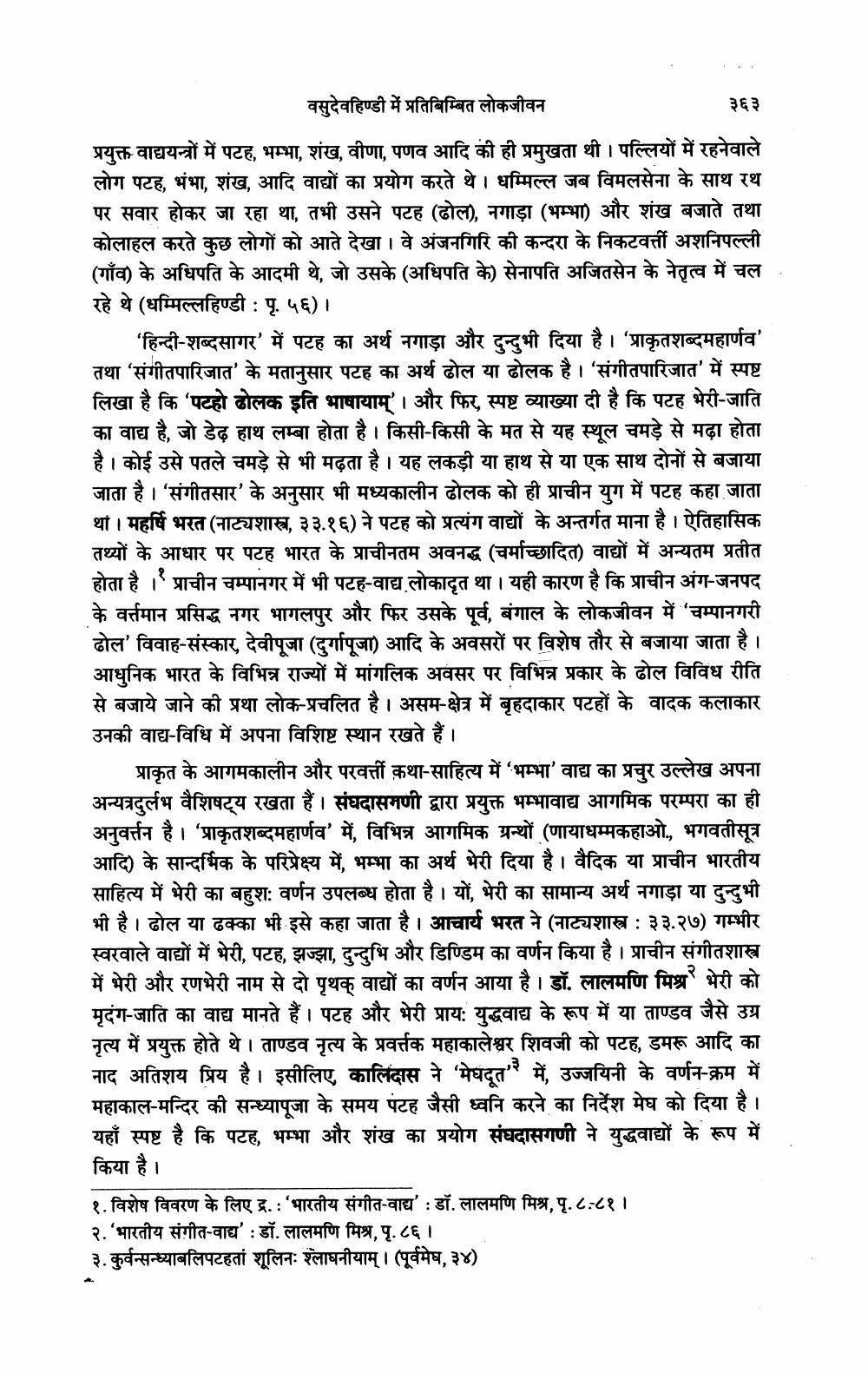________________
३६३
वसुदेवहिण्डी में प्रतिबिम्बित लोकजीवन प्रयुक्त वाद्ययन्त्रों में पटह, भम्भा, शंख, वीणा, पणव आदि की ही प्रमुखता थी। पल्लियों में रहनेवाले लोग पटह, भंभा, शंख, आदि वाद्यों का प्रयोग करते थे। धम्मिल्ल जब विमलसेना के साथ रथ पर सवार होकर जा रहा था, तभी उसने पटह (ढोल), नगाड़ा (भम्भा) और शंख बजाते तथा कोलाहल करते कुछ लोगों को आते देखा। वे अंजनगिरि की कन्दरा के निकटवर्ती अशनिपल्ली (गाँव) के अधिपति के आदमी थे, जो उसके (अधिपति के) सेनापति अजितसेन के नेतृत्व में चल रहे थे (धम्मिल्लहिण्डी : पृ. ५६)।
___ 'हिन्दी-शब्दसागर' में पटह का अर्थ नगाड़ा और दुन्दुभी दिया है। 'प्राकृतशब्दमहार्णव' तथा 'संगीतपारिजात' के मतानुसार पटह का अर्थ ढोल या ढोलक है। 'संगीतपारिजात' में स्पष्ट लिखा है कि 'पटहो ढोलक इति भाषायाम्। और फिर, स्पष्ट व्याख्या दी है कि पटह भेरी-जाति का वाद्य है, जो डेढ़ हाथ लम्बा होता है। किसी-किसी के मत से यह स्थूल चमड़े से मढ़ा होता है। कोई उसे पतले चमड़े से भी मढ़ता है। यह लकड़ी या हाथ से या एक साथ दोनों से बजाया जाता है । 'संगीतसार' के अनुसार भी मध्यकालीन ढोलक को ही प्राचीन युग में पटह कहा जाता था। महर्षि भरत (नाट्यशास्त्र, ३३.१६) ने पटह को प्रत्यंग वाद्यों के अन्तर्गत माना है । ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पटह भारत के प्राचीनतम अवनद्ध (चर्माच्छादित) वाद्यों में अन्यतम प्रतीत होता है । प्राचीन चम्पानगर में भी पटह-वाद्य लोकादृत था। यही कारण है कि प्राचीन अंग-जनपद के वर्तमान प्रसिद्ध नगर भागलपुर और फिर उसके पूर्व, बंगाल के लोकजीवन में 'चम्पानगरी ढोल' विवाह-संस्कार, देवीपूजा (दुर्गापूजा) आदि के अवसरों पर विशेष तौर से बजाया जाता है। आधुनिक भारत के विभिन्न राज्यों में मांगलिक अवसर पर विभिन्न प्रकार के ढोल विविध रीति से बजाये जाने की प्रथा लोक-प्रचलित है। असम-क्षेत्र में बृहदाकार पटहों के वादक कलाकार उनकी वाद्य-विधि में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।
प्राकृत के आगमकालीन और परवर्ती कथा-साहित्य में भम्भा' वाद्य का प्रचुर उल्लेख अपना अन्यत्रदुर्लभ वैशिषट्य रखता हैं। संघदासमणी द्वारा प्रयुक्त भम्भावाद्य आगमिक परम्परा का ही अनुवर्तन है। 'प्राकृतशब्दमहार्णव' में, विभिन्न आगमिक ग्रन्थों (णायाधम्मकहाओ, भगवतीसूत्र आदि) के सान्दर्भिक के परिप्रेक्ष्य में, भम्भा का अर्थ भेरी दिया है। वैदिक या प्राचीन भारतीय साहित्य में भेरी का बहुश: वर्णन उपलब्ध होता है। यों, भेरी का सामान्य अर्थ नगाड़ा या दुन्दुभी भी है। ढोल या ढक्का भी इसे कहा जाता है। आचार्य भरत ने (नाट्यशास्त्र : ३३.२७) गम्भीर स्वरवाले वाद्यों में भेरी, पटह, झज्झा, दुन्दुभि और डिण्डिम का वर्णन किया है। प्राचीन संगीतशास्त्र में भेरी और रणभेरी नाम से दो पृथक् वाद्यों का वर्णन आया है। डॉ. लालमणि मिश्र भेरी को मृदंग-जाति का वाद्य मानते हैं। पटह और भेरी प्राय: युद्धवाद्य के रूप में या ताण्डव जैसे उग्र नृत्य में प्रयुक्त होते थे। ताण्डव नृत्य के प्रवर्तक महाकालेश्वर शिवजी को पटह, डमरू आदि का नाद अतिशय प्रिय है। इसीलिए, कालिंदास ने 'मेघदूत' में, उज्जयिनी के वर्णन-क्रम में महाकाल-मन्दिर की सन्ध्यापूजा के समय पटह जैसी ध्वनि करने का निर्देश मेघ को दिया है। यहाँ स्पष्ट है कि पटह, भम्भा और शंख का प्रयोग संघदासगणी ने युद्धवाद्यों के रूप में किया है। १.विशेष विवरण के लिए द्र. : 'भारतीय संगीत-वाद्य' : डॉ. लालमणि मिश्र,पृ.८.८१ । २. भारतीय संगीत-वाद्य' : डॉ. लालमणि मिश्र, पृ.८६ । ३. कुर्वन्सन्ध्याबलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीयाम् । (पूर्वमेघ, ३४)