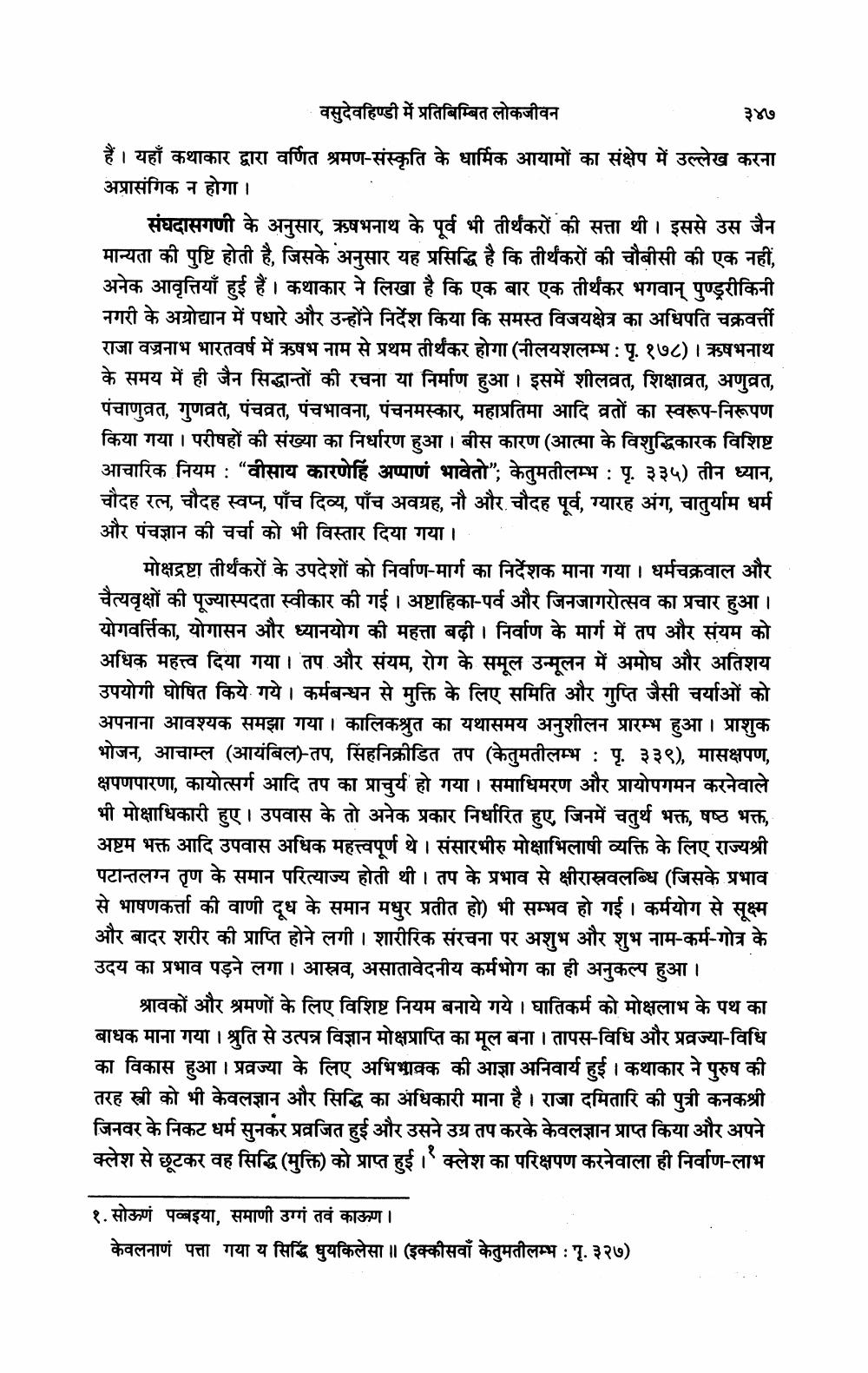________________
वसुदेवहिण्डी में प्रतिबिम्बित लोकजीवन
३४७ हैं। यहाँ कथाकार द्वारा वर्णित श्रमण-संस्कृति के धार्मिक आयामों का संक्षेप में उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा।
संघदासगणी के अनुसार, ऋषभनाथ के पूर्व भी तीर्थंकरों की सत्ता थी। इससे उस जैन मान्यता की पुष्टि होती है, जिसके अनुसार यह प्रसिद्धि है कि तीर्थंकरों की चौबीसी की एक नहीं, अनेक आवृत्तियाँ हुई हैं। कथाकार ने लिखा है कि एक बार एक तीर्थंकर भगवान् पुण्ड्ररीकिनी नगरी के अग्रोद्यान में पधारे और उन्होंने निर्देश किया कि समस्त विजयक्षेत्र का अधिपति चक्रवर्ती राजा वज्रनाभ भारतवर्ष में ऋषभ नाम से प्रथम तीर्थंकर होगा (नीलयशलम्भ : पृ. १७८) । ऋषभनाथ के समय में ही जैन सिद्धान्तों की रचना या निर्माण हुआ। इसमें शीलवत, शिक्षाव्रत, अणुव्रत, पंचाणुव्रत, गुणवत, पंचव्रत, पंचभावना, पंचनमस्कार, महाप्रतिमा आदि व्रतों का स्वरूप-निरू किया गया। परीषहों की संख्या का निर्धारण हुआ। बीस कारण (आत्मा के विशुद्धिकारक विशिष्ट आचारिक नियम : “वीसाय कारणेहि अप्पाणं भावेतो”; केतुमतीलम्भ : पृ. ३३५) तीन ध्यान, चौदह रत्न, चौदह स्वप्न, पाँच दिव्य, पाँच अवग्रह, नौ और चौदह पूर्व, ग्यारह अंग, चातुर्याम धर्म और पंचज्ञान की चर्चा को भी विस्तार दिया गया।
मोक्षद्रष्टा तीर्थंकरों के उपदेशों को निर्वाण-मार्ग का निर्देशक माना गया। धर्मचक्रवाल और चैत्यवृक्षों की पूज्यास्पदता स्वीकार की गई। अष्टाहिका-पर्व और जिनजागरोत्सव का प्रचार हुआ। योगवर्त्तिका, योगासन और ध्यानयोग की महत्ता बढ़ी। निर्वाण के मार्ग में तप और संयम को अधिक महत्त्व दिया गया। तप और संयम, रोग के समूल उन्मूलन में अमोघ और अतिशय उपयोगी घोषित किये गये। कर्मबन्धन से मुक्ति के लिए समिति और गुप्ति जैसी चर्याओं को अपनाना आवश्यक समझा गया। कालिकश्रुत का यथासमय अनुशीलन प्रारम्भ हुआ। प्राशुक भोजन, आचाम्ल (आयंबिल)-तप, सिंहनिक्रीडित तप (केतुमतीलम्भ : पृ. ३३९), मासक्षपण, क्षपणपारणा, कायोत्सर्ग आदि तप का प्राचुर्य हो गया। समाधिमरण और प्रायोपगमन करनेवाले भी मोक्षाधिकारी हुए। उपवास के तो अनेक प्रकार निर्धारित हुए, जिनमें चतुर्थ भक्त, षष्ठ भक्त, अष्टम भक्त आदि उपवास अधिक महत्त्वपूर्ण थे। संसारभीरु मोक्षाभिलाषी व्यक्ति के लिए राज्यश्री पटान्तलग्न तृण के समान परित्याज्य होती थी। तप के प्रभाव से क्षीरास्रवलब्धि (जिसके प्रभाव से भाषणकर्ता की वाणी दूध के समान मधुर प्रतीत हो) भी सम्भव हो गई। कर्मयोग से सूक्ष्म
और बादर शरीर की प्राप्ति होने लगी। शारीरिक संरचना पर अशुभ और शुभ नाम-कर्म-गोत्र के उदय का प्रभाव पड़ने लगा। आस्रव, असातावेदनीय कर्मभोग का ही अनुकल्प हुआ।
श्रावकों और श्रमणों के लिए विशिष्ट नियम बनाये गये। घातिकर्म को मोक्षलाभ के पथ का बाधक माना गया । श्रुति से उत्पन्न विज्ञान मोक्षप्राप्ति का मूल बना । तापस-विधि और प्रव्रज्या-विधि का विकास हुआ। प्रव्रज्या के लिए अभिभावक की आज्ञा अनिवार्य हुई। कथाकार ने पुरुष की तरह स्त्री को भी केवलज्ञान और सिद्धि का अधिकारी माना है। राजा दमितारि की पुत्री कनकश्री जिनवर के निकट धर्म सुनकर प्रवजित हुई और उसने उग्र तप करके केवलज्ञान प्राप्त किया और अपने क्लेश से छूटकर वह सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त हुई। क्लेश का परिक्षपण करनेवाला ही निर्वाण-लाभ
१. सोऊणं पब्बइया, समाणी उग्गं तवं काऊण ।
केवलनाणं पत्ता गया य सिद्धिं धुयकिलेसा ॥ (इक्कीसवाँ केतुमतीलम्भ : पृ. ३२७)