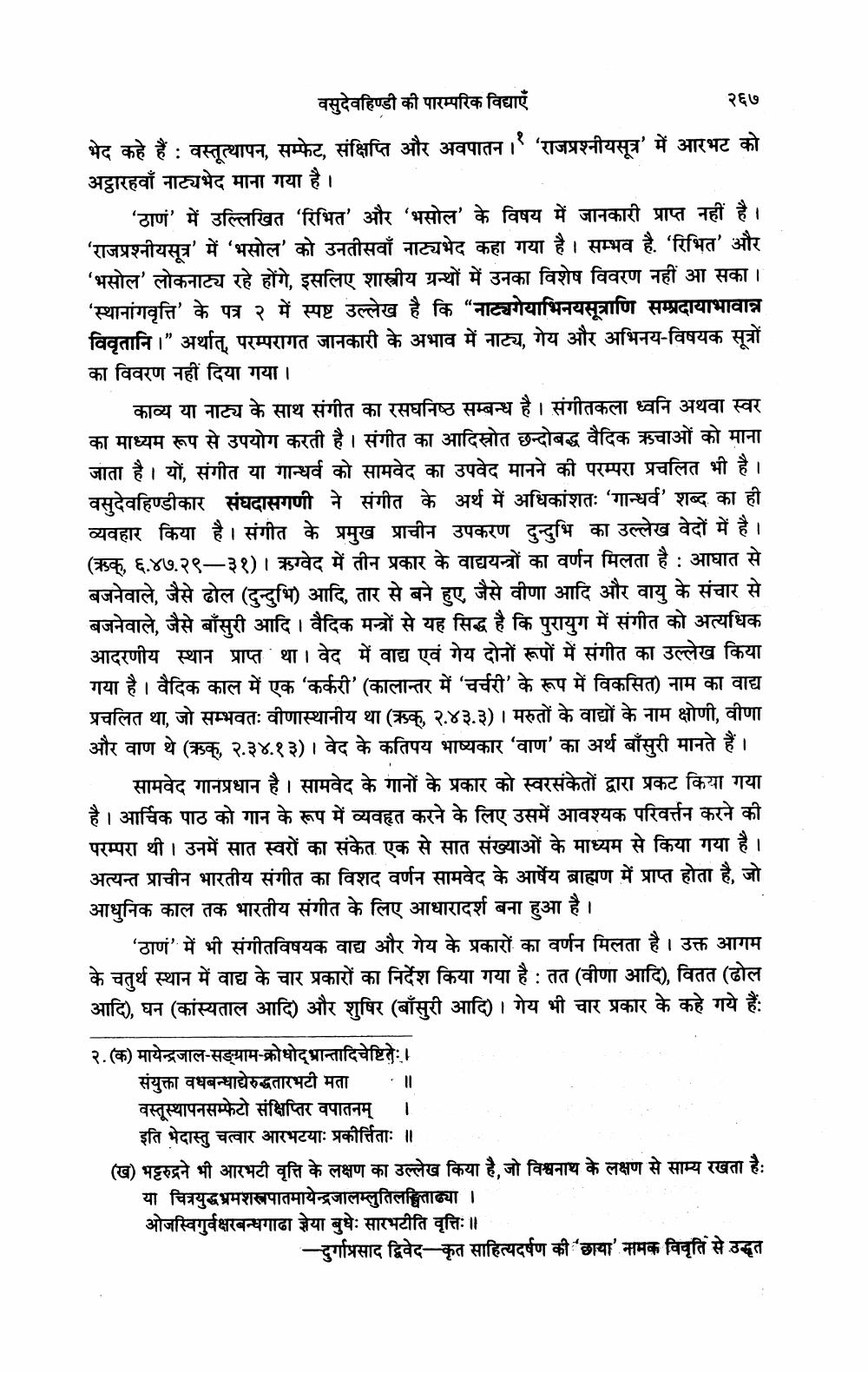________________
वसुदेवहिण्डी की पारम्परिक विद्याएँ
२६७
भेद कहे हैं : वस्तूत्थापन, सम्फेट, संक्षिप्ति और अवपातन ।' 'राजप्रश्नीयसूत्र' में आरभट को अट्ठारहवाँ नाट्यभेद माना गया है ।
'ठाणं' में उल्लिखित 'रिभित' और 'भसोल' के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं है । 'राजप्रश्नीयसूत्र' में 'भसोल' को उनतीसवाँ नाट्यभेद कहा गया है । सम्भव है. 'रिभित' और 'भसोल' लोकनाट्य रहे होंगे, इसलिए शास्त्रीय ग्रन्थों में उनका विशेष विवरण नहीं आ सका । 'स्थानांगवृत्ति' के पत्र २ में स्पष्ट उल्लेख है कि “नाट्यगेयाभिनयसूत्राणि सम्प्रदायाभावान्न विवृतानि ।” अर्थात्, परम्परागत जानकारी के अभाव में नाट्य, गेय और अभिनय - विषयक सूत्रों का विवरण नहीं दिया गया ।
काव्य या नाट्य के साथ संगीत का रसघनिष्ठ सम्बन्ध है । संगीतकला ध्वनि अथवा स्वर का माध्यम रूप से उपयोग करती है । संगीत का आदिस्रोत छन्दोबद्ध वैदिक ऋचाओं को माना जाता है । यों, संगीत या गान्धर्व को सामवेद का उपवेद मानने की परम्परा प्रचलित भी है । वसुदेवहिण्डीकार संघदासगणी ने संगीत के अर्थ में अधिकांशतः 'गान्धर्व' शब्द का ही व्यवहार किया है । संगीत के प्रमुख प्राचीन उपकरण दुन्दुभि का उल्लेख वेदों में है । (ऋक्, ६.४७.२९ – ३१) । ऋग्वेद में तीन प्रकार के वाद्ययन्त्रों का वर्णन मिलता है : आघात से बजनेवाले, जैसे ढोल (दुन्दुभि) आदि, तार से बने हुए, जैसे वीणा आदि और वायु के संचार से बजनेवाले, जैसे बाँसुरी आदि। वैदिक मन्त्रों से यह सिद्ध है कि पुरायुग में संगीत को अत्यधिक आदरणीय स्थान प्राप्त था । वेद में वाद्य एवं गेय दोनों रूपों में संगीत का उल्लेख किया गया है । वैदिक काल में एक 'कर्करी' (कालान्तर में 'चर्चरी' के रूप में विकसित) नाम का वाद्य प्रचलित था, जो सम्भवतः वीणास्थानीय था (ऋक्, २.४३.३) । मरुतों के वाद्यों के नाम क्षोणी, वीणा और वाण थे (ऋक्, २.३४.१३) । वेद के कतिपय भाष्यकार 'वाण' का अर्थ बाँसुरी मानते हैं ।
सामवेद गानप्रधान है। सामवेद के गानों के प्रकार को स्वरसंकेतों द्वारा प्रकट किया गया है । आर्चिक पाठ को गान के रूप में व्यवहृत करने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन करने की परम्परा थी। उनमें सात स्वरों का संकेत एक से सात संख्याओं के माध्यम से किया गया है। अत्यन्त प्राचीन भारतीय संगीत का विशद वर्णन सामवेद के आर्षेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है, जो आधुनिक काल तक भारतीय संगीत के लिए आधारादर्श बना हुआ है 1
'ठाणं' में भी संगीतविषयक वाद्य और गेय के प्रकारों का वर्णन मिलता है । उक्त आगम चतुर्थ स्थान में वाद्य के चार प्रकारों का निर्देश किया गया है: तत (वीणा आदि), वितत (ढोल आदि), घन (कांस्यताल आदि) और शुषिर (बाँसुरी आदि) । गेय भी चार प्रकार के कहे गये हैं:
२. (क) मायेन्द्रजाल-सङ्ग्राम-क्रोधो भ्रान्तादिचेष्टितेः । संयुक्ता वधबन्धाद्येरुद्धतारभटी मता वस्तूस्थापनसम्फेटो संक्षिप्तिर वपातनम्
||
1
इति भेदास्तु चत्वार आरभटयाः प्रकीर्त्तिताः ॥
(ख) भट्टरुद्रने भी आरभटी वृत्ति के लक्षण का उल्लेख किया है, जो विश्वनाथ के लक्षण से साम्य रखता है: या चित्रयुद्धभ्रमशस्त्रपातमायेन्द्रजालम्लुतिलङ्घिताढ्या ।
ओजस्विगुर्वक्षरबन्धगाढा ज्ञेया बुधेः सारभटीति वृत्तिः ॥
- दुर्गाप्रसाद द्विवेद—कृत साहित्यदर्पण की 'छाया' नामक विवृति से उद्धृत