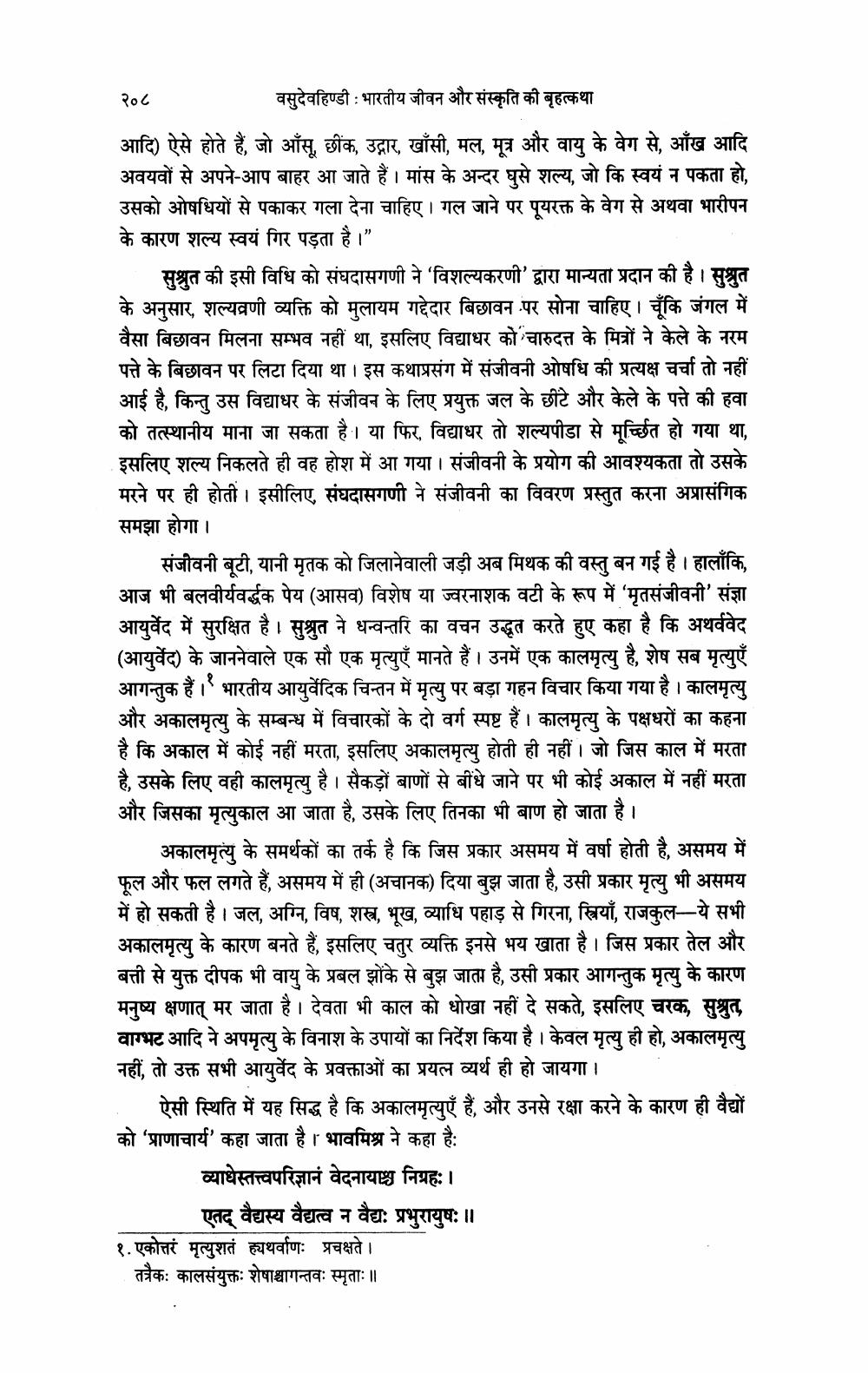________________
२०८
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा
आदि) ऐसे होते हैं, जो आँसू, छींक, उद्गार, खाँसी, मल, मूत्र और वायु के वेग से, आँख आदि अवयवों से अपने-आप बाहर आ जाते हैं। मांस के अन्दर घुसे शल्य, जो कि स्वयं न पकता हो, उसको ओषधियों से पकाकर गला देना चाहिए। गल जाने पर पूयरक्त के वेग से अथवा भारीपन के कारण शल्य स्वयं गिर पड़ता है।"
सुश्रुत की इसी विधि को संघदासगणी ने 'विशल्यकरणी' द्वारा मान्यता प्रदान की है। सुश्रुत के अनुसार, शल्यव्रणी व्यक्ति को मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोना चाहिए। चूँकि जंगल में वैसा बिछावन मिलना सम्भव नहीं था, इसलिए विद्याधर को चारुदत्त के मित्रों ने केले के नरम पत्ते के बिछावन पर लिटा दिया था। इस कथाप्रसंग में संजीवनी ओषधि की प्रत्यक्ष चर्चा तो नहीं आई है, किन्तु उस विद्याधर के संजीवन के लिए प्रयुक्त जल के छीटे और केले के पत्ते की हवा को तत्स्थानीय माना जा सकता है। या फिर, विद्याधर तो शल्यपीडा से मूर्च्छित हो गया था, इसलिए शल्य निकलते ही वह होश में आ गया। संजीवनी के प्रयोग की आवश्यकता तो उसके मरने पर ही होती। इसीलिए, संघदासगणी ने संजीवनी का विवरण प्रस्तुत करना अप्रासंगिक समझा होगा। __ संजीवनी बूटी, यानी मृतक को जिलानेवाली जड़ी अब मिथक की वस्तु बन गई है। हालाँकि, आज भी बलवीर्यवर्द्धक पेय (आसव) विशेष या ज्वरनाशक वटी के रूप में 'मृतसंजीवनी' संज्ञा आयुर्वेद में सुरक्षित है। सुश्रुत ने धन्वन्तरि का वचन उद्धृत करते हुए कहा है कि अथर्ववेद (आयुर्वेद) के जाननेवाले एक सौ एक मृत्युएँ मानते हैं। उनमें एक कालमृत्यु है, शेष सब मृत्युएँ आगन्तुक हैं। भारतीय आयुर्वेदिक चिन्तन में मृत्यु पर बड़ा गहन विचार किया गया है । कालमृत्यु और अकालमृत्यु के सम्बन्ध में विचारकों के दो वर्ग स्पष्ट हैं। कालमृत्यु के पक्षधरों का कहना है कि अकाल में कोई नहीं मरता, इसलिए अकालमृत्यु होती ही नहीं। जो जिस काल में मरता है, उसके लिए वही कालमृत्यु है। सैकड़ों बाणों से बीधे जाने पर भी कोई अकाल में नहीं मरता और जिसका मृत्युकाल आ जाता है, उसके लिए तिनका भी बाण हो जाता है। ___ अकालमृत्यु के समर्थकों का तर्क है कि जिस प्रकार असमय में वर्षा होती है, असमय में फूल और फल लगते हैं, असमय में ही (अचानक) दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार मृत्यु भी असमय में हो सकती है। जल, अग्नि, विष, शस्त्र, भूख, व्याधि पहाड़ से गिरना, स्त्रियाँ, राजकुल-ये सभी अकालमृत्यु के कारण बनते हैं, इसलिए चतुर व्यक्ति इनसे भय खाता है। जिस प्रकार तेल और बत्ती से युक्त दीपक भी वायु के प्रबल झोंके से बुझ जाता है, उसी प्रकार आगन्तुक मृत्यु के कारण मनुष्य क्षणात् मर जाता है। देवता भी काल को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि ने अपमृत्यु के विनाश के उपायों का निर्देश किया है । केवल मृत्यु ही हो, अकालमृत्यु नहीं, तो उक्त सभी आयुर्वेद के प्रवक्ताओं का प्रयत्न व्यर्थ ही हो जायगा। . ऐसी स्थिति में यह सिद्ध है कि अकालमृत्युएँ हैं, और उनसे रक्षा करने के कारण ही वैद्यों को 'प्राणाचार्य' कहा जाता है। भावमिश्र ने कहा है:
व्याघेस्तत्त्वपरिज्ञानं वेदनायाच निग्रहः ।
एतद् वैद्यस्य वैद्यत्व न वैद्यः प्रभुरायुषः ।। १. एकोत्तरं मृत्युशतं यथर्वाणः प्रचक्षते । तत्रैकः कालसंयुक्तः शेषाश्चागन्तवः स्मृताः ॥