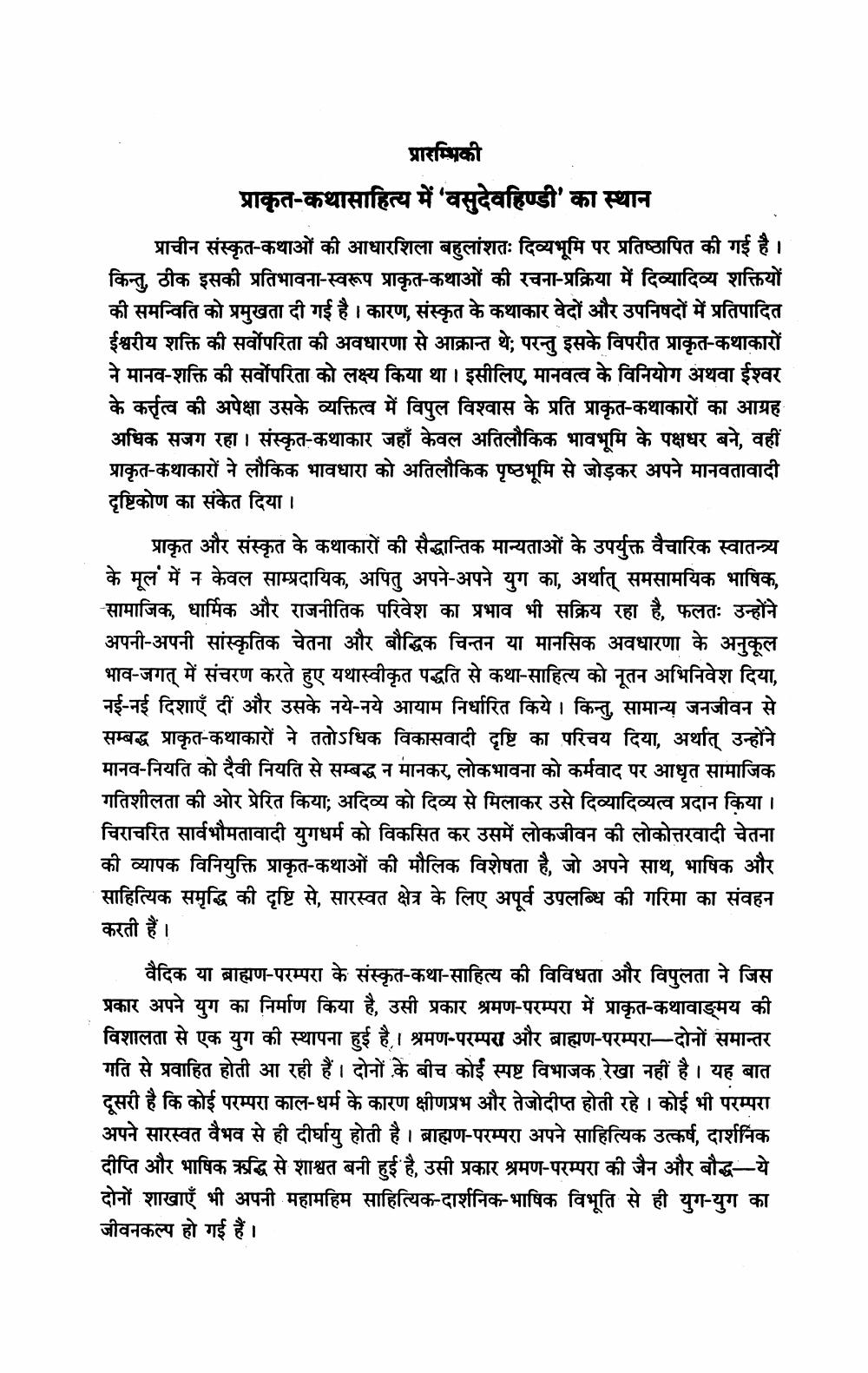________________
प्रारम्भिकी प्राकृत-कथासाहित्य में 'वसुदेवहिण्डी' का स्थान प्राचीन संस्कृत-कथाओं की आधारशिला बहुलांशतः दिव्यभूमि पर प्रतिष्ठापित की गई है। किन्तु, ठीक इसकी प्रतिभावना-स्वरूप प्राकृत-कथाओं की रचना-प्रक्रिया में दिव्यादिव्य शक्तियों की समन्विति को प्रमुखता दी गई है । कारण, संस्कृत के कथाकार वेदों और उपनिषदों में प्रतिपादित ईश्वरीय शक्ति की सर्वोपरिता की अवधारणा से आक्रान्त थे; परन्तु इसके विपरीत प्राकृत-कथाकारों ने मानव-शक्ति की सर्वोपरिता को लक्ष्य किया था। इसीलिए, मानवत्व के विनियोग अथवा ईश्वर के कर्तृत्व की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व में विपुल विश्वास के प्रति प्राकृत-कथाकारों का आग्रह अधिक सजग रहा। संस्कृत-कथाकार जहाँ केवल अतिलौकिक भावभूमि के पक्षधर बने, वहीं प्राकृत-कथाकारों ने लौकिक भावधारा को अतिलौकिक पृष्ठभूमि से जोड़कर अपने मानवतावादी दृष्टिकोण का संकेत दिया।
प्राकृत और संस्कृत के कथाकारों की सैद्धान्तिक मान्यताओं के उपर्युक्त वैचारिक स्वातन्त्र्य के मूल में न केवल साम्प्रदायिक, अपितु अपने-अपने युग का, अर्थात् समसामयिक भाषिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवेश का प्रभाव भी सक्रिय रहा है, फलतः उन्होंने अपनी-अपनी सांस्कृतिक चेतना और बौद्धिक चिन्तन या मानसिक अवधारणा के अनुकूल भाव-जगत् में संचरण करते हुए यथास्वीकृत पद्धति से कथा-साहित्य को नूतन अभिनिवेश दिया, नई-नई दिशाएँ दी और उसके नये-नये आयाम निर्धारित किये। किन्तु, सामान्य जनजीवन से सम्बद्ध प्राकृत-कथाकारों ने ततोऽधिक विकासवादी दृष्टि का परिचय दिया, अर्थात् उन्होंने मानव-नियति को दैवी नियति से सम्बद्ध न मानकर, लोकभावना को कर्मवाद पर आधृत सामाजिक गतिशीलता की ओर प्रेरित किया; अदिव्य को दिव्य से मिलाकर उसे दिव्यादिव्यत्व प्रदान किया। चिराचरित सार्वभौमतावादी युगधर्म को विकसित कर उसमें लोकजीवन की लोकोत्तरवादी चेतना की व्यापक विनियुक्ति प्राकृत-कथाओं की मौलिक विशेषता है, जो अपने साथ, भाषिक और साहित्यिक समृद्धि की दृष्टि से, सारस्वत क्षेत्र के लिए अपूर्व उपलब्धि की गरिमा का संवहन करती हैं।
वैदिक या ब्राह्मण-परम्परा के संस्कृत-कथा-साहित्य की विविधता और विपुलता ने जिस प्रकार अपने युग का निर्माण किया है, उसी प्रकार श्रमण-परम्परा में प्राकृत-कथावाङ्मय की विशालता से एक युग की स्थापना हुई है,। श्रमण-परम्परा और ब्राह्मण-परम्परा-दोनों समान्तर गति से प्रवाहित होती आ रही हैं। दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है। यह बात दूसरी है कि कोई परम्परा काल-धर्म के कारण क्षीणप्रभ और तेजोदीप्त होती रहे। कोई भी परम्परा अपने सारस्वत वैभव से ही दीर्घायु होती है। ब्राह्मण-परम्परा अपने साहित्यिक उत्कर्ष, दार्शनिक दीप्ति और भाषिक ऋद्धि से शाश्वत बनी हुई है, उसी प्रकार श्रमण-परम्परा की जैन और बौद्ध-ये दोनों शाखाएँ भी अपनी महामहिम साहित्यिक दार्शनिक-भाषिक विभूति से ही युग-युग का जीवनकल्प हो गई हैं।