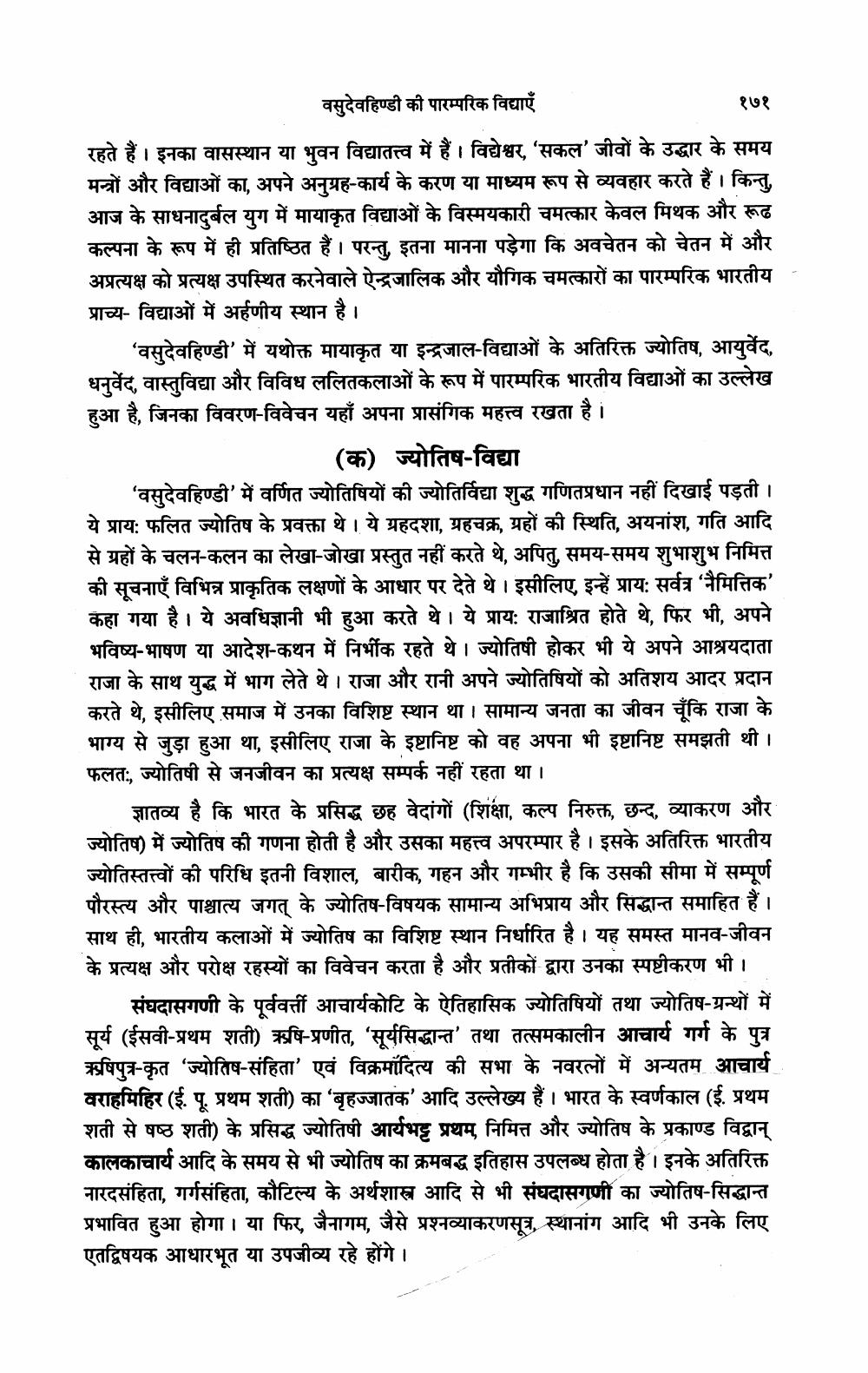________________
वसुदेवहिण्डी की पारम्परिक विद्याएँ
१७१ रहते हैं। इनका वासस्थान या भुवन विद्यातत्त्व में हैं। विद्येश्वर, 'सकल' जीवों के उद्धार के समय मन्त्रों और विद्याओं का, अपने अनुग्रह-कार्य के करण या माध्यम रूप से व्यवहार करते हैं। किन्तु, आज के साधनादुर्बल युग में मायाकृत विद्याओं के विस्मयकारी चमत्कार केवल मिथक और रूढ कल्पना के रूप में ही प्रतिष्ठित हैं। परन्तु, इतना मानना पड़ेगा कि अवचेतन को चेतन में और अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष उपस्थित करनेवाले ऐन्द्रजालिक और यौगिक चमत्कारों का पारम्परिक भारतीय प्राच्य- विद्याओं में अर्हणीय स्थान है।
'वसुदेवहिण्डी' में यथोक्त मायाकृत या इन्द्रजाल-विद्याओं के अतिरिक्त ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, वास्तुविद्या और विविध ललितकलाओं के रूप में पारम्परिक भारतीय विद्याओं का उल्लेख हुआ है, जिनका विवरण-विवेचन यहाँ अपना प्रासंगिक महत्त्व रखता है।
(क) ज्योतिष-विद्या 'वसुदेवहिण्डी' में वर्णित ज्योतिषियों की ज्योतिर्विद्या शुद्ध गणितप्रधान नहीं दिखाई पड़ती। ये प्राय: फलित ज्योतिष के प्रवक्ता थे। ये ग्रहदशा, ग्रहचक्र, ग्रहों की स्थिति, अयनांश, गति आदि से ग्रहों के चलन-कलन का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं करते थे, अपितु, समय-समय शुभाशुभ निमित्त की सूचनाएँ विभिन्न प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर देते थे। इसीलिए, इन्हें प्राय: सर्वत्र 'नैमित्तिक' कहा गया है। ये अवधिज्ञानी भी हुआ करते थे। ये प्राय: राजाश्रित होते थे, फिर भी, अपने भविष्य-भाषण या आदेश-कथन में निर्भीक रहते थे। ज्योतिषी होकर भी ये अपने आश्रयदाता राजा के साथ युद्ध में भाग लेते थे। राजा और रानी अपने ज्योतिषियों को अतिशय आदर प्रदान करते थे, इसीलिए समाज में उनका विशिष्ट स्थान था। सामान्य जनता का जीवन चूँकि राजा के भाग्य से जुड़ा हुआ था, इसीलिए राजा के इष्टानिष्ट को वह अपना भी इष्टानिष्ट समझती थी। फलतः, ज्योतिषी से जनजीवन का प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रहता था।
ज्ञातव्य है कि भारत के प्रसिद्ध छह वेदांगों (शिक्षा, कल्प निरुक्त, छन्द, व्याकरण और ज्योतिष) में ज्योतिष की गणना होती है और उसका महत्त्व अपरम्पार है। इसके अतिरिक्त भारतीय ज्योतिस्तत्त्वों की परिधि इतनी विशाल, बारीक, गहन और गम्भीर है कि उसकी सीमा में सम्पूर्ण पौरस्त्य और पाश्चात्य जगत् के ज्योतिष-विषयक सामान्य अभिप्राय और सिद्धान्त समाहित हैं। साथ ही, भारतीय कलाओं में ज्योतिष का विशिष्ट स्थान निर्धारित है। यह समस्त मानव-जीवन के प्रत्यक्ष और परोक्ष रहस्यों का विवेचन करता है और प्रतीकों द्वारा उनका स्पष्टीकरण भी।
संघदासगणी के पूर्ववत्ती आचार्यकोटि के ऐतिहासिक ज्योतिषियों तथा ज्योतिष-ग्रन्थों में सूर्य (ईसवी-प्रथम शती) ऋषि-प्रणीत, 'सूर्यसिद्धान्त' तथा तत्समकालीन आचार्य गर्ग के पुत्र ऋषिपुत्र-कृत ‘ज्योतिष-संहिता' एवं विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में अन्यतम आचार्य वराहमिहिर (ई. पू. प्रथम शती) का 'बृहज्जातक' आदि उल्लेख्य हैं। भारत के स्वर्णकाल (ई. प्रथम शती से षष्ठ शती) के प्रसिद्ध ज्योतिषी आर्यभट्ट प्रथम, निमित्त और ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वान् कालकाचार्य आदि के समय से भी ज्योतिष का क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध होता है। इनके अतिरिक्त नारदसंहिता, गर्गसंहिता, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि से भी संघदासगणी का ज्योतिष-सिद्धान्त प्रभावित हुआ होगा। या फिर, जैनागम, जैसे प्रश्नव्याकरणसूत्र, स्थानांग आदि भी उनके लिए एतद्विषयक आधारभूत या उपजीव्य रहे होंगे।