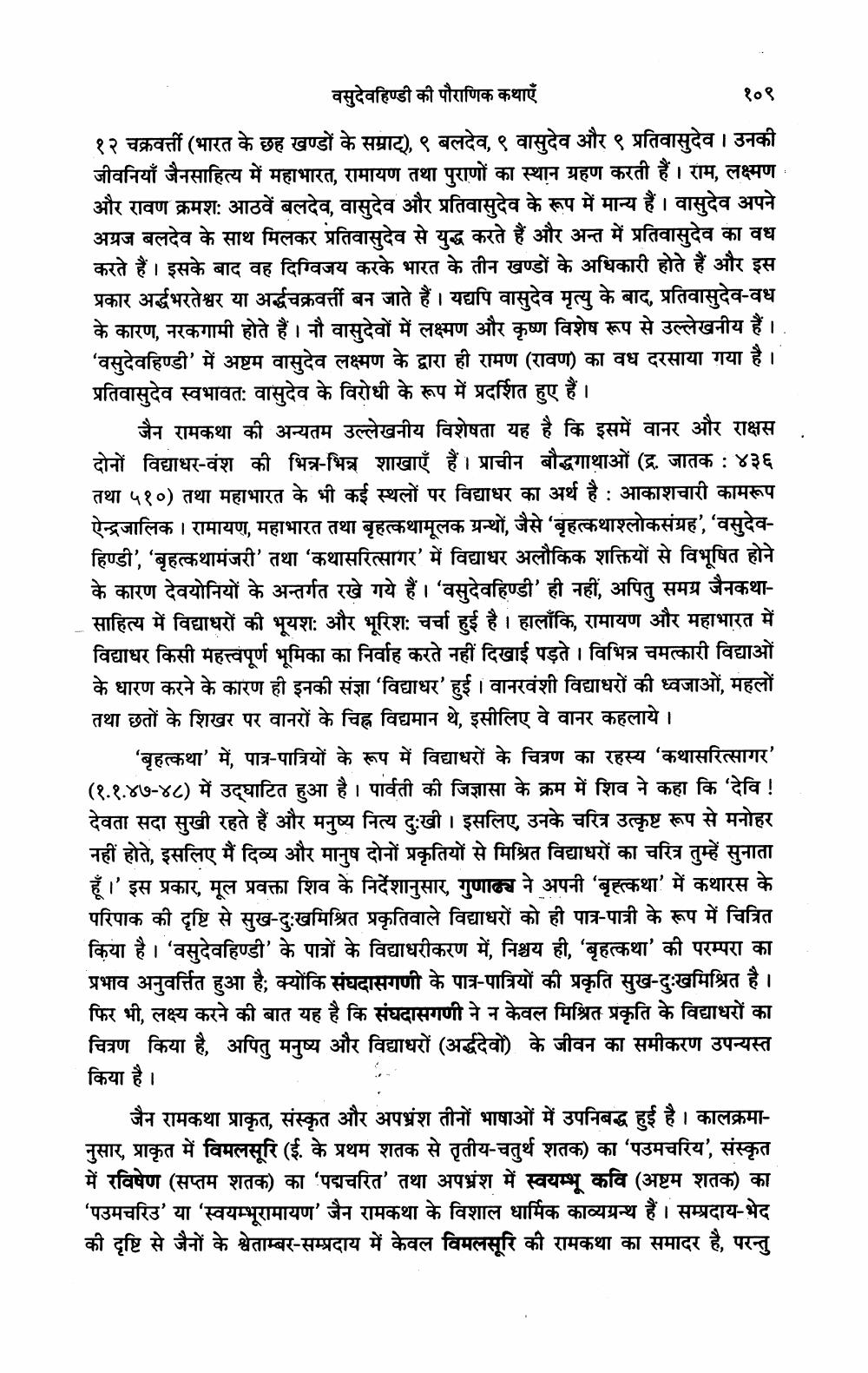________________
वसुदेवहिण्डी की पौराणिक कथाएँ
१०९
१२ चक्रवर्त्ती (भारत के छह खण्डों के सम्राट्), ९ बलदेव, ९ वासुदेव और ९ प्रतिवासुदेव । उनकी जीवनियाँ जैनसाहित्य में महाभारत, रामायण तथा पुराणों का स्थान ग्रहण करती हैं। राम, लक्ष्मण और रावण क्रमशः आठवें बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव के रूप में मान्य हैं । वासुदेव अपने अग्रज बलदेव के साथ मिलकर प्रतिवासुदेव से युद्ध करते हैं और अन्त में प्रतिवासुदेव का वध करते हैं। इसके बाद वह दिग्विजय करके भारत के तीन खण्डों के अधिकारी होते हैं और इस प्रकार अर्द्धभरतेश्वर या अर्द्धचक्रवर्ती बन जाते हैं। यद्यपि वासुदेव मृत्यु के बाद, प्रतिवासुदेव-वध के कारण, नरकगामी होते हैं। नौ वासुदेवों में लक्ष्मण और कृष्ण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 'वसुदेवहिण्डी' में अष्टम वासुदेव लक्ष्मण के द्वारा ही रामण (रावण) का वध दरसाया गया है । प्रतिवासुदेव स्वभावतः वासुदेव के विरोधी के रूप में प्रदर्शित हुए हैं ।
जैन रामकथा की अन्यतम उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें वानर और राक्षस दोनों विद्याधर- वंश की भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं । प्राचीन बौद्धगाथाओं (द्र. जातक : ४३६ तथा ५१०) तथा महाभारत के भी कई स्थलों पर विद्याधर का अर्थ है : आकाशचारी कामरूप ऐन्द्रजालिक । रामायण, महाभारत तथा बृहत्कथामूलक ग्रन्थों, जैसे 'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह', 'वसुदेवहिण्डी', 'बृहत्कथामंजरी' तथा 'कथासरित्सागर' में विद्याधर अलौकिक शक्तियों से विभूषित होने के कारण देवयोनियों के अन्तर्गत रखे गये हैं । 'वसुदेवहिण्डी' ही नहीं, अपितु समग्र जैनकथासाहित्य में विद्याधरों की भूयश: और भूरिशः चर्चा हुई है। हालाँकि, रामायण और महाभारत में विद्याधर किसी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते नहीं दिखाई पड़ते । विभिन्न चमत्कारी विद्याओं
धारण करने के कारण ही इनकी संज्ञा 'विद्याधर' हुई। वानरवंशी विद्याधरों की ध्वजाओं, महलों तथा छतों के शिखर पर वानरों के चिह्न विद्यमान थे, इसीलिए वे वानर कहलाये ।
'बृहत्कथा' में, पात्र - पात्रियों के रूप में विद्याधरों के चित्रण का रहस्य 'कथासरित्सागर' (१.१.४७-४८) में उद्घाटित हुआ है। पार्वती की जिज्ञासा के क्रम में शिव ने कहा कि 'देवि ! देवता सदा सुखी रहते हैं और मनुष्य नित्य दुःखी । इसलिए, उनके चरित्र उत्कृष्ट रूप से मनोहर नहीं होते, इसलिए मैं दिव्य और मानुष दोनों प्रकृतियों से मिश्रित विद्याधरों का चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ।' इस प्रकार, मूल प्रवक्ता शिव के निर्देशानुसार, गुणाढ्य ने अपनी 'बृहत्कथा' में कथारस के परिपाक की दृष्टि से सुख-दुःखमिश्रित प्रकृतिवाले विद्याधरों को ही पात्र - पात्री के रूप में चित्रित किया है। 'वसुदेवहिण्डी' के पात्रों के विद्याधरीकरण में, निश्चय ही, 'बृहत्कथा' की परम्परा का प्रभाव अनुवर्त्तित हुआ है; क्योंकि संघदासगणी के पात्र - पात्रियों की प्रकृति सुख-दुःखमिश्रित है । फिर भी, लक्ष्य करने की बात यह है कि संघदासगणी ने न केवल मिश्रित प्रकृति के विद्याधरों का चित्रण किया है, अपितु मनुष्य और विद्याधरों (अर्द्धदेवों) के जीवन का समीकरण उपन्यस्त किया है।
जैन रामकथा प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं में उपनिबद्ध हुई है । कालक्रमानुसार, प्राकृत में विमलसूरि (ई. के प्रथम शतक से तृतीय- चतुर्थ शतक) का 'पउमचरिय', संस्कृत में रविषेण (सप्तम शतक) का 'पद्मचरित' तथा अपभ्रंश में स्वयम्भू कवि (अष्टम शतक) का 'पउमचरिउ' या 'स्वयम्भूरामायण' जैन रामकथा के विशाल धार्मिक काव्यग्रन्थ हैं। सम्प्रदाय-भेद की दृष्टि से जैनों के श्वेताम्बर - सम्प्रदाय में केवल विमलसूरि की रामकथा का समादर है, परन्तु