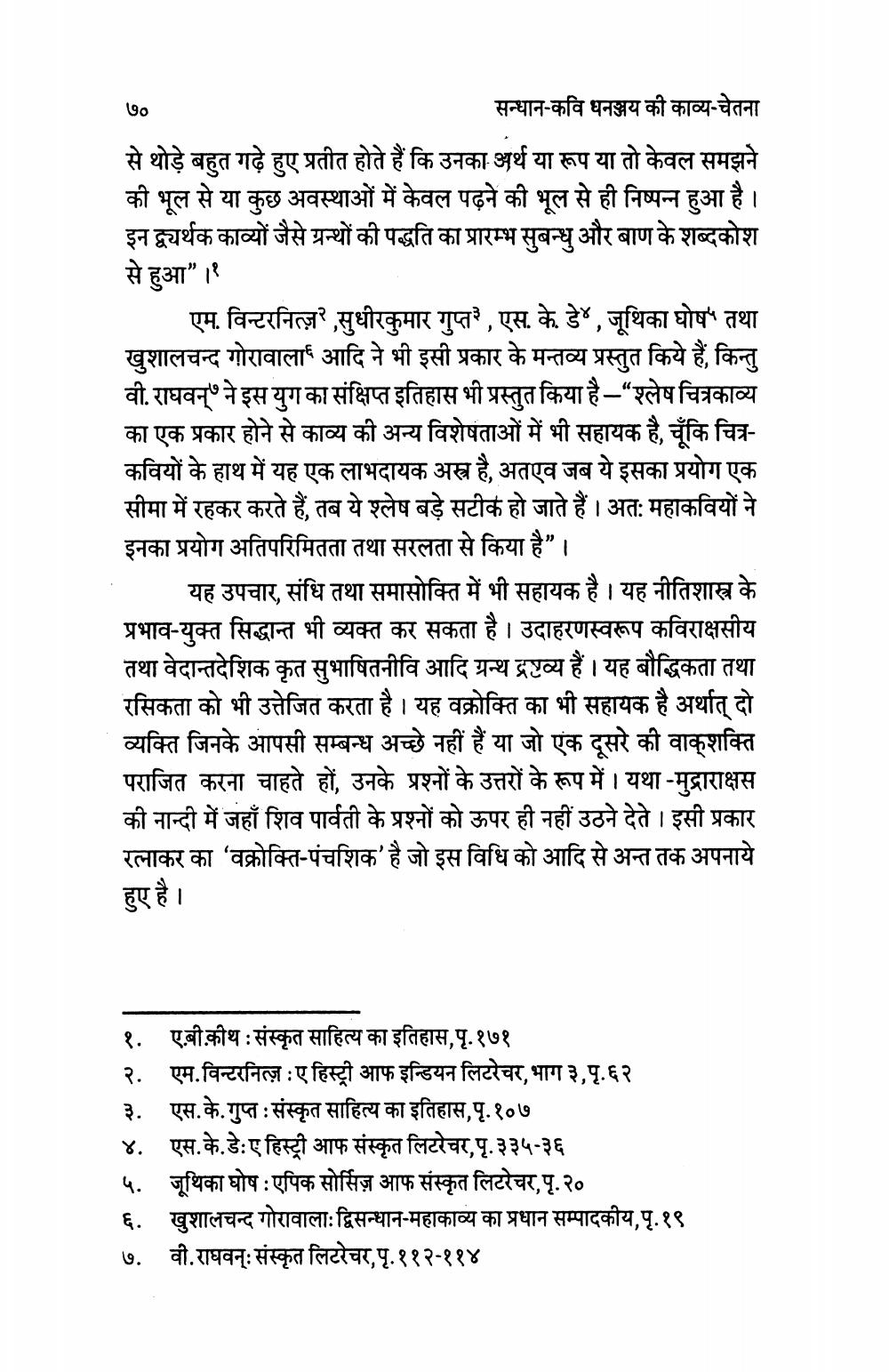________________
सन्धान-कवि धनञ्जय की काव्य-चेतना से थोड़े बहुत गढ़े हुए प्रतीत होते हैं कि उनका अर्थ या रूप या तो केवल समझने की भूल से या कुछ अवस्थाओं में केवल पढ़ने की भूल से ही निष्पन्न हुआ है। इन व्यर्थक काव्यों जैसे ग्रन्थों की पद्धति का प्रारम्भ सुबन्धु और बाण के शब्दकोश से हुआ" ।
एम. विन्टरनित्ज़रे ,सुधीरकुमार गुप्तः, एस. के. डे, जूथिका घोष' तथा खुशालचन्द गोरावाला आदि ने भी इसी प्रकार के मन्तव्य प्रस्तुत किये हैं, किन्तु वी. राघवन् ने इस युग का संक्षिप्त इतिहास भी प्रस्तुत किया है-"श्लेष चित्रकाव्य का एक प्रकार होने से काव्य की अन्य विशेषताओं में भी सहायक है, चूँकि चित्रकवियों के हाथ में यह एक लाभदायक अस्त्र है, अतएव जब ये इसका प्रयोग एक सीमा में रहकर करते हैं, तब ये श्लेष बड़े सटीक हो जाते हैं। अत: महाकवियों ने इनका प्रयोग अतिपरिमितता तथा सरलता से किया है”।
यह उपचार, संधि तथा समासोक्ति में भी सहायक है। यह नीतिशास्त्र के प्रभाव-युक्त सिद्धान्त भी व्यक्त कर सकता है। उदाहरणस्वरूप कविराक्षसीय तथा वेदान्तदेशिक कृत सुभाषितनीवि आदि ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं । यह बौद्धिकता तथा रसिकता को भी उत्तेजित करता है। यह वक्रोक्ति का भी सहायक है अर्थात् दो व्यक्ति जिनके आपसी सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं या जो एक दूसरे की वाक्शक्ति पराजित करना चाहते हों, उनके प्रश्नों के उत्तरों के रूप में । यथा -मुद्राराक्षस की नान्दी में जहाँ शिव पार्वती के प्रश्नों को ऊपर ही नहीं उठने देते । इसी प्रकार रत्नाकर का 'वक्रोक्ति-पंचशिक' है जो इस विधि को आदि से अन्त तक अपनाये हुए है।
१. ए.बी.कीथ : संस्कृत साहित्य का इतिहास,पृ.१७१ २. एम.विन्टरनित्ज़ : ए हिस्ट्री आफ इन्डियन लिटरेचर,भाग ३,पृ.६२ ३. एस.के. गुप्त : संस्कृत साहित्य का इतिहास,पृ.१०७ ४. एस.के.डे: ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर,पृ.३३५-३६ ५. जूथिका घोष : एपिक सोर्सिज़ आफ संस्कृत लिटरेचर,पृ.२० ६. खुशालचन्द गोरावालाःद्विसन्धान-महाकाव्य का प्रधान सम्पादकीय,पृ.१९ ७. वी.राघवनःसंस्कृत लिटरेचर,पृ.११२-११४