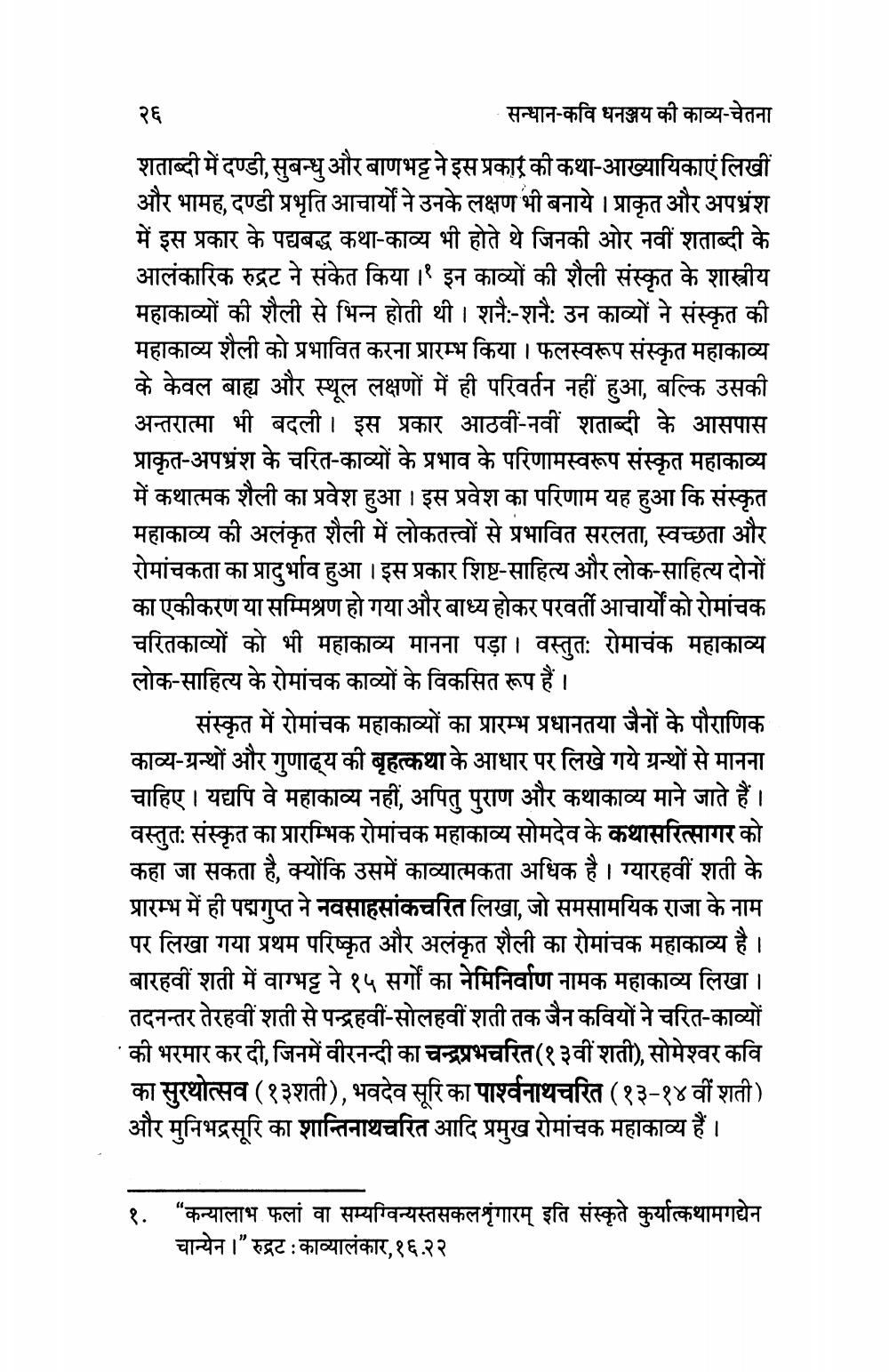________________
सन्धान-कवि धनञ्जय की काव्य-चेतना शताब्दी में दण्डी, सुबन्धु और बाणभट्ट ने इस प्रकार की कथा-आख्यायिकाएं लिखीं
और भामह, दण्डी प्रभृति आचार्यों ने उनके लक्षण भी बनाये । प्राकृत और अपभ्रंश में इस प्रकार के पद्यबद्ध कथा-काव्य भी होते थे जिनकी ओर नवीं शताब्दी के आलंकारिक रुद्रट ने संकेत किया। इन काव्यों की शैली संस्कृत के शास्त्रीय महाकाव्यों की शैली से भिन्न होती थी। शनै:-शनै: उन काव्यों ने संस्कृत की महाकाव्य शैली को प्रभावित करना प्रारम्भ किया। फलस्वरूप संस्कृत महाकाव्य के केवल बाह्य और स्थूल लक्षणों में ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि उसकी अन्तरात्मा भी बदली। इस प्रकार आठवीं-नवीं शताब्दी के आसपास प्राकृत-अपभ्रंश के चरित-काव्यों के प्रभाव के परिणामस्वरूप संस्कृत महाकाव्य में कथात्मक शैली का प्रवेश हुआ। इस प्रवेश का परिणाम यह हुआ कि संस्कृत महाकाव्य की अलंकृत शैली में लोकतत्त्वों से प्रभावित सरलता, स्वच्छता और रोमांचकता का प्रादुर्भाव हुआ । इस प्रकार शिष्ट-साहित्य और लोक-साहित्य दोनों का एकीकरण या सम्मिश्रण हो गया और बाध्य होकर परवर्ती आचार्यों को रोमांचक चरितकाव्यों को भी महाकाव्य मानना पड़ा। वस्तुत: रोमाचंक महाकाव्य लोक-साहित्य के रोमांचक काव्यों के विकसित रूप हैं।
संस्कृत में रोमांचक महाकाव्यों का प्रारम्भ प्रधानतया जैनों के पौराणिक काव्य-ग्रन्थों और गुणाढ्य की बृहत्कथा के आधार पर लिखे गये ग्रन्थों से मानना चाहिए। यद्यपि वे महाकाव्य नहीं, अपितु पुराण और कथाकाव्य माने जाते हैं। वस्तुत: संस्कृत का प्रारम्भिक रोमांचक महाकाव्य सोमदेव के कथासरित्सागर को कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें काव्यात्मकता अधिक है। ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ में ही पद्मगुप्त ने नवसाहसांकचरित लिखा, जो समसामयिक राजा के नाम पर लिखा गया प्रथम परिष्कृत और अलंकृत शैली का रोमांचक महाकाव्य है। बारहवीं शती में वाग्भट्ट ने १५ सर्गों का नेमिनिर्वाण नामक महाकाव्य लिखा। तदनन्तर तेरहवीं शती से पन्द्रहवीं-सोलहवीं शती तक जैन कवियों ने चरित-काव्यों 'की भरमार कर दी, जिनमें वीरनन्दी का चन्द्रप्रभचरित(१३वीं शती), सोमेश्वर कवि का सुरथोत्सव (१३शती), भवदेव सूरि का पार्श्वनाथचरित (१३-१४ वीं शती) और मुनिभद्रसूरि का शान्तिनाथचरित आदि प्रमुख रोमांचक महाकाव्य हैं।
१. “कन्यालाभ फलां वा सम्यग्विन्यस्तसकलशृंगारम् इति संस्कृते कुर्यात्कथामगद्येन
चान्येन ।” रुद्रट : काव्यालंकार,१६.२२