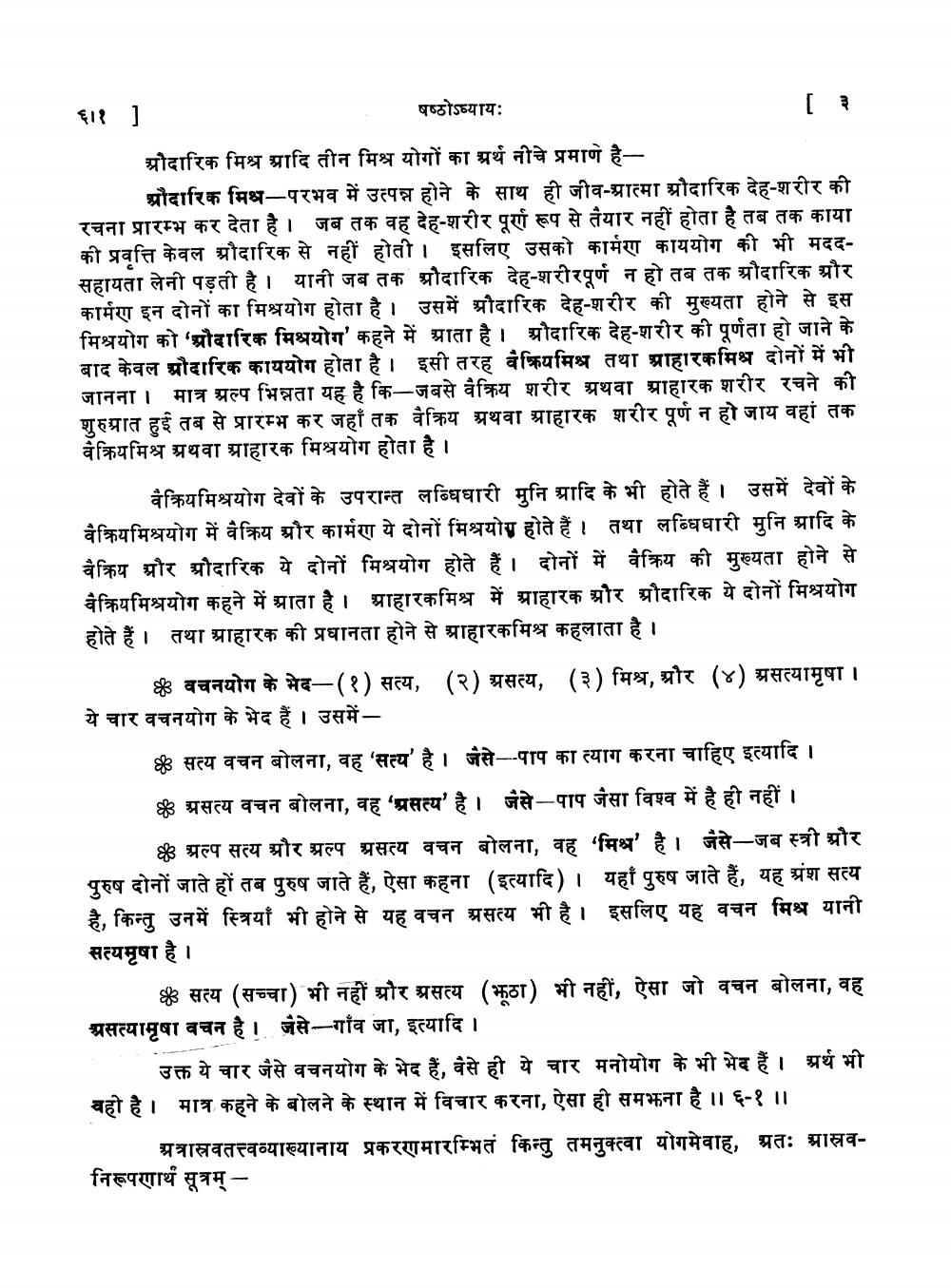________________
षष्ठोऽध्यायः
दारिक मिश्र आदि तीन मिश्र योगों का अर्थ नीचे प्रमाणे है -
श्रदारिक मिश्र - परभव में उत्पन्न होने के साथ ही जीव- श्रात्मा श्रदारिक देह शरीर की रचना प्रारम्भ कर देता है । जब तक वह देह शरीर पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है तब तक काया की प्रवृत्ति केवल प्रदारिक से नहीं होती । इसलिए उसको कार्मरण काययोग की भी मदद - सहायता लेनी पड़ती है। यानी जब तक प्रौदारिक देह शरीरपूर्ण न हो तब तक प्रौदारिक और कारण इन दोनों का मिश्रयोग होता है । उसमें प्रौदारिक देह शरीर की मुख्यता होने से इस मिश्रयोग को 'दारिक मिश्रयोग' कहने में आता है । प्रौदारिक देह शरीर की पूर्णता हो जाने के बाद केवल औदारिक काययोग होता है । इसी तरह वैक्रियमिश्र तथा श्राहारकमिश्र दोनों में भी जानना । मात्र अल्प भिन्नता यह है कि - जबसे वैक्रिय शरीर अथवा श्राहारक शरीर रचने की शुरुप्रात हुई तब से प्रारम्भ कर जहाँ तक वैक्रिय अथवा प्रहारक शरीर पूर्ण न हो जाय वहां तक वैक्रियमिश्र अथवा श्राहारक मिश्रयोग होता है ।
६।१]
वैक्रियमिश्रयोग देवों के उपरान्त लब्धिधारी मुनि आदि के भी होते हैं । उसमें देवों के वैयमिश्रयोग में वैक्रिय और कार्मण ये दोनों मिश्रयोग होते हैं । तथा लब्धिधारी मुनि आदि के वैक्रिय और श्रदारिक ये दोनों मिश्रयोग होते हैं। दोनों में वैक्रिय की मुख्यता होने से मिश्रयोग कहने में आता है । आहारकमिश्र में आहारक और प्रौदारिक ये दोनों मिश्रयोग होते हैं । तथा प्रहारक की प्रधानता होने से आहारकमिश्र कहलाता है ।
( २ ) असत्य, (३) मिश्र, और ( ४ ) असत्यामृषा ।
* वचनयोग के भेद - ( १ ) सत्य,
[ ३
ये चार वचनयोग के भेद हैं । उसमें —
* सत्य वचन बोलना, वह 'सत्य' है । जैसे - पाप का त्याग करना चाहिए इत्यादि । * असत्य वचन बोलना, वह 'असत्य' है । जैसे- पाप जैसा विश्व में है ही नहीं ।
* अल्प सत्य और अल्प असत्य वचन बोलना, वह पुरुष दोनों जाते हों तब पुरुष जाते हैं, ऐसा कहना ( इत्यादि) । है, किन्तु उनमें स्त्रियाँ भी होने से यह वचन असत्य भी है । सत्यमृषा है ।
'मिश्र' है । जैसे—जब स्त्री और
यहाँ पुरुष जाते हैं, यह अंश सत्य इसलिए यह वचन मिश्र यानी
* सत्य ( सच्चा ) भी नहीं और असत्य ( झूठा ) भी नहीं, ऐसा जो वचन बोलना, वह । जैसे - गाँव जा, इत्यादि । असत्यामृषा वचन
वही है ।
उक्त ये चार जैसे वचनयोग के भेद हैं, वैसे ही ये चार मनोयोग के भी भेद हैं । अर्थ भी मात्र कहने के बोलने के स्थान में विचार करना, ऐसा ही समझना है ।। ६-१ ।। अत्रास्रवतत्त्वव्याख्यानाय प्रकरणमारम्भितं किन्तु तमनुक्त्वा योगमेवाह, अतः प्रास्रवनिरूपणार्थं सूत्रम् –