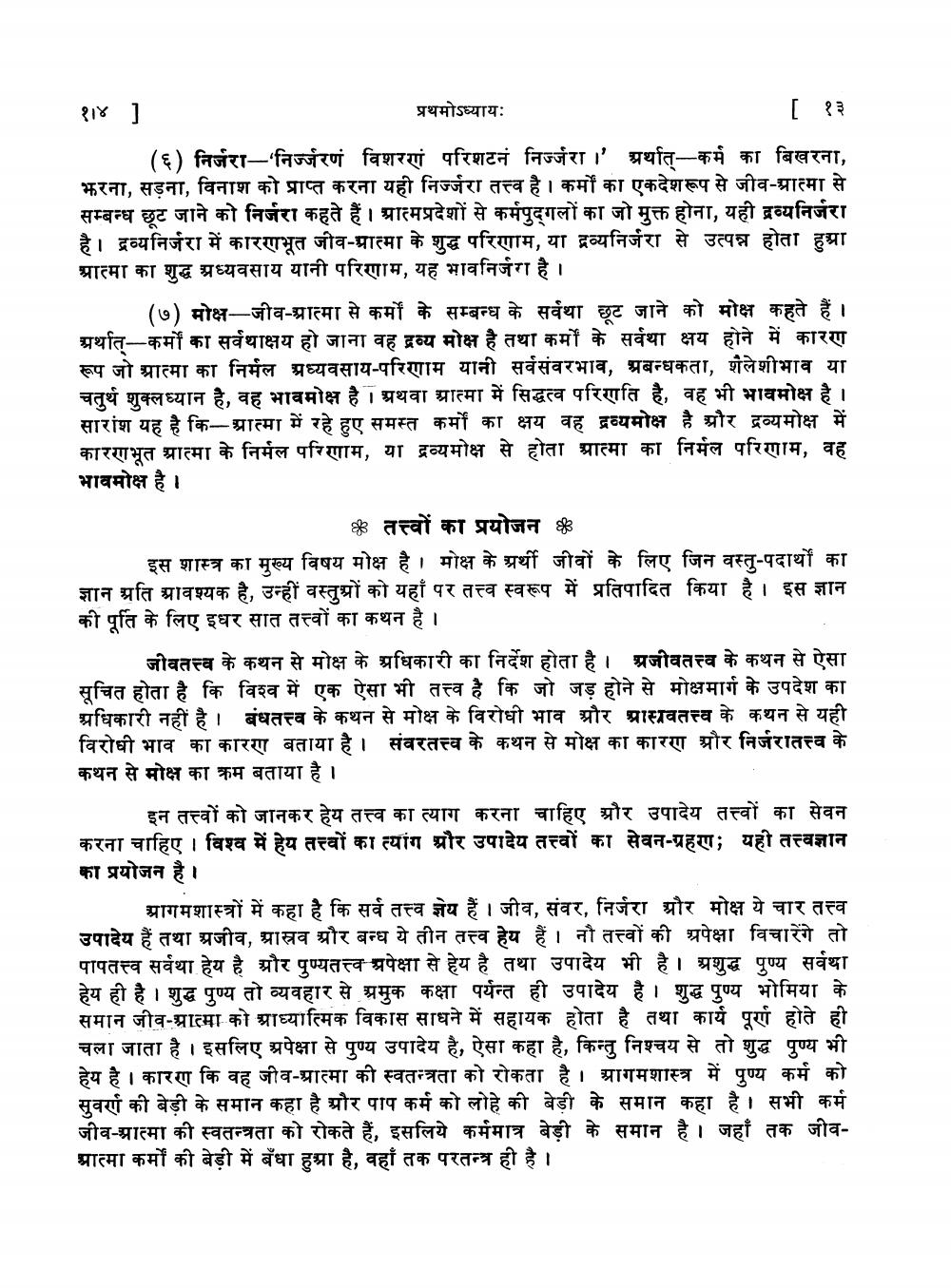________________
१।४ ]
प्रथमोऽध्यायः
[ १३
(६) निर्जरा - निर्जरणं विशरणं परिशटनं निर्जरा ।' अर्थात् - कर्म का बिखरना, भरना, सड़ना, विनाश को प्राप्त करना यही निर्जरा तत्त्व है । कर्मों का एकदेशरूप से जीव- श्रात्मा से सम्बन्ध छूट जाने को निर्जरा कहते हैं । श्रात्मप्रदेशों से कर्मपुद्गलों का जो मुक्त होना, यही द्रव्यनिर्जरा है । द्रव्यनिर्जरा में काररणभूत जीव-प्रात्मा के शुद्ध परिणाम, या द्रव्यनिर्जरा से उत्पन्न होता हुआ आत्मा का शुद्ध अध्यवसाय यानी परिणाम, यह भावनिर्जरा है ।
(७) मोक्ष - जीव - प्रात्मा से कर्मों के सम्बन्ध के सर्वथा छूट जाने को मोक्ष कहते हैं । अर्थात् - कर्मों का सर्वथाक्षय हो जाना वह द्रव्य मोक्ष है तथा कर्मों के सर्वथा क्षय होने में कारण रूप जो आत्मा का निर्मल अध्यवसाय - परिणाम यानी सर्वसंवरभाव, श्रबन्धकता, शैलेशीभाव या चतुर्थ शुक्लध्यान है, वह भावमोक्ष है । अथवा आत्मा में सिद्धत्व परिणति है, वह भी भावमोक्ष है । सारांश यह है कि आत्मा में रहे हुए समस्त कर्मों का क्षय वह द्रव्यमोक्ष है और द्रव्यमोक्ष में कारणभूत आत्मा के निर्मल परिणाम, या द्रव्यमोक्ष से होता आत्मा का निर्मल परिणाम, वह भावमोक्ष है ।
* तत्त्वों का प्रयोजन
इस शास्त्र का मुख्य विषय मोक्ष है । मोक्ष के अर्थी जीवों के लिए जिन वस्तु-पदार्थों का ज्ञान प्रति आवश्यक है, उन्हीं वस्तुनों को यहाँ पर तत्त्व स्वरूप में प्रतिपादित किया है। इस ज्ञान की पूर्ति के लिए इधर सात तत्त्वों का कथन है ।
जीवत्व के कथन से मोक्ष के अधिकारी का निर्देश होता है । श्रजीवतत्त्व के कथन से ऐसा सूचित होता है कि विश्व में एक ऐसा भी तत्त्व है कि जो जड़ होने से मोक्षमार्ग के उपदेश का अधिकारी नहीं है । बंधतत्त्व के कथन से मोक्ष के विरोधी भाव और प्रास्वतत्त्व के कथन से यही विरोधी भाव का कारण बताया है । संवरतत्त्व के कथन से मोक्ष का कारण और निर्जरातत्त्व के कथन से मोक्ष का क्रम बताया है ।
इन तत्त्वों को जानकर हेय तत्त्व का त्याग करना चाहिए और उपादेय तत्त्वों का सेवन करना चाहिए । विश्व में हेय तत्त्वों का त्याग और उपादेय तत्त्वों का सेवन-ग्रहण; यही तत्त्वज्ञान का प्रयोजन है ।
आगमशास्त्रों में कहा है कि सर्व तत्त्व ज्ञेय हैं। जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये चार तत्त्व उपादेय हैं तथा जीव, प्रास्रव और बन्ध ये तीन तत्त्व हेय हैं। नौ तत्त्वों की अपेक्षा विचारेंगे तो पापतत्त्व सर्वथा हेय है और पुण्यतत्त्व अपेक्षा से हेय है तथा उपादेय भी है । अशुद्ध पुण्य सर्वथा यही है । शुद्ध पुण्य तो व्यवहार से अमुक कक्षा पर्यन्त ही उपादेय है । शुद्ध पुण्य भोमिया के समान जीव- श्रात्मा को आध्यात्मिक विकास साधने में सहायक होता है तथा कार्य पूर्ण होते ही चला जाता है । इसलिए अपेक्षा से पुण्य उपादेय है, ऐसा कहा है, किन्तु निश्चय से तो शुद्ध पुण्य भी है है । कारण कि वह जीव- श्रात्मा की स्वतन्त्रता को रोकता है। श्रागमशास्त्र में पुण्य कर्म को सुवर्ण की बेड़ी के समान कहा है और पाप कर्म को लोहे की बेड़ी के समान कहा है। सभी कर्म जीव आत्मा की स्वतन्त्रता को रोकते हैं, इसलिये कर्ममात्र बेड़ी के समान है । जहाँ तक जीवश्रात्मा कर्मों की बेड़ी में बँधा हुआ है, वहाँ तक परतन्त्र ही है ।