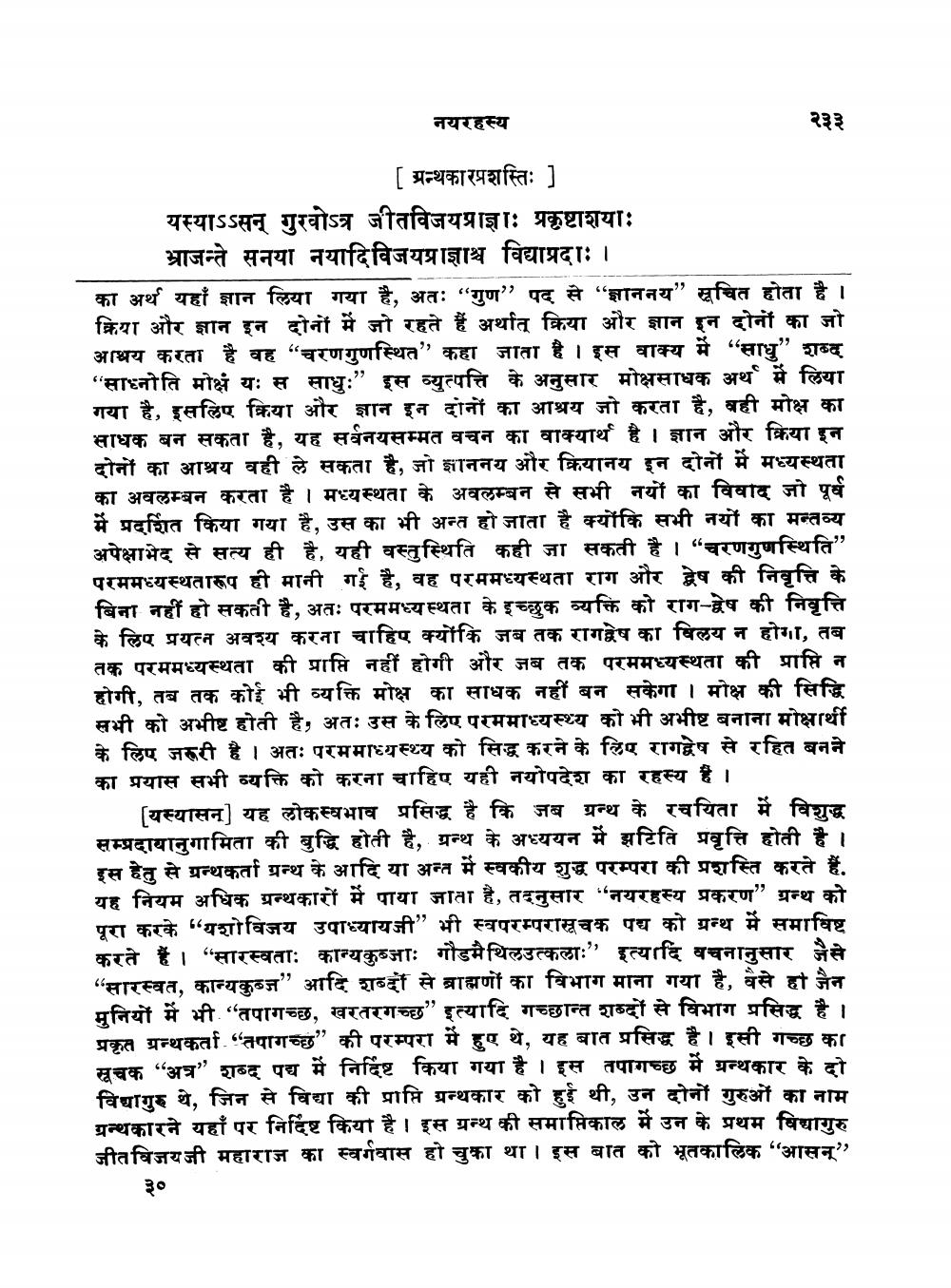________________
नयरहस्य
२३३
[ ग्रन्थकारप्रशस्तिः ] यस्याऽऽसन् गुरवोऽत्र जीतविजयप्राज्ञाः प्रकृष्टाशयाः
भ्राजन्ते सनया नयादिविजयप्राज्ञाश्च विद्याप्रदाः । का अर्थ यहाँ ज्ञान लिया गया है, अतः "गुण" पद से "ज्ञाननय” सूचित होता है । क्रिया और ज्ञान इन दोनों में जो रहते हैं अर्थात् क्रिया और ज्ञान इन दोनों का जो आश्रय करता है वह “चरणगुणस्थित' कहा जाता है । इस वाक्य में “साधु" शब्द "साध्नोति मोक्षं यः स साधुः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार मोक्षसाधक अर्थ में लिया गया है, इसलिए क्रिया और ज्ञान इन दोनों का आश्रय जो करता है, वही मोक्ष का साधक बन सकता है, यह सर्वनयसम्मत वचन का वाक्यार्थ है । ज्ञान और क्रिया इन दोनों का आश्रय वही ले सकता है, जो ज्ञाननय और क्रियानय इन दोनों में मध्यस्थता का अवलम्बन करता है । मध्यस्थता के अवलम्बन से सभी नयों का विवाद जो पूर्व में प्रदर्शित किया गया है, उस का भी अन्त हो जाता है क्योंकि सभी नयों का मन्तव्य अपेक्षाभेद से सत्य ही है, यही वस्तुस्थिति कही जा सकती है । "चरणगुणस्थिति" परममध्यस्थतारूप ही मानी गई है, वह परममध्यस्थता राग और द्वेष की निवृत्ति के बिना नहीं हो सकती है, अतः परममध्यस्थता के इच्छुक व्यक्ति को राग-द्वेष की निवृत्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए क्योंकि जब तक रागद्वेष का विलय न होगा, तब तक परममध्यस्थता की प्राप्ति नहीं होगी और जब तक परममध्यस्थता की प्राप्ति न होगी, तब तक कोई भी व्यक्ति मोक्ष का साधक नहीं बन सकेगा। मोक्ष की सिद्धि सभी को अभीष्ट होती है, अतः उस के लिए परममाध्यस्थ्य को भी अभीष्ट बनाना मोक्षार्थी के लिए जरूरी है। अतः परममाध्यस्थ्य को सिद्ध करने के लिए रागद्वेष से रहित बनने का प्रयास सभी व्यक्ति को करना चाहिए यही नयोपदेश का रहस्य है।
यस्यासन यह लोकस्वभाव प्रसिद्ध है कि जब ग्रन्थ के रचयिता में विशुद्ध सम्प्रदायानुगामिता की बुद्धि होती है, ग्रन्थ के अध्ययन में झटिति प्रवृत्ति होती है। इस हेतु से ग्रन्थकर्ता ग्रन्थ के आदि या अन्त में स्वकीय शुद्ध परम्परा की प्रशस्ति करते हैं. यह नियम अधिक ग्रन्थकारों में पाया जाता है, तदनुसार “नयरहस्य प्रकरण” ग्रन्थ को पूरा करके "यशोविजय उपाध्यायजी” भी स्वपरम्परासूचक पद्य को ग्रन्थ में समाविष्ट करते हैं । “सारस्वता: कान्यकुब्जाः गौडमैथिलउत्कलाः' इत्यादि वचनानुसार जैसे "सारस्वत, कान्यकुब्ज” आदि शब्दों से ब्राह्मणों का विभाग माना गया है, वैसे ही जैन
भी “तपागच्छ, खरतरगच्छ” इत्यादि गच्छान्त शब्दों से विभाग प्रसिद्ध है। प्रकृत ग्रन्थकर्ता “तपागच्छ” की परम्परा में हुए थे, यह बात प्रसिद्ध है। इसी गच्छ का सूचक “अत्र" शब्द पद्य में निर्दिष्ट किया गया है । इस तपागच्छ में ग्रन्थकार के दो विद्यागुरु थे, जिन से विद्या की प्राप्ति ग्रन्थकार को हुई थी, उन दोनों गुरुओं का नाम ग्रन्थकारने यहाँ पर निर्दिष्ट किया है। इस ग्रन्थ की समाप्तिकाल में उन के प्रथम विद्यागुरु जीतविजयजी महाराज का स्वर्गवास हो चुका था। इस बात को भूतकालिक "आसन्"