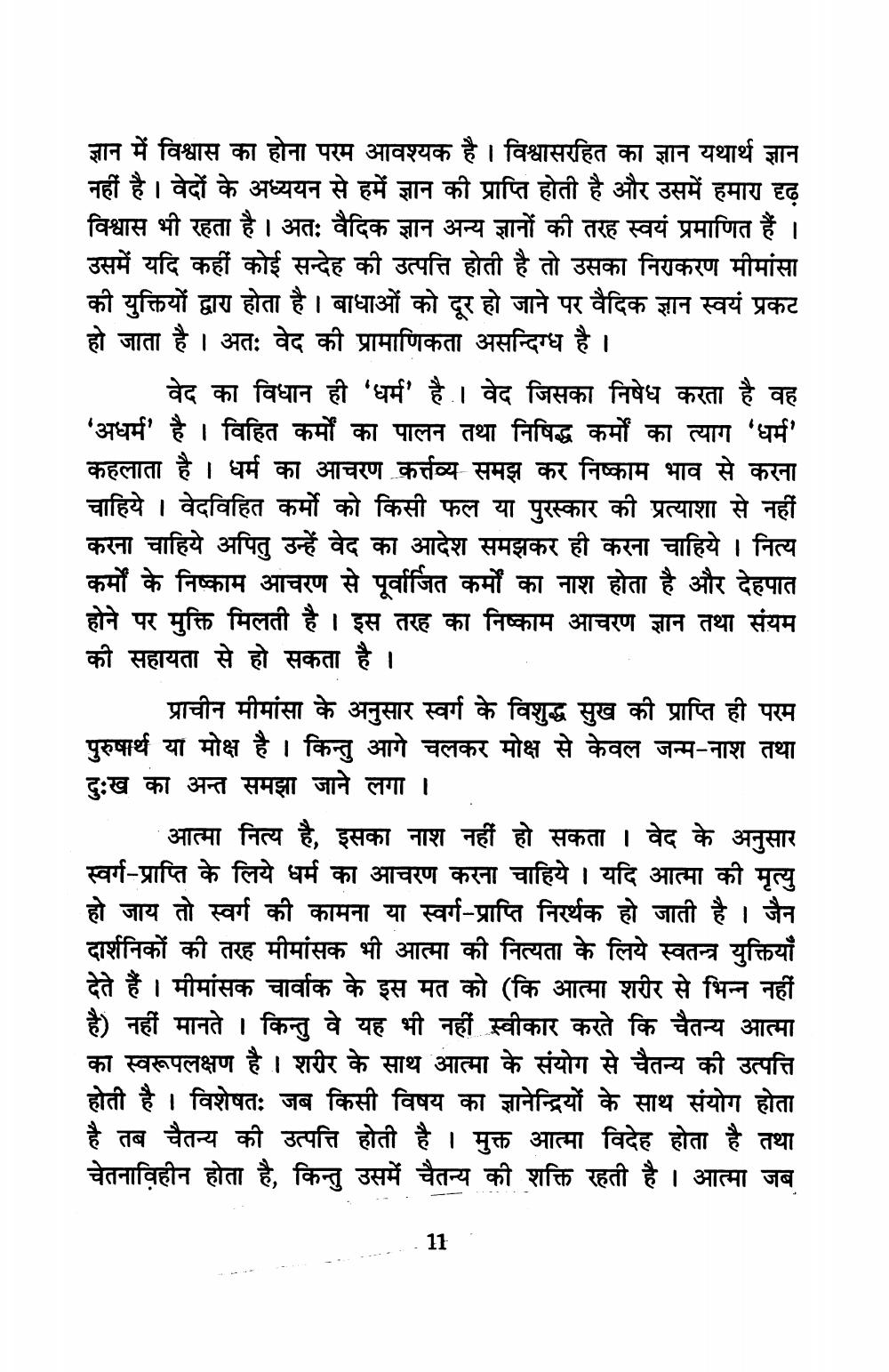________________
ज्ञान में विश्वास का होना परम आवश्यक है । विश्वासरहित का ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है । वेदों के अध्ययन से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसमें हमारा दृढ़ विश्वास भी रहता है। अतः वैदिक ज्ञान अन्य ज्ञानों की तरह स्वयं प्रमाणित हैं । उसमें यदि कहीं कोई सन्देह की उत्पत्ति होती है तो उसका निराकरण मीमांसा की युक्तियों द्वारा होता है। बाधाओं को दूर हो जाने पर वैदिक ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। अतः वेद की प्रामाणिकता असन्दिग्ध है।
वेद का विधान ही 'धर्म' है । वेद जिसका निषेध करता है वह 'अधर्म' है । विहित कर्मों का पालन तथा निषिद्ध कर्मों का त्याग 'धर्म' कहलाता है । धर्म का आचरण कर्तव्य समझ कर निष्काम भाव से करना चाहिये । वेदविहित कर्मों को किसी फल या पुरस्कार की प्रत्याशा से नहीं करना चाहिये अपितु उन्हें वेद का आदेश समझकर ही करना चाहिये । नित्य कर्मों के निष्काम आचरण से पूर्वार्जित कर्मों का नाश होता है और देहपात होने पर मुक्ति मिलती है । इस तरह का निष्काम आचरण ज्ञान तथा संयम की सहायता से हो सकता है ।
___ प्राचीन मीमांसा के अनुसार स्वर्ग के विशुद्ध सुख की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ या मोक्ष है । किन्तु आगे चलकर मोक्ष से केवल जन्म-नाश तथा दुःख का अन्त समझा जाने लगा ।
आत्मा नित्य है, इसका नाश नहीं हो सकता । वेद के अनुसार स्वर्ग-प्राप्ति के लिये धर्म का आचरण करना चाहिये । यदि आत्मा की मृत्यु हो जाय तो स्वर्ग की कामना या स्वर्ग-प्राप्ति निरर्थक हो जाती है। जैन दार्शनिकों की तरह मीमांसक भी आत्मा की नित्यता के लिये स्वतन्त्र युक्तियाँ देते हैं । मीमांसक चार्वाक के इस मत को (कि आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है) नहीं मानते । किन्तु वे यह भी नहीं स्वीकार करते कि चैतन्य आत्मा का स्वरूपलक्षण है। शरीर के साथ आत्मा के संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति होती है । विशेषतः जब किसी विषय का ज्ञानेन्द्रियों के साथ संयोग होता है तब चैतन्य की उत्पत्ति होती है । मुक्त आत्मा विदेह होता है तथा चेतनाविहीन होता है, किन्तु उसमें चैतन्य की शक्ति रहती है । आत्मा जब
.......................... 11