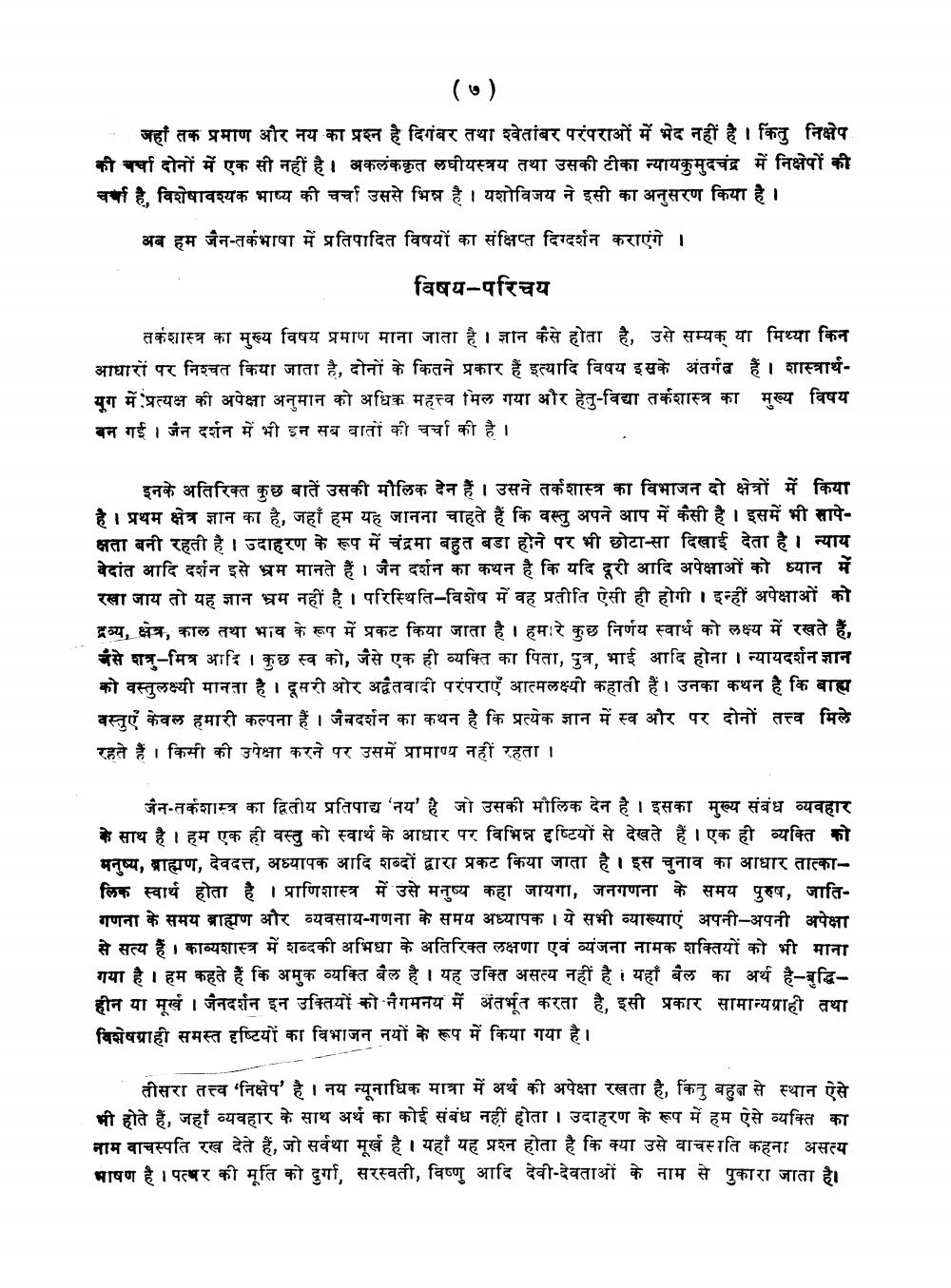________________
(७)
- जहाँ तक प्रमाण और नय का प्रश्न है दिगंबर तथा श्वेतांबर परंपराओं में भेद नहीं है। किंतु निक्षेप की चर्चा दोनों में एक सी नहीं है। अकलंककृत लघीयस्त्रय तथा उसकी टीका न्यायकुमुदचंद्र में निक्षेपों की चर्चा है. विशेषावश्यक भाष्य की चर्चा उससे भिन्न है। यशोविजय ने इसी का अनुसरण किया है।
अब हम जैन-तर्कभाषा में प्रतिपादित विषयों का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराएंगे ।
विषय-परिचय
तर्कशास्त्र का मुख्य विषय प्रमाण माना जाता है। ज्ञान कैसे होता है, उसे सम्यक् या मिथ्या किन आधारों पर निश्चत किया जाता है, दोनों के कितने प्रकार हैं इत्यादि विषय इसके अंतर्गत हैं। शास्त्रार्थयुग में प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान को अधिक महत्त्व मिल गया और हेतु-विद्या तर्कशास्त्र का मुख्य विषय बन गई। जैन दर्शन में भी इन सब बातों की चर्चा की है।
इनके अतिरिक्त कुछ बातें उसकी मौलिक देन हैं। उसने तर्कशास्त्र का विभाजन दो क्षेत्रों में किया है। प्रथम क्षेत्र ज्ञान का है, जहाँ हम यह जानना चाहते हैं कि वस्तु अपने आप में कैसी है। इसमें भी सापेक्षता बनी रहती है। उदाहरण के रूप में चंद्रमा बहुत बडा होने पर भी छोटा-सा दिखाई देता है। न्याय वेदांत आदि दर्शन इसे भ्रम मानते हैं। जैन दर्शन का कथन है कि यदि दूरी आदि अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाय तो यह ज्ञान भ्रम नहीं है। परिस्थिति-विशेष में वह प्रतीति ऐसी ही होगी। इन्हीं अपेक्षाओं को द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव के रूप में प्रकट किया जाता है। हमारे कुछ निर्णय स्वार्थ को लक्ष्य में रखते हैं,
से शत्रु-मित्र आदि । कुछ स्व को, जैसे एक ही व्यक्ति का पिता, पुत्र, भाई आदि होना । न्यायदर्शन ज्ञान को वस्तुलक्ष्यी मानता है । दूसरी ओर अद्वैतवादी परंपराएँ आत्मलक्ष्यो कहाती हैं। उनका कथन है कि बाह्य वस्तुएँ केवल हमारी कल्पना हैं । जैवदर्शन का कथन है कि प्रत्येक ज्ञान में स्व और पर दोनों तत्त्व मिले रहते हैं। किसी की उपेक्षा करने पर उसमें प्रामाण्य नहीं रहता।
जैन-तर्कशास्त्र का द्वितीय प्रतिपाद्य 'नय' है जो उसकी मौलिक देन है। इसका मुख्य संबंध व्यवहार के साथ है। हम एक ही वस्तु को स्वार्थ के आधार पर विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं । एक ही व्यक्ति को मनुष्य, ब्राह्मण, देवदत्त, अध्यापक आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। इस चुनाव का आधार तात्कालिक स्वार्थ होता है । प्राणिशास्त्र में उसे मनुष्य कहा जायगा, जनगणना के समय पुरुष, जातिगणना के समय ब्राह्मण और व्यवसाय-गणना के समय अध्यापक । ये सभी व्याख्याएं अपनी-अपनी अपेक्षा से सत्य हैं। काव्यशास्त्र में शब्दकी अभिधा के अतिरिक्त लक्षणा एवं व्यंजना नामक शक्तियों को भी माना गया है । हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बैल है । यह उक्ति असत्य नहीं है। यहाँ बैल का अर्थ है-बुद्धिहीन या मूर्ख । जैनदर्शन इन उक्तियों को नैगमनय में अंतर्भूत करता है, इसी प्रकार सामान्यग्राही तथा विशेषग्राही समस्त दृष्टियों का विभाजन नयों के रूप में किया गया है।
तीसरा तत्त्व 'निक्षेप' है । नय न्यूनाधिक मात्रा में अर्थ की अपेक्षा रखता है, किंतु बहुत से स्थान ऐसे भी होते हैं, जहाँ व्यवहार के साथ अर्थ का कोई संबंध नहीं होता । उदाहरण के रूप में हम ऐसे व्यक्ति का नाम वाचस्पति रख देते हैं, जो सर्वथा मूर्ख है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि क्या उसे वाचसति कहना असत्य भाषण है । पत्थर की मूर्ति को दुर्गा, सरस्वती, विष्णु आदि देवी-देवताओं के नाम से पुकारा जाता है।