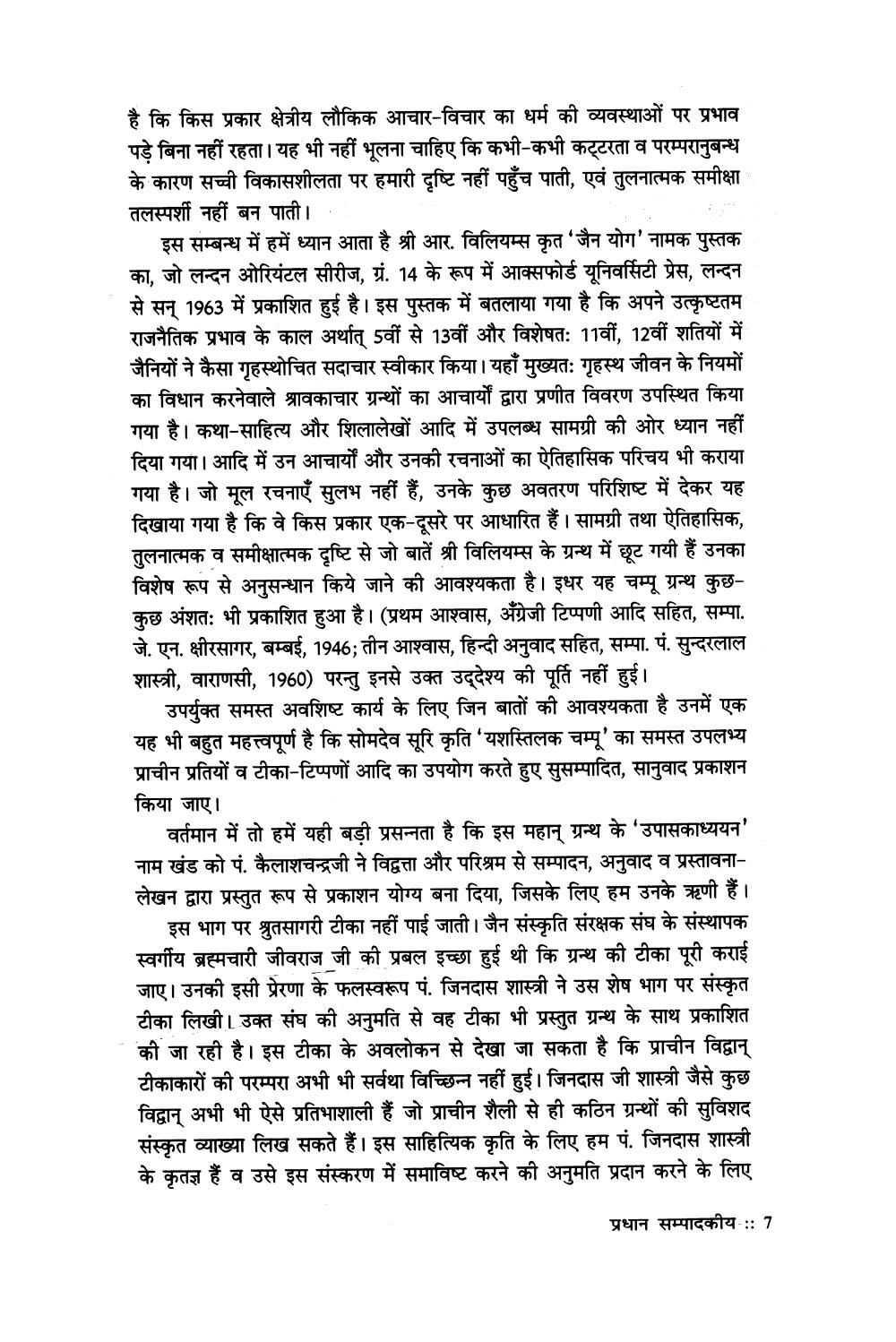________________
है कि किस प्रकार क्षेत्रीय लौकिक आचार-विचार का धर्म की व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी-कभी कट्टरता व परम्परानुबन्ध कारण सच्ची विकासशीलता पर हमारी दृष्टि नहीं पहुँच पाती, एवं तुलनात्मक समीक्षा तलस्पर्शी नहीं बन पाती ।
इस सम्बन्ध में हमें ध्यान आता है श्री आर. विलियम्स कृत 'जैन योग' नामक पुस्तक का, जो लन्दन ओरियंटल सीरीज, ग्रं. 14 के रूप में आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन
सन् 1963 में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में बतलाया गया है कि अपने उत्कृष्टतम राजनैतिक प्रभाव के काल अर्थात् 5वीं से 13वीं और विशेषतः 11वीं, 12वीं शतियों में जैनियों ने कैसा गृहस्थोचित सदाचार स्वीकार किया । यहाँ मुख्यतः गृहस्थ जीवन के नियमों का विधान करनेवाले श्रावकाचार ग्रन्थों का आचार्यों द्वारा प्रणीत विवरण उपस्थित किया गया है। कथा - साहित्य और शिलालेखों आदि में उपलब्ध सामग्री की ओर ध्यान नहीं दिया गया । आदि में उन आचार्यों और उनकी रचनाओं का ऐतिहासिक परिचय भी कराया गया है। जो मूल रचनाएँ सुलभ नहीं हैं, उनके कुछ अवतरण परिशिष्ट में देकर यह दिखाया गया है कि वे किस प्रकार एक-दूसरे पर आधारित हैं। सामग्री तथा ऐतिहासिक, तुलनात्मक व समीक्षात्मक दृष्टि से जो बातें श्री विलियम्स के ग्रन्थ में छूट गयी हैं उनका विशेष रूप से अनुसन्धान किये जाने की आवश्यकता है। इधर यह चम्पू ग्रन्थ कुछकुछ अंशत: भी प्रकाशित हुआ है। (प्रथम आश्वास, अँग्रेजी टिप्पणी आदि सहित, सम्पा. जे. एन. क्षीरसागर, बम्बई, 1946; तीन आश्वास, हिन्दी अनुवाद सहित, सम्पा. पं. सुन्दरलाल शास्त्री, वाराणसी, 1960) परन्तु इनसे उक्त उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई ।
उपर्युक्त समस्त अवशिष्ट कार्य के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उनमें एक यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण है कि सोमदेव सूरि कृति 'यशस्तिलक चम्पू' का समस्त उपलभ्य प्राचीन प्रतियों व टीका-टिप्पणों आदि का उपयोग करते हुए सुसम्पादित, सानुवाद प्रकाशन किया जाए।
वर्तमान में तो हमें यही बड़ी प्रसन्नता है कि इस महान् ग्रन्थ के 'उपासकाध्ययन' नाम खंड को पं. कैलाशचन्द्रजी ने विद्वत्ता और परिश्रम से सम्पादन, अनुवाद व प्रस्तावनालेखन द्वारा प्रस्तुत रूप से प्रकाशन योग्य बना दिया, जिसके लिए हम उनके ऋणी हैं।
इस भाग पर श्रुतसागरी टीका नहीं पाई जाती। जैन संस्कृति संरक्षक संघ के संस्थापक स्वर्गीय ब्रह्मचारी जीवराज जी की प्रबल इच्छा हुई थी कि ग्रन्थ की टीका पूरी कराई जाए। उनकी इसी प्रेरणा के फलस्वरूप पं. जिनदास शास्त्री ने उस शेष भाग पर संस्कृत टीका लिखी। उक्त संघ की अनुमति से वह टीका भी प्रस्तुत ग्रन्थ के साथ प्रकाशित की जा रही है। इस टीका के अवलोकन से देखा जा सकता है कि प्राचीन विद्वान् टीकाकारों की परम्परा अभी भी सर्वथा विच्छिन्न नहीं हुई। जिनदास जी शास्त्री जैसे कुछ विद्वान् अभी भी ऐसे प्रतिभाशाली हैं जो प्राचीन शैली से ही कठिन ग्रन्थों की सुविशद संस्कृत व्याख्या लिख सकते हैं। इस साहित्यिक कृति के लिए हम पं. जिनदास शास्त्री के कृतज्ञ हैं व उसे इस संस्करण में समाविष्ट करने की अनुमति प्रदान करने के लिए
प्रधान सम्पादकीय :: 7