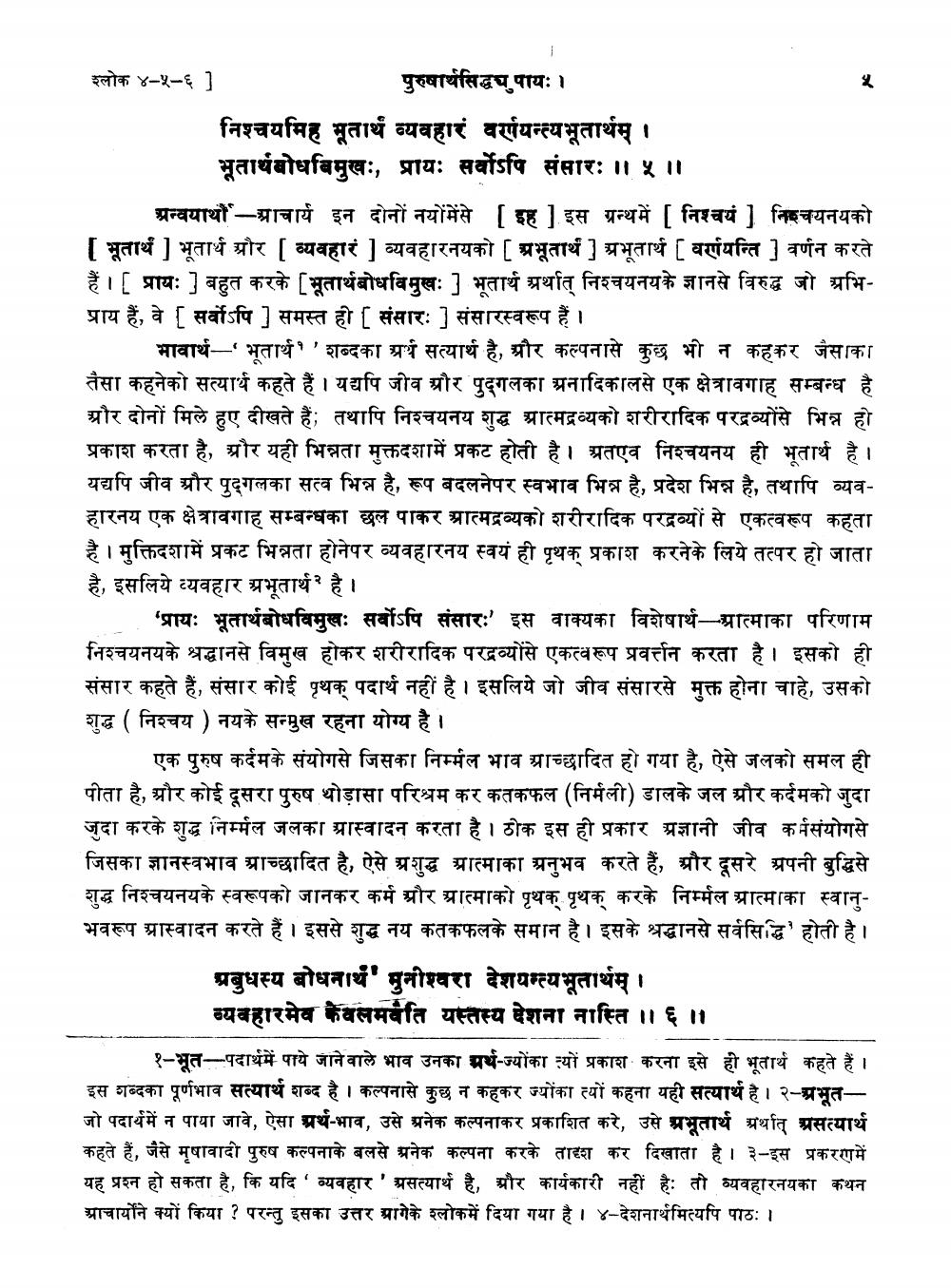________________
श्लोक ४-५-६ ]
पुरुषार्थसिद्धघु पायः। निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम् ।
भूतार्थबोधबिमुखः, प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥ ५ ॥ अन्वयार्थी-प्राचार्य इन दोनों नयोंमेंसे [इह ] इस ग्रन्थमें [ निश्चयं ] निश्चयनयको [ भूतार्थ ] भूतार्थ और [ व्यवहारं ] व्यवहारनयको [अभूतार्थं ] अभूतार्थ [ वर्णयन्ति ] वर्णन करते हैं। [ प्रायः ] बहुत करके [भूतार्थबोधविमुखः ] भूतार्थ अर्थात् निश्चयनयके ज्ञानसे विरुद्ध जो अभिप्राय हैं, वे [ सर्वोऽपि ] समस्त हो [ संसारः ] संसारस्वरूप हैं।
भावार्थ- भूतार्थ' ' शब्दका अर्थ सत्यार्थ है, और कल्पनासे कुछ भी न कहकर जैसाका तैसा कहनेको सत्यार्थ कहते हैं । यद्यपि जीव और पुद्गलका अनादिकालसे एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है
और दोनों मिले हुए दीखते हैं; तथापि निश्चयनय शुद्ध प्रात्मद्रव्यको शरीरादिक परद्रव्योंसे भिन्न हो प्रकाश करता है, और यही भिन्नता मुक्तदशामें प्रकट होती है। अतएव निश्चयनय ही भूतार्थ है। यद्यपि जीव और पुद्गलका सत्व भिन्न है, रूप बदलनेपर स्वभाव भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, तथापि व्यवहारनय एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धका छल पाकर आत्मद्रव्यको शरीरादिक परद्रव्यों से एकत्वरूप कहता है । मुक्तिदशामें प्रकट भिन्नता होनेपर व्यवहारनय स्वयं ही पृथक् प्रकाश करनेके लिये तत्पर हो जाता है, इसलिये व्यवहार अभूतार्थ है।
__ 'प्रायः भूतार्थबोधविमुखः सर्वोऽपि संसारः' इस वाक्यका विशेषार्थ-आत्माका परिणाम निश्चयनयके श्रद्धानसे विमुख होकर शरीरादिक परद्रव्योंसे एकत्वरूप प्रवर्तन करता है। इसको ही संसार कहते हैं, संसार कोई पृथक् पदार्थ नहीं है। इसलिये जो जीव संसारसे मुक्त होना चाहे, उसको शद्ध ( निश्चय ) नयके सन्मुख रहना योग्य है।
एक पुरुष कर्दमके संयोगसे जिसका निर्मल भाव आच्छादित हो गया है, ऐसे जलको समल ही पीता है, और कोई दूसरा पुरुष थोड़ासा परिश्रम कर कतकफल (निर्मली) डालके जल और कर्दमको जुदा जुदा करके शुद्ध निर्मल जलका पास्वादन करता है । ठोक इस ही प्रकार अज्ञानी जीव कर्नसंयोगसे जिसका ज्ञानस्वभाव आच्छादित है, ऐसे अशुद्ध प्रात्माका अनुभव करते हैं, और दूसरे अपनी बुद्धिसे शुद्ध निश्चयनयके स्वरूपको जानकर कर्म और आत्माको पृथक् पृथक् करके निर्मल आत्माका स्वानुभवरूप प्रास्वादन करते हैं। इससे शुद्ध नय कतकफलके समान है। इसके श्रद्धानसे सर्वसिद्धि' होती है।
प्रबुधस्य बोधनार्थ" मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।।
व्यवहारमेव केवलमवति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥ १-भूत-पदार्थमें पाये जाने वाले भाव उनका अर्थ-ज्योंका न्यों प्रकाश करना इसे ही भूतार्थ कहते हैं । इस शब्दका पूर्णभाव सत्यार्थ शब्द है । कल्पनासे कुछ न कहकर ज्योंका त्यों कहना यही सत्यार्थ है । २-अभूतजो पदार्थ में न पाया जावे, ऐसा अर्थ-भाव, उसे अनेक कल्पनाकर प्रकाशित करे, उसे प्रभूतार्थ अर्थात् असत्यार्थ कहते हैं, जैसे मृषावादी पुरुष कल्पनाके बलसे अनेक कल्पना करके तादृश कर दिखाता है। ३-इस प्रकरणमें यह प्रश्न हो सकता है, कि यदि — व्यवहार ' असत्यार्थ है, और कार्यकारी नहीं है: तो व्यवहारनयका कथन आचार्योंने क्यों किया? परन्तु इसका उत्तर प्रागेके श्लोकमें दिया गया है। ४-देशनार्थमित्यपि पाठः ।