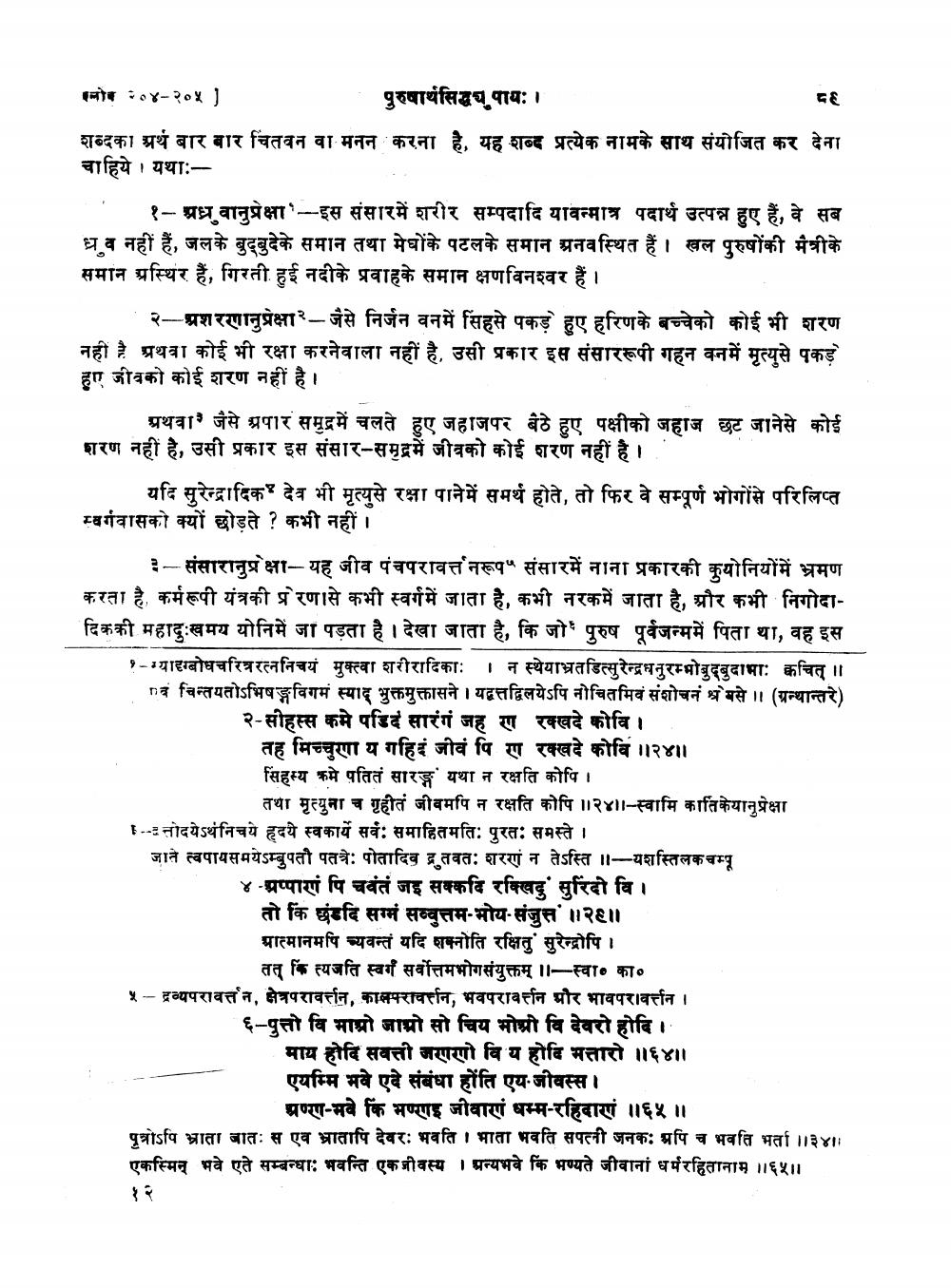________________
इनोव २०४-२०५ ) पुरुषार्थसिवय पायः।
८६ शब्दका अर्थ बार बार चितवन वा मनन करना है, यह शब्द प्रत्येक नामके साथ संयोजित कर देना चाहिये । यथा:
१- अध्र वानुप्रेक्षा'-इस संसारमें शरीर सम्पदादि यावन्मात्र पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, वे सब ध्र व नहीं हैं, जलके बुबुदेके समान तथा मेघोंके पटलके समान अनव स्थित हैं। खल पुरुषोंकी मैत्रीके समान अस्थिर हैं, गिरती हुई नदीके प्रवाहके समान क्षणविनश्वर हैं।
२-अशरणानुप्रेक्षा२- जैसे निर्जन वनमें सिंहसे पकड़े हुए हरिणके बच्चेको कोई भी शरण नहीं है अथवा कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं है, उसी प्रकार इस संसाररूपी गहन वनमें मृत्युसे पकड़े हए जीवको कोई शरण नहीं है।
अथवा' जैसे अपार समुद्र में चलते हुए जहाजपर बैठे हुए पक्षीको जहाज छट जानेसे कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार इस संसार-समुद्र में जीवको कोई शरण नहीं है।
__यदि सुरेन्द्रादिक देव भी मृत्युसे रक्षा पानेमें समर्थ होते, तो फिर वे सम्पूर्ण भोगोंसे परिलिप्त म्वर्गवासको क्यों छोड़ते ? कभी नहीं।
३-संसारानुप्रेक्षा- यह जीव पंचपरावर्तनरूप" संसारमें नाना प्रकारकी कुयोनियों में भ्रमण करता है, कर्मरूपी यंत्रकी प्रेरणासे कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरकमें जाता है, और कभी निगोदादिककी महादुःखमय योनिमें जा पड़ता है । देखा जाता है, कि जो पुरुष पूर्वजन्ममें पिता था, वह इस
१-याहग्बोधचरित्ररत्ननिचयं मुक्त्वा शरीरादिकाः । न स्थेयाभ्रतडित्सुरेन्द्रधनुरम्भोबुबुदामाः क्वचित् ।। nवं चिन्तयतोऽभिषङ्गविगमं स्याद् भुक्तमुक्तासने । यद्वत्तद्विलयेऽपि नोचितमिवं संशोचनं श्रेयसे ।। (ग्रन्थान्तरे)
२-सीहस्स कमे पडिद सारंगं जह ण रक्खदे कोवि। तह मिच्चुरणा य गहिदं जीवं पि रण रक्खदे कोविं ॥२४॥ सिंहस्य क्रमे पतितं सारङ्ग यथा न रक्षति कोपि ।
तथा मृत्युना च गृहीतं जीवमपि न रक्षति कोपि ॥२४॥-स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा 1 -- नोदयेऽथंनिचये हृदये स्वकार्ये सर्वः समाहितमतिः पुरतः समस्ते । जाते त्वपायसमयेऽम्बुपती पतत्रेः पोतादिव द्रुतवतः शरणं न तेऽस्ति ।-यशस्तिलकचम्पू
४ -अप्पारणं पिचवंतं जइ सक्कदि रक्खि सूरिंदो वि।
तो कि छंडदि सग्मं सव्वुत्तम-भोय-संजुस ॥२६॥ मात्मानमपि च्यवन्तं यदि शक्नोति रक्षितु सुरेन्द्रोपि ।
तत् किं त्यजति स्वर्ग सर्वोत्तमभोगसंयुक्तम् ।।-स्वा. का. ५ - द्रव्यपरावर्तन, क्षेत्रपरावर्तन, कालपरावर्तन, भवपरावर्तन और भावपरावर्त्तन ।
६-पुत्तो वि भानो जानो सो चिय मोनो वि देवरो होदि ।
माय होदि सवत्ती जणणो वि य होदि भत्तारो ॥६४॥ एयम्मि भवे एवे संबंधा होंति एय-जीवस्स।
अण्ण-मवे किं भण्णइ जीवाणं धम्म-रहिवारणं ॥६५॥ पुत्रोऽपि भ्राता जातः स एव भ्रातापि देवरः भवति । भाता भवति सपत्नी जनकः अपि च भवति भर्ता ॥३४॥ एकस्मिन् भवे एते सम्बन्धाः भवन्ति एकजीवस्य । अन्यभवे किं भण्यते जीवानां धर्मरहितानाम ॥६५॥