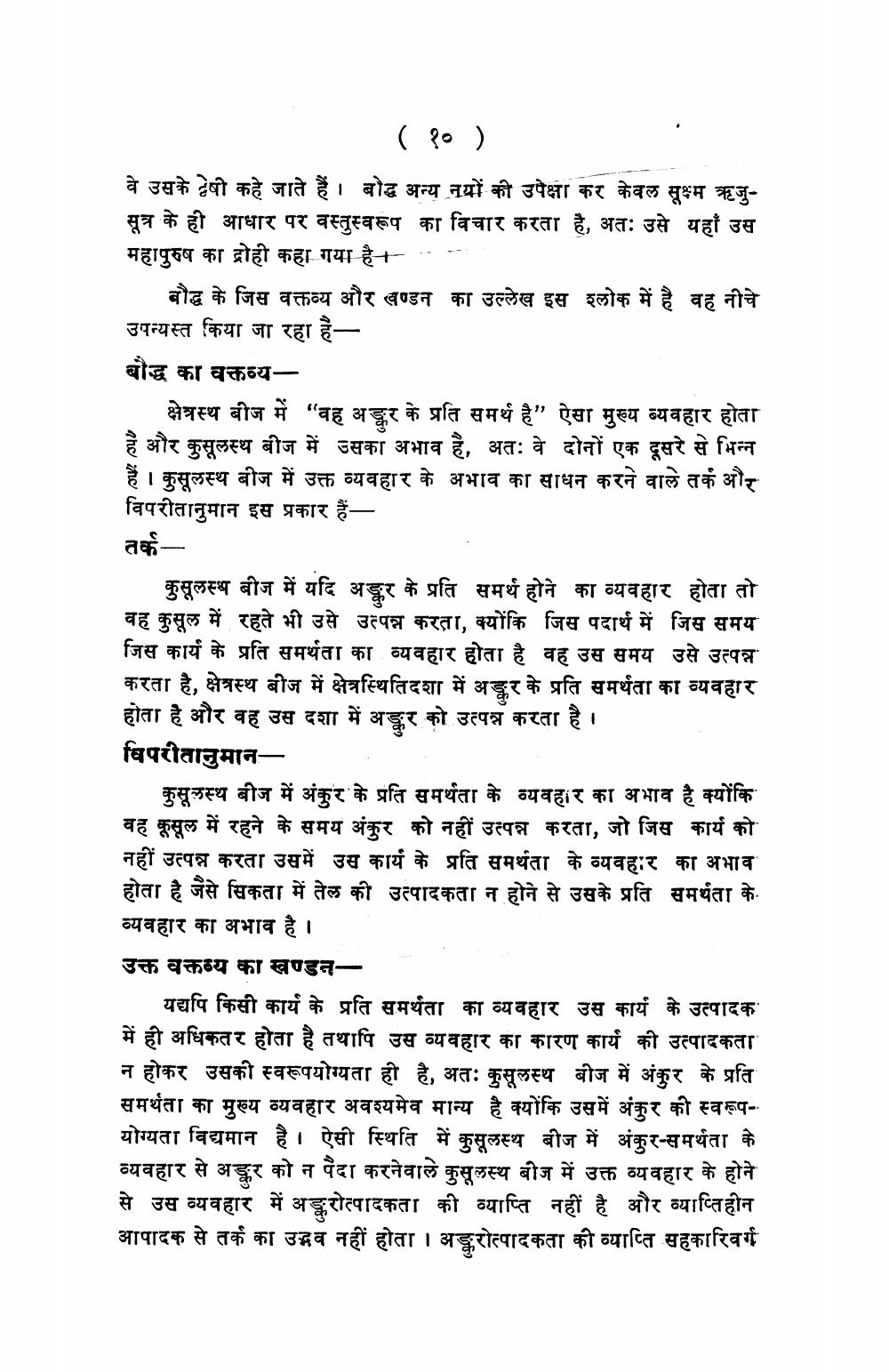________________
( १० ) वे उसके द्वेषी कहे जाते हैं। बोद्ध अन्य नयों की उपेक्षा कर केवल सूक्ष्म ऋजुसूत्र के ही आधार पर वस्तुस्वरूप का विचार करता है, अतः उसे यहाँ उस महापुरुष का द्रोही कहा गया है।
बौद्ध के जिस वक्तव्य और खण्डन का उल्लेख इस श्लोक में है वह नीचे उपन्यस्त किया जा रहा हैबौद्ध का वक्तव्य
क्षेत्रस्थ बीज में "वह अङ्कर के प्रति समर्थ है" ऐसा मुख्य ब्यवहार होता है और कुसूलस्थ बीज में उसका अभाव है, अतः वे दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं । कुसूलस्थ बीज में उक्त व्यवहार के अभाव का साधन करने वाले तर्क और विपरीतानुमान इस प्रकार हैंतर्क
कुसूलस्थ बीज में यदि अङ्कर के प्रति समर्थ होने का व्यवहार होता तो वह कुसूल में रहते भी उसे उत्पन्न करता, क्योंकि जिस पदार्थ में जिस समय जिस कार्य के प्रति समर्थता का व्यवहार होता है वह उस समय उसे उत्पन्न करता है, क्षेत्रस्थ बीज में क्षेत्रस्थितिदशा में अङ्कर के प्रति समर्थता का व्यवहार होता है और वह उस दशा में अङ्कर को उत्पन्न करता है। विपरीतानुमान
कुसूलस्थ बीज में अंकुर के प्रति समर्थता के व्यवहार का अभाव है क्योंकि वह कूसूल में रहने के समय अंकुर को नहीं उत्पन्न करता, जो जिस कार्य को नहीं उत्पन्न करता उसमें उस कार्य के प्रति समर्थता के व्यवहार का अभाव होता है जैसे सिकता में तेल की उत्पादकता न होने से उसके प्रति समर्थता के व्यवहार का अभाव है। उक्त वक्तव्य का खण्डन__ यद्यपि किसी कार्य के प्रति समर्थता का व्यवहार उस कार्य के उत्पादक में ही अधिकतर होता है तथापि उस व्यवहार का कारण कार्य की उत्पादकता न होकर उसकी स्वरूपयोग्यता ही है, अतः कुसूलस्थ बीज में अंकुर के प्रति समर्थता का मुख्य व्यवहार अवश्यमेव मान्य है क्योंकि उसमें अंकुर की स्वरूपयोग्यता विद्यमान है। ऐसी स्थिति में कुसूलस्थ बीज में अंकुर-समर्थता के व्यवहार से अङ्कर को न पैदा करनेवाले कुसूलस्थ बीज में उक्त व्यवहार के होने से उस व्यवहार में अङ्करोत्पादकता की व्याप्ति नहीं है और व्याप्तिहीन आपादक से तर्क का उद्भव नहीं होता । अङ्करोत्पादकता की व्याप्ति सहकारिवर्ग