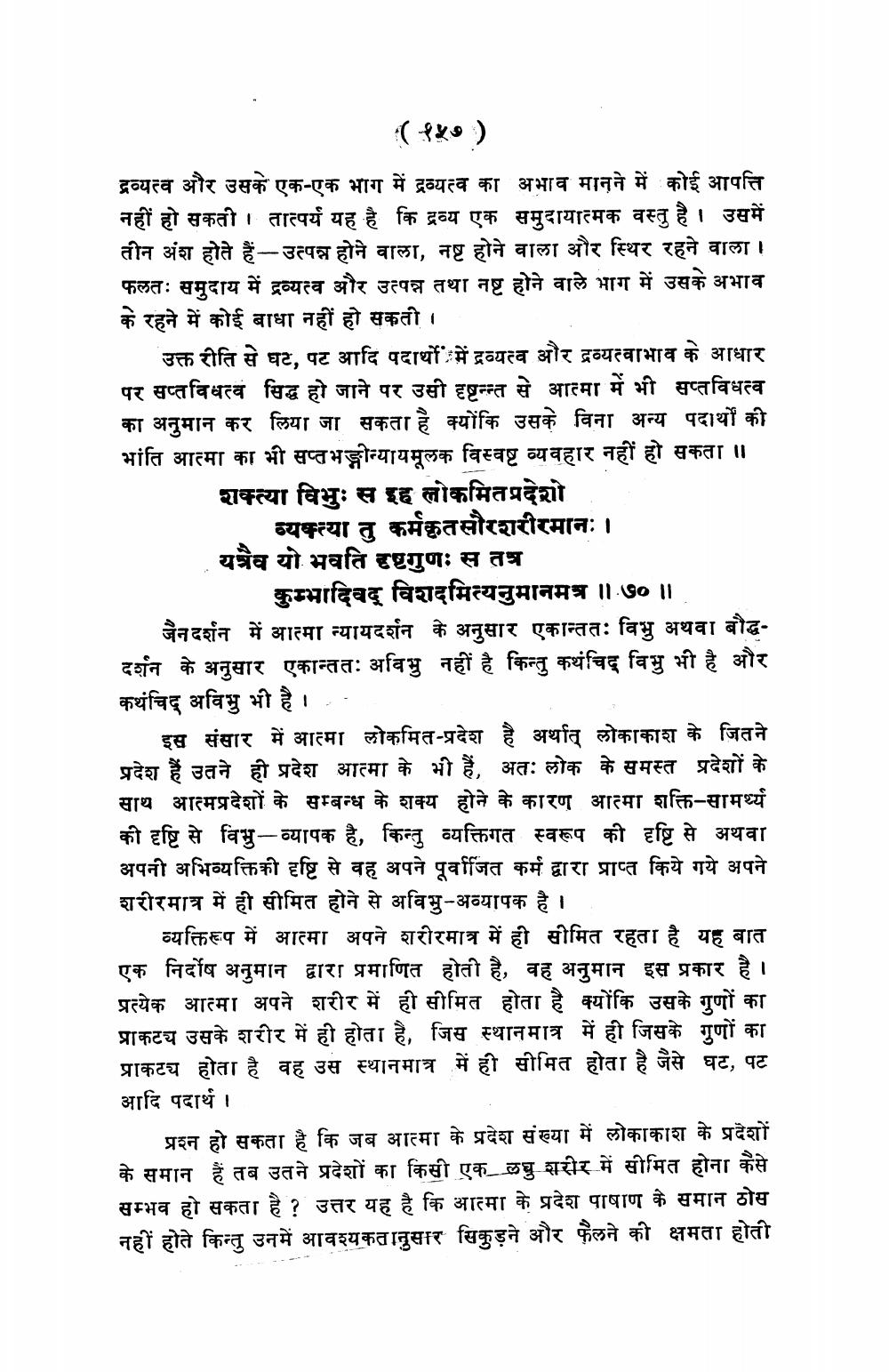________________
( १५७ )
द्रव्यत्व और उसके एक-एक भाग में द्रव्यत्व का अभाव मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । तात्पर्य यह है कि द्रव्य एक समुदायात्मक वस्तु है । उसमें तीन अंश होते हैं - उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला और स्थिर रहने वाला । फलतः समुदाय में द्रव्यत्व और उत्पन्न तथा नष्ट होने वाले भाग में उसके अभाव के रहने में कोई बाधा नहीं हो सकती ।
उक्त रीति से घट, पट आदि पदार्थों में द्रव्यत्व और द्रव्यत्वाभाव के आधार पर सप्तविधत्वं सिद्ध हो जाने पर उसी दृष्टन्न्त से आत्मा में भी सप्तविधत्व का अनुमान कर लिया जा सकता है क्योंकि उसके विना अन्य पदार्थों की भांति आत्मा का भी सप्तभङ्गीन्यायमूलक विस्वष्ट व्यवहार नहीं हो सकता ॥ शक्त्या विभुः स इह लोकमित प्रदेशो व्यक्त्या तु कर्मकृतसौरशरीरमानः । यत्रैव यो भवति दृष्टगुणः स तत्र
कुम्भादिवद् विशदमित्यनुमानमत्र ॥ ७० ॥
जैनदर्शन में आत्मा न्यायदर्शन के अनुसार एकान्ततः विभु अथवा बौद्धदर्शन के अनुसार एकान्ततः अविभु नहीं है किन्तु कथंचिद् विभु भी है और कथंचिद् अविभु भी है ।
इस संसार में आत्मा लोकमित- प्रदेश है अर्थात् लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश आत्मा के भी हैं, अतः लोक के समस्त प्रदेशों के साथ आत्मप्रदेशों के सम्बन्ध के शक्य होने के कारण आत्मा शक्ति - सामर्थ्य की दृष्टि से विभु -व्यापक है, किन्तु व्यक्तिगत स्वरूप की दृष्टि से अथवा अपनी अभिव्यक्तिकी दृष्टि से वह अपने पूर्वार्जित कर्म द्वारा प्राप्त किये गये अपने शरीरमात्र में ही सीमित होने से अविभु-अव्यापक है ।
व्यक्तिरूप में आत्मा अपने शरीरमात्र में ही सीमित रहता है यह बात एक निर्दोष अनुमान द्वारा प्रमाणित होती है, वह अनुमान इस प्रकार है । प्रत्येक आत्मा अपने शरीर में ही सीमित होता है क्योंकि उसके गुणों का प्राकट्य उसके शरीर में ही होता है, जिस स्थानमात्र में ही जिसके गुणों का प्राकट्य होता है वह उस स्थानमात्र में ही सीमित होता है जैसे घट, पट आदि पदार्थ ।
प्रश्न हो सकता है कि जब आत्मा के प्रदेश संख्या में लोकाकाश के प्रदेशों के समान हैं तब उतने प्रदेशों का किसी एक लघु शरीर सीमित होना कैसे सम्भव हो सकता है ? उत्तर यह है कि आत्मा के प्रदेश पाषाण के समान ठोस नहीं होते किन्तु उनमें आवश्यकतानुसार सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती