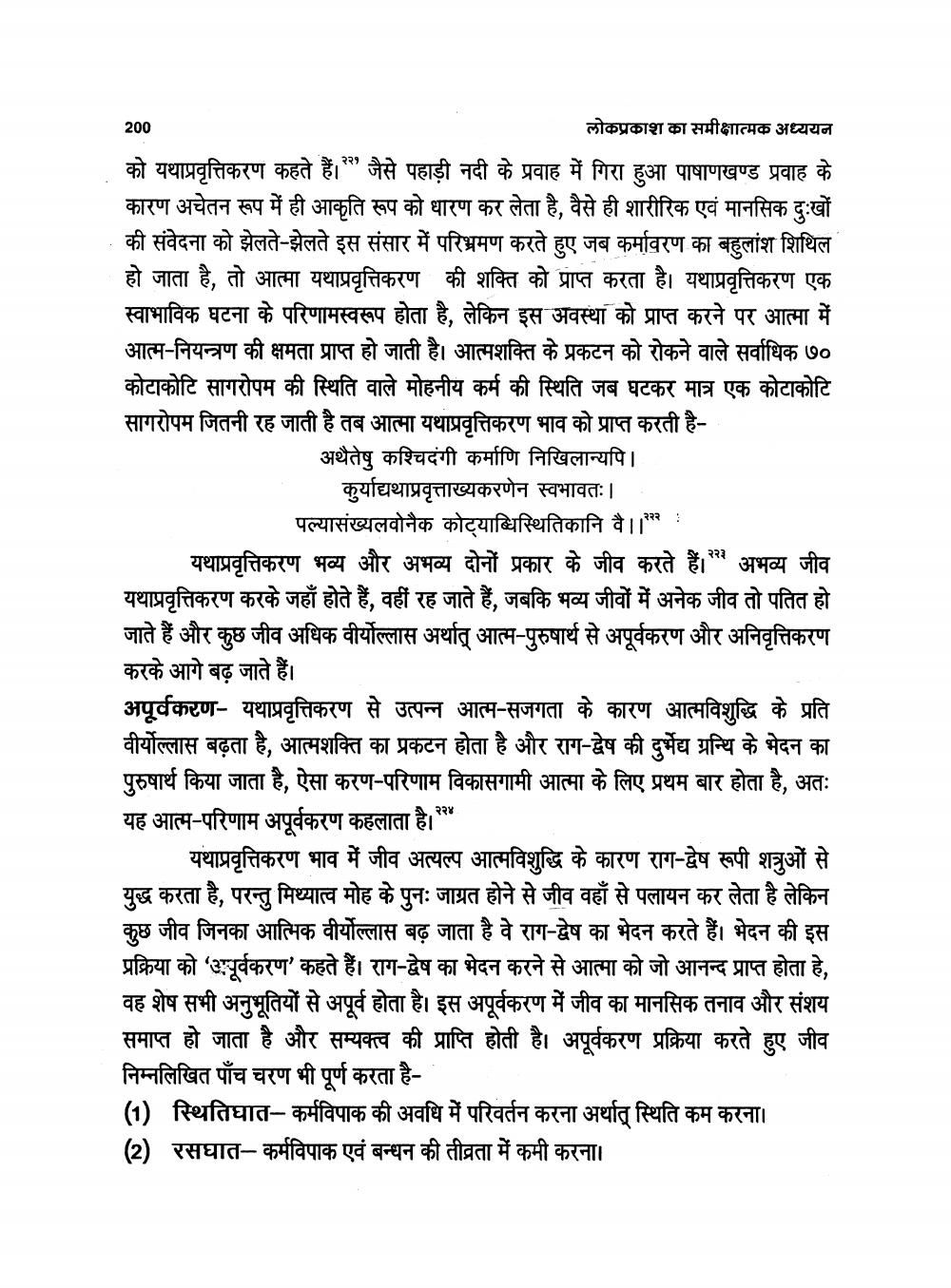________________
200
लोकप्रकाश का समीक्षात्मक अध्ययन को यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं। जैसे पहाड़ी नदी के प्रवाह में गिरा हुआ पाषाणखण्ड प्रवाह के कारण अचेतन रूप में ही आकृति रूप को धारण कर लेता है, वैसे ही शारीरिक एवं मानसिक दुःखों की संवेदना को झेलते-झेलते इस संसार में परिभ्रमण करते हुए जब कर्मावरण का बहुलांश शिथिल हो जाता है, तो आत्मा यथाप्रवृत्तिकरण की शक्ति को प्राप्त करता है। यथाप्रवृत्तिकरण एक स्वाभाविक घटना के परिणामस्वरूप होता है, लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने पर आत्मा में आत्म-नियन्त्रण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आत्मशक्ति के प्रकटन को रोकने वाले सर्वाधिक ७० कोटाकोटि सागरोपम की स्थिति वाले मोहनीय कर्म की स्थिति जब घटकर मात्र एक कोटाकोटि सागरोपम जितनी रह जाती है तब आत्मा यथाप्रवृत्तिकरण भाव को प्राप्त करती है
अर्थतेषु कश्चिदंगी कर्माणि निखिलान्यपि। - कुर्याद्यथाप्रवृत्ताख्यकरणेन स्वभावतः।
पल्यासंख्यलवोनैक कोट्याब्धिस्थितिकानि वै ।।२२।। यथाप्रवृत्तिकरण भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीव करते हैं।२२२ अभव्य जीव यथाप्रवृत्तिकरण करके जहाँ होते हैं, वहीं रह जाते हैं, जबकि भव्य जीवों में अनेक जीव तो पतित हो जाते हैं और कुछ जीव अधिक वीर्योल्लास अर्थात् आत्म-पुरुषार्थ से अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण करके आगे बढ़ जाते हैं। अपूर्वकरण- यथाप्रवृत्तिकरण से उत्पन्न आत्म-सजगता के कारण आत्मविशुद्धि के प्रति वीर्योल्लास बढ़ता है, आत्मशक्ति का प्रकटन होता है और राग-द्वेष की दुर्भेद्य ग्रन्थि के भेदन का पुरुषार्थ किया जाता है, ऐसा करण-परिणाम विकासगामी आत्मा के लिए प्रथम बार होता है, अतः यह आत्म-परिणाम अपूर्वकरण कहलाता है।२२४
___ यथाप्रवृत्तिकरण भाव में जीव अत्यल्प आत्मविशुद्धि के कारण राग-द्वेष रूपी शत्रुओं से युद्ध करता है, परन्तु मिथ्यात्व मोह के पुनः जाग्रत होने से जीव वहाँ से पलायन कर लेता है लेकिन कुछ जीव जिनका आत्मिक वीर्योल्लास बढ़ जाता है वे राग-द्वेष का भेदन करते हैं। भेदन की इस प्रक्रिया को 'अपूर्वकरण' कहते हैं। राग-द्वेष का भेदन करने से आत्मा को जो आनन्द प्राप्त होता है, वह शेष सभी अनुभूतियों से अपूर्व होता है। इस अपूर्वकरण में जीव का मानसिक तनाव और संशय समाप्त हो जाता है और सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अपूर्वकरण प्रक्रिया करते हुए जीव निम्नलिखित पाँच चरण भी पूर्ण करता है(1) स्थितिघात-कर्मविपाक की अवधि में परिवर्तन करना अर्थात् स्थिति कम करना। (2) रसघात- कर्मविपाक एवं बन्धन की तीव्रता में कमी करना।