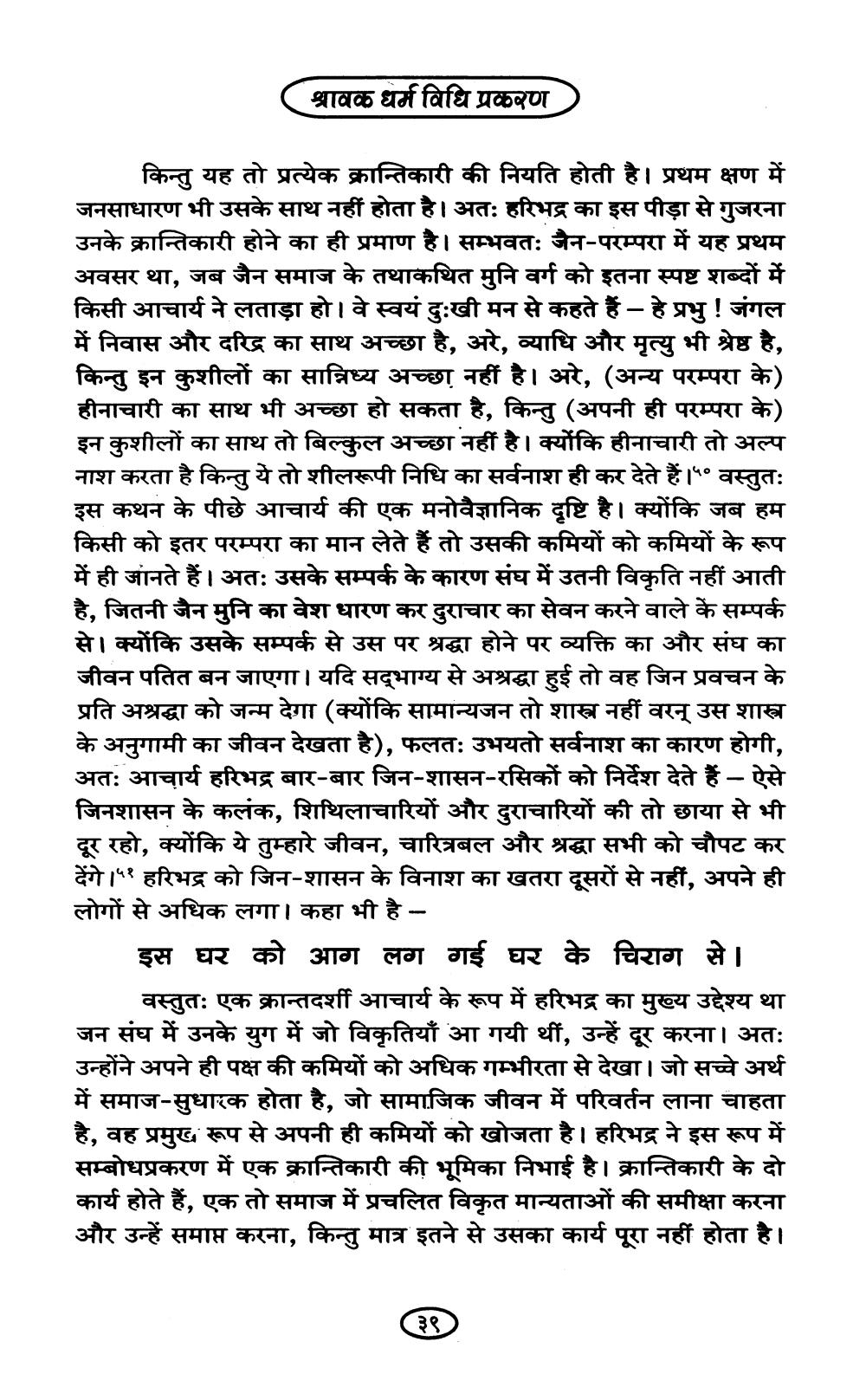________________
(श्रावक धर्म विधि प्रकरण )
किन्तु यह तो प्रत्येक क्रान्तिकारी की नियति होती है। प्रथम क्षण में जनसाधारण भी उसके साथ नहीं होता है। अतः हरिभद्र का इस पीड़ा से गुजरना उनके क्रान्तिकारी होने का ही प्रमाण है। सम्भवत: जैन-परम्परा में यह प्रथम अवसर था, जब जैन समाज के तथाकथित मुनि वर्ग को इतना स्पष्ट शब्दों में किसी आचार्य ने लताड़ा हो। वे स्वयं दुःखी मन से कहते हैं- हे प्रभु ! जंगल में निवास और दरिद्र का साथ अच्छा है, अरे, व्याधि और मृत्यु भी श्रेष्ठ है, किन्तु इन कुशीलों का सान्निध्य अच्छा नहीं है। अरे, (अन्य परम्परा के) हीनाचारी का साथ भी अच्छा हो सकता है, किन्तु (अपनी ही परम्परा के) इन कुशीलों का साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि हीनाचारी तो अल्प नाश करता है किन्तु ये तो शीलरूपी निधि का सर्वनाश ही कर देते हैं। वस्तुतः इस कथन के पीछे आचार्य की एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। क्योंकि जब हम किसी को इतर परम्परा का मान लेते हैं तो उसकी कमियों को कमियों के रूप में ही जानते हैं। अत: उसके सम्पर्क के कारण संघ में उतनी विकृति नहीं आती है, जितनी जैन मुनि का वेश धारण कर दुराचार का सेवन करने वाले के सम्पर्क से। क्योंकि उसके सम्पर्क से उस पर श्रद्धा होने पर व्यक्ति का और संघ का जीवन पतित बन जाएगा। यदि सद्भाग्य से अश्रद्धा हुई तो वह जिन प्रवचन के प्रति अश्रद्धा को जन्म देगा (क्योंकि सामान्यजन तो शास्त्र नहीं वरन् उस शास्त्र के अनुगामी का जीवन देखता है), फलत: उभयतो सर्वनाश का कारण होगी, अत: आचार्य हरिभद्र बार-बार जिन-शासन-रसिकों को निर्देश देते हैं- ऐसे जिनशासन के कलंक, शिथिलाचारियों और दुराचारियों की तो छाया से भी दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन, चारित्रबल और श्रद्धा सभी को चौपट कर देंगे।५१ हरिभद्र को जिन-शासन के विनाश का खतरा दूसरों से नहीं, अपने ही लोगों से अधिक लगा। कहा भी है
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।
वस्तुत: एक क्रान्तदर्शी आचार्य के रूप में हरिभद्र का मुख्य उद्देश्य था जन संघ में उनके युग में जो विकृतियाँ आ गयी थीं, उन्हें दूर करना। अत: उन्होंने अपने ही पक्ष की कमियों को अधिक गम्भीरता से देखा। जो सच्चे अर्थ में समाज-सुधारक होता है, जो सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, वह प्रमुख रूप से अपनी ही कमियों को खोजता है। हरिभद्र ने इस रूप में सम्बोधप्रकरण में एक क्रान्तिकारी की भूमिका निभाई है। क्रान्तिकारी के दो कार्य होते हैं, एक तो समाज में प्रचलित विकृत मान्यताओं की समीक्षा करना और उन्हें समाप्त करना, किन्तु मात्र इतने से उसका कार्य पूरा नहीं होता है।