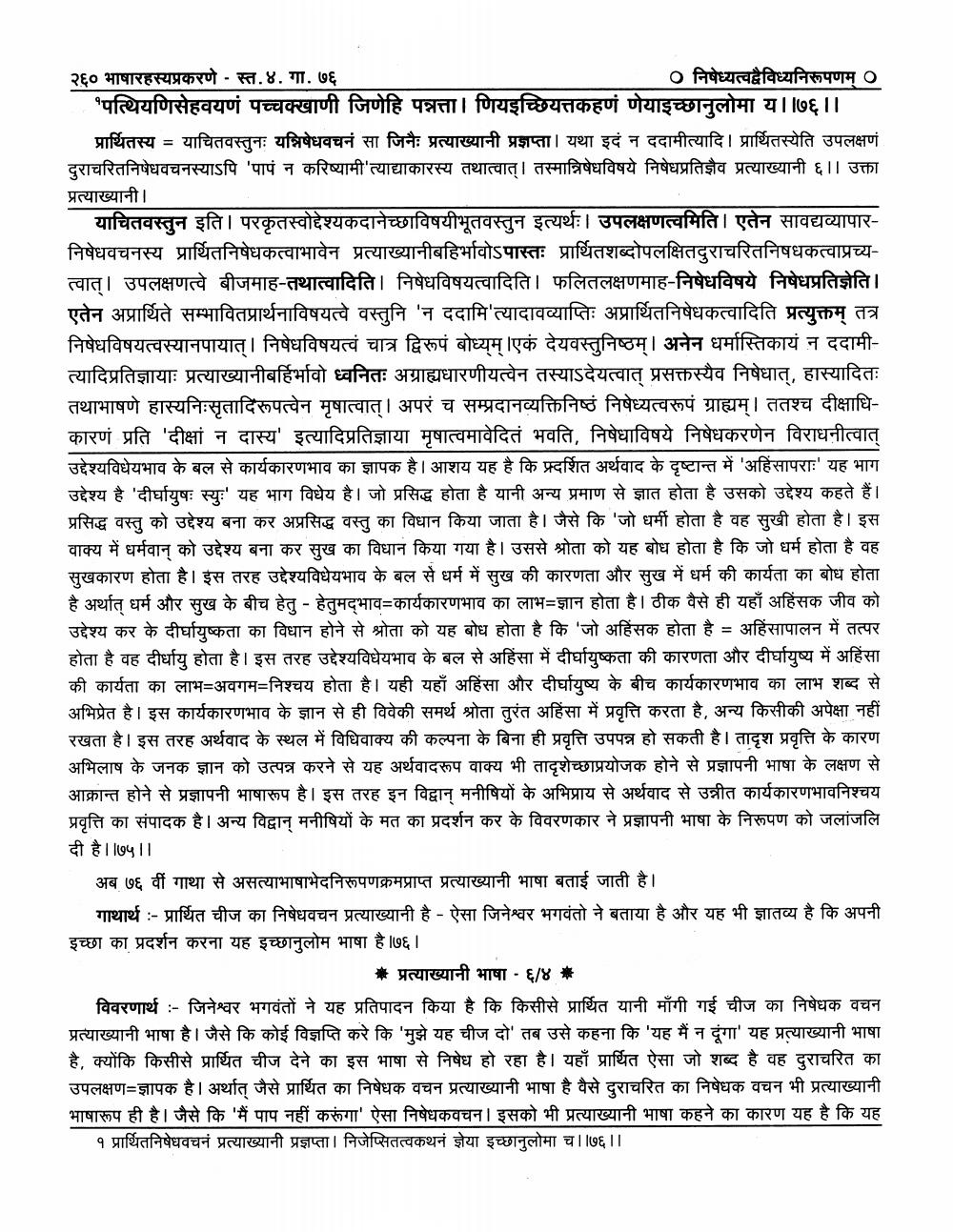________________
२६० भाषारहस्यप्रकरणे स्त. ४. गा. ७६
० निषेध्यत्वद्वैविध्यनिरूपणम् 0
'पत्थियणिसेहवयणं पच्चक्खाणी जिणेहि पन्नत्ता । णियइच्छियत्तकहणं णेयाइच्छानुलोमा य ||७६ ।। प्रार्थितस्य = याचितवस्तुनः यन्निषेधवचनं सा जिनैः प्रत्याख्यानी प्रज्ञप्ता । यथा इदं न ददामीत्यादि । प्रार्थितस्येति उपलक्षणं दुराचरितनिषेधवचनस्याऽपि 'पापं न करिष्यामीत्याद्याकारस्य तथात्वात् । तस्मान्निषेधविषये निषेधप्रतिज्ञैव प्रत्याख्यानी ६।। उक्ता प्रत्याख्यानी ।
याचितवस्तुन इति। परकृतस्वोद्देश्यकदानेच्छाविषयीभूतवस्तुन इत्यर्थः । उपलक्षणत्वमिति । एतेन सावद्यव्यापारनिषेधवचनस्य प्रार्थितनिषेधकत्वाभावेन प्रत्याख्यानीबहिर्भावोऽपास्तः प्रार्थितशब्दोपलक्षितदुराचरितनिषधकत्वाप्रच्यत्वात्। उपलक्षणत्वे बीजमाह - तथात्वादिति । निषेधविषयत्वादिति । फलितलक्षणमाह-निषेधविषये निषेधप्रतिज्ञेति । एतेन अप्रार्थिते सम्भावितप्रार्थनाविषयत्वे वस्तुनि 'न ददामि' त्यादावव्याप्तिः अप्रार्थितनिषेधकत्वादिति प्रत्युक्तम् तत्र निषेधविषयत्वस्यानपायात् । निषेधविषयत्वं चात्र द्विरूपं बोध्यम् । एकं देयवस्तुनिष्ठम् । अनेन धर्मास्तिकायं न ददामीत्यादिप्रतिज्ञायाः प्रत्याख्यानीबर्हिर्भावो ध्वनितः अग्राह्यधारणीयत्वेन तस्याऽदेयत्वात् प्रसक्तस्यैव निषेधात्, हास्यादितः तथाभाषणे हास्यनिःसृतादिरूपत्वेन मृषात्वात् । अपरं च सम्प्रदानव्यक्तिनिष्ठं निषेध्यत्वरूपं ग्राह्यम् । ततश्च दीक्षाधिकारणं प्रति 'दीक्षां न दास्य' इत्यादिप्रतिज्ञाया मृषात्वमावेदितं भवति निषेधाविषये निषेधकरणेन विराधनीत्वात् उद्देश्यविधेयभाव के बल से कार्यकारणभाव का ज्ञापक है। आशय यह है कि प्रदर्शित अर्थवाद के दृष्टान्त में 'अहिंसापराः' यह भाग उद्देश्य है 'दीर्घायुषः स्युः यह भाग विधेय है। जो प्रसिद्ध होता है यानी अन्य प्रमाण से ज्ञात होता है उसको उद्देश्य कहते हैं। प्रसिद्ध वस्तु को उद्देश्य बना कर अप्रसिद्ध वस्तु का विधान किया जाता है। जैसे कि 'जो धर्मी होता है वह सुखी होता है। इस वाक्य में धर्मवान् को उद्देश्य बना कर सुख का विधान किया गया है। उससे श्रोता को यह बोध होता है कि जो धर्म होता है वह सुखकारण होता है। इस तरह उद्देश्यविधेयभाव के बल से धर्म में सुख की कारणता और सुख में धर्म की कार्यता का बोध होता है अर्थात् धर्म और सुख के बीच हेतु हेतुमद्भाव = कार्यकारणभाव का लाभ ज्ञान होता है। ठीक वैसे ही यहाँ अहिंसक जीव को उद्देश्य कर के दीर्घायुष्कता का विधान होने से श्रोता को यह बोध होता है कि 'जो अहिंसक होता है = अहिंसापालन में तत्पर होता है वह दीर्घायु होता है। इस तरह उद्देश्यविधेयभाव के बल से अहिंसा में दीर्घायुष्कता की कारणता और दीर्घायुष्य में अहिंसा की कार्यता का लाभ = अवगम = निश्चय होता है। यही यहाँ अहिंसा और दीर्घायुष्य के बीच कार्यकारणभाव का लाभ शब्द से अभिप्रेत है। इस कार्यकारणभाव के ज्ञान से ही विवेकी समर्थ श्रोता तुरंत अहिंसा में प्रवृत्ति करता है, अन्य किसीकी अपेक्षा नहीं रखता है। इस तरह अर्थवाद के स्थल में विधिवाक्य की कल्पना के बिना ही प्रवृत्ति उपपन्न हो सकती है। तादृश प्रवृत्ति के कारण अभिलाष के जनक ज्ञान को उत्पन्न करने से यह अर्थवादरूप वाक्य भी तादृशेच्छाप्रयोजक होने से प्रज्ञापनी भाषा के लक्षण से आक्रान्त होने से प्रज्ञापनी भाषारूप है। इस तरह इन विद्वान् मनीषियों के अभिप्राय से अर्थवाद से उन्नीत कार्यकारणभावनिश्चय प्रवृत्ति का संपादक है। अन्य विद्वान् मनीषियों के मत का प्रदर्शन कर के विवरणकार ने प्रज्ञापनी भाषा के निरूपण को जलांजलि दी है । ७५ ।।
-
अब ७६ वीं गाथा से असत्याभाषाभेदनिरूपणक्रमप्राप्त प्रत्याख्यानी भाषा बताई जाती है।
गाथार्थ :- प्रार्थित चीज का निषेधवचन प्रत्याख्यानी है ऐसा जिनेश्वर भगवंतो ने बताया है और यह भी ज्ञातव्य है कि अपनी इच्छा का प्रदर्शन करना यह इच्छानुलोम भाषा है । ७६ ।
* प्रत्याख्यानी भाषा ६/४*
विवरणार्थ :- जिनेश्वर भगवंतों ने यह प्रतिपादन किया है कि किसीसे प्रार्थित यानी माँगी गई चीज का निषेधक वचन प्रत्याख्यानी भाषा है। जैसे कि कोई विज्ञप्ति करे कि 'मुझे यह चीज दो' तब उसे कहना कि 'यह मैं न दूंगा' यह प्रत्याख्यानी भाषा है, क्योंकि किसीसे प्रार्थित चीज देने का इस भाषा से निषेध हो रहा है। यहाँ प्रार्थित ऐसा जो शब्द है वह दुराचरित का उपलक्षण= ज्ञापक है। अर्थात् जैसे प्रार्थित का निषेधक वचन प्रत्याख्यानी भाषा है वैसे दुराचरित का निषेधक वचन भी प्रत्याख्यानी भाषारूप ही है। जैसे कि 'मैं पाप नहीं करूंगा' ऐसा निषेधकवचन । इसको भी प्रत्याख्यानी भाषा कहने का कारण यह है कि यह
१ प्रार्थितनिषेधवचनं प्रत्याख्यानी प्रज्ञप्ता । निजेप्सितत्वकथनं ज्ञेया इच्छानुलोमा च । ७६ ।।