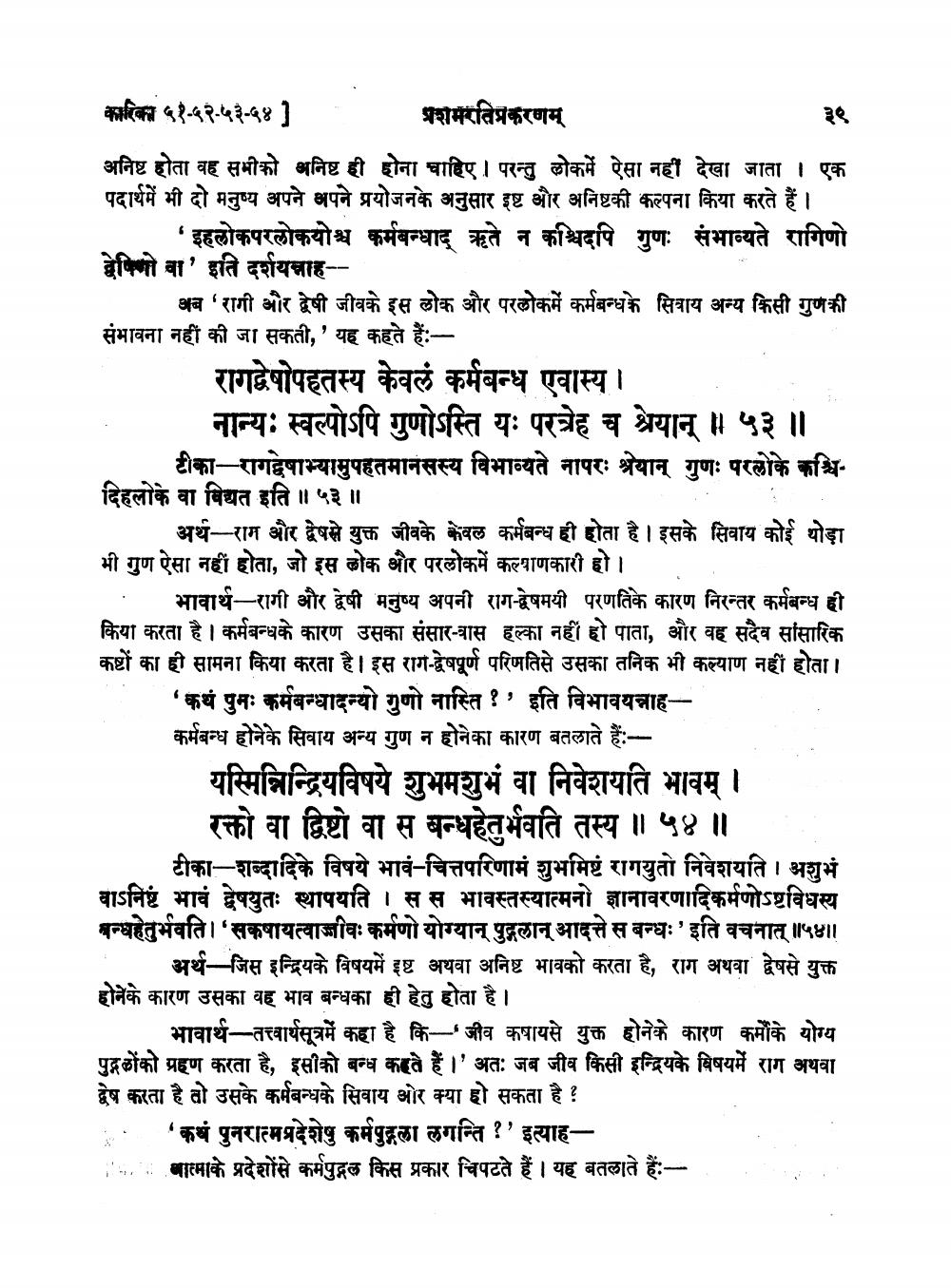________________
कारिका ५१-५२-५३-५४ ] प्रशमरतिप्रकरणम् अनिष्ट होता वह सभीको अनिष्ट ही होना चाहिए। परन्तु लोकमें ऐसा नहीं देखा जाता । एक पदार्थमें भी दो मनुष्य अपने अपने प्रयोजनके अनुसार इष्ट और अनिष्टकी कल्पना किया करते हैं।
'इहलोकपरलोकयोश्च कर्मबन्धाद् ऋते न कश्चिदपि गुणः संभाव्यते रागिणो वेषिको वा' इति दर्शयन्नाह--
अब 'रागी और द्वेषी जीवके इस लोक और परलोकमें कर्मबन्धके सिवाय अन्य किसी गुणकी संभावना नहीं की जा सकती,' यह कहते हैं:
रागद्वेषोपहतस्य केवलं कर्मबन्ध एवास्य।
नान्यः स्वल्पोऽपि गुणोऽस्ति यः परत्रेह च श्रेयान् ॥ ५३॥
टीका-रागद्वेषाभ्यामुपहतमानसस्य विभाव्यते नापरः श्रेयान् गुणः परलोके कश्चिदिहलोके वा विद्यत इति ॥ ५३ ॥
अर्थ-राम और द्वेषसे युक्त जीवके केवल कर्मबन्ध ही होता है । इसके सिवाय कोई थोड़ा भी गुण ऐसा नहीं होता, जो इस लोक और परलोकमें कल्याणकारी हो।
__ भावार्थ-रागी और द्वेषी मनुष्य अपनी राग-द्वेषमयी परणतिके कारण निरन्तर कर्मबन्ध ही किया करता है । कर्मबन्धके कारण उसका संसार-वास हल्का नहीं हो पाता, और वह सदैव सांसारिक कष्टों का ही सामना किया करता है। इस राग-द्वेषपूर्ण परिणतिसे उसका तनिक भी कल्याण नहीं होता।
'कथं पुमः कर्मबन्धादन्यो गुणो नास्ति ? ' इति विभावयन्नाहकर्मबन्ध होनेके सिवाय अन्य गुण न होनेका कारण बतलाते हैं:
यस्मिन्निन्द्रियविषये शुभमशुभं वा निवेशयति भावम् ।
रक्तो वा द्विष्टो वा स बन्धहेतुर्भवति तस्य ॥ ५४॥
टीका-शब्दादिके विषये भाव-चित्तपरिणाम शुभमिष्टं रागयुतो निवेशयति । अशुभं वाऽनिष्टं भावं द्वेषयुतः स्थापयति । स स भावस्तस्यात्मनो ज्ञानावरणादिकर्मणोऽष्टविधस्य बन्धहेतुर्भवति। 'सकषायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् आदत्तेस बन्धः' इति वचनात् ॥५४॥
अर्थ-जिस इन्द्रियके विषयमें इष्ट अथवा अनिष्ट भावको करता है, राग अथवा द्वेषसे युक्त होनेके कारण उसका वह भाव बन्धका ही हेतु होता है।
भावार्थ-तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है कि-'जीव कषायसे युक्त होनेके कारण कर्मोंके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण करता है, इसीको बन्ध कहते हैं।' अतः जब जीव किसी इन्द्रियके विषयमें राग अथवा द्वेष करता है तो उसके कर्मबन्धके सिवाय ओर क्या हो सकता है ?
कथं पुनरात्मप्रदेशेषु कर्मपुद्गला लगन्ति ?' इत्याह...: बात्माके प्रदेशोंसे कर्मपुद्गल किस प्रकार चिपटते हैं । यह बतलाते हैं: