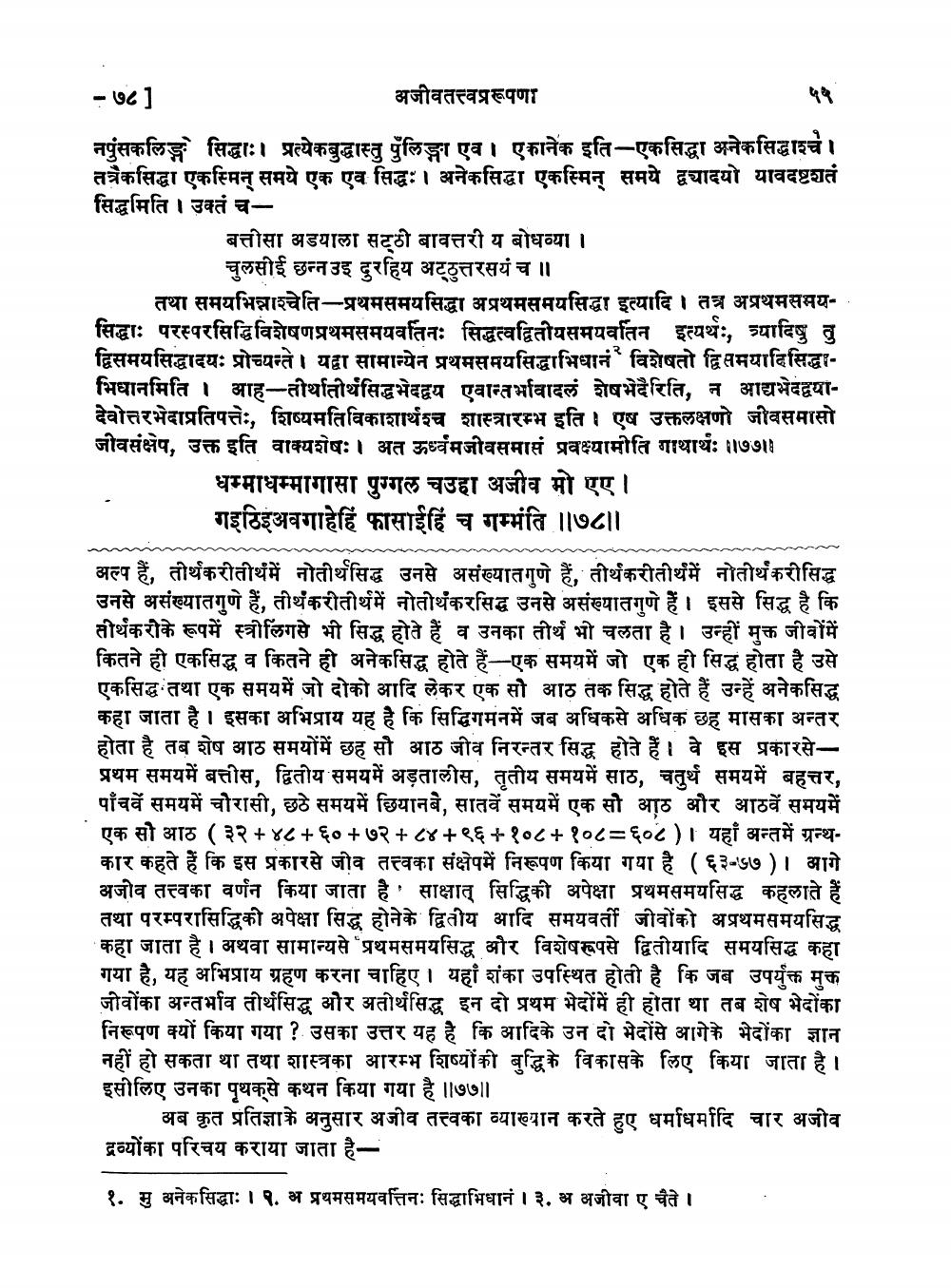________________
-७८]
अजीवतत्वप्ररूपणा नपुंसकलिङ्ग सिद्धाः। प्रत्येकबुद्धास्तु पुंलिङ्गा एव । एकानेक इति-एकसिद्धा अनेकसिद्धाश्चे। तत्रैकसिद्धा एकस्मिन् समये एक एव सिद्धः । अनेकसिद्धा एकस्मिन् समये द्वयादयो यावदष्टशतं सिद्धमिति । उक्तं च
बत्तीसा अडयाला सट्ठी बावत्तरी य बोधव्या ।
चुलसीई छन्न उइ दुरहिय अठुत्तरसयं च ॥ तथा समयभिन्नाश्चेति-प्रथमसमयसिद्धा अप्रथमसमयसिद्धा इत्यादि । तत्र अप्रथमसमयसिद्धाः परस्परसिद्धिविशेषणप्रथमसमयतिनः सिद्धत्वद्वितीयसमयतिन इत्यर्थः, ज्यादिषु तु द्विसमयसिद्धादयःप्रोच्यन्ते। यद्वा सामान्येन प्रथमसमयसिद्धाभिधानं विशेषतो द्विसमयादिसिद्धाभिधानमिति । आह-तीर्थातीर्थसिद्धभेदद्वय एवान्तर्भावादलं शेषभेदैरिति, न आद्यभेदद्वयादेवोत्तरभेदाप्रतिपत्तेः, शिष्यमतिविकाशार्थश्च शास्त्रारम्भ इति । एष उक्तलक्षणो जीवसमासो जीवसंक्षेप, उक्त इति वाक्यशेषः। अत ऊर्ध्वमजीवसमासं प्रवक्ष्यामीति गाथार्थः ॥७॥
धम्माधम्मागासा पुग्गल चउहा अजीव मो एए। गइठिइअवगाहेहिं फासाईहिं च गम्भंति ॥७८॥
अल्प हैं, तीर्थकरीतीर्थमें नोतीर्थसिद्ध उनसे असंख्यातगुणे हैं, तीर्थकरीतीर्थमें नोतीर्थकरीसिद्ध उनसे असंख्यातगुणे हैं, तीर्थकरीतीर्थमें नोतीथंकरसिद्ध उनसे असंख्यातगुणे हैं। इससे सिद्ध है कि तीर्थकरोके रूपमें स्त्रीलिंगसे भी सिद्ध होते हैं व उनका तीर्थ भी चलता है। उन्हीं मुक्त जीवोंमें कितने ही एकसिद्ध व कितने ही अनेकसिद्ध होते हैं—एक समयमें जो एक ही सिद्ध होता है उसे एकसिद्ध तथा एक समय में जो दोको आदि लेकर एक सौ आठ तक सिद्ध होते हैं उन्हें अनेकसिद्ध कहा जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि सिद्धिगमनमें जब अधिकसे अधिक छह मासका अन्तर होता है तब शेष आठ समयोंमें छह सौ आठ जीव निरन्तर सिद्ध होते हैं। वे इस प्रकारसेप्रथम समयमें बत्तीस, द्वितीय समयमें अड़तालीस, तृतीय समयमें साठ, चतुर्थ समयमें बहत्तर, पाँचवें समयमें चौरासी, छठे समयमें छियानबै, सातवें समयमें एक सौ आठ और आठवें समयमें एक सौ आठ (३२ + ४८ + ६० + ७२ + ८४ +९६+ १०८+ १०८= ६०८)। यहाँ अन्तमें ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकारसे जीव तत्त्वका संक्षेपमें निरूपण किया गया है (६३-७७ )। आगे अजीव तत्त्वका वर्णन किया जाता है। साक्षात् सिद्धिकी अपेक्षा प्रथमसमयसिद्ध कहलाते हैं तथा परम्परासिद्धिकी अपेक्षा सिद्ध होनेके द्वितीय आदि समयवर्ती जीवोंको अप्रथमसमयसिट कहा जाता है । अथवा सामान्यसे प्रथमसमयसिद्ध और विशेषरूपसे द्वितीयादि समयसिद्ध कहा गया है, यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए। यहाँ शंका उपस्थित होती है कि जब उपर्युक्त मुक्त जीवोंका अन्तर्भाव तीर्थसिद्ध और अतीर्थसिद्ध इन दो प्रथम भेदोंमें ही होता था तब शेष भेदोंका निरूपण क्यों किया गया? उसका उत्तर यह है कि आदिके उन दो भेदोंसे आगेके भेदोंका ज्ञान नहीं हो सकता था तथा शास्त्रका आरम्भ शिष्योंकी बुद्धि के विकासके लिए किया जाता है। इसीलिए उनका पृथक्से कथन किया गया है ।।७७॥
अब कृत प्रतिज्ञाके अनुसार अजीव तत्त्वका व्याख्यान करते हुए धर्माधर्मादि चार अजीव द्रव्योंका परिचय कराया जाता है
१. मु अनेकसिद्धाः । . अ प्रथमसमयत्तिनः सिद्धाभिधानं । ३. अ अजीवा ए चैते ।