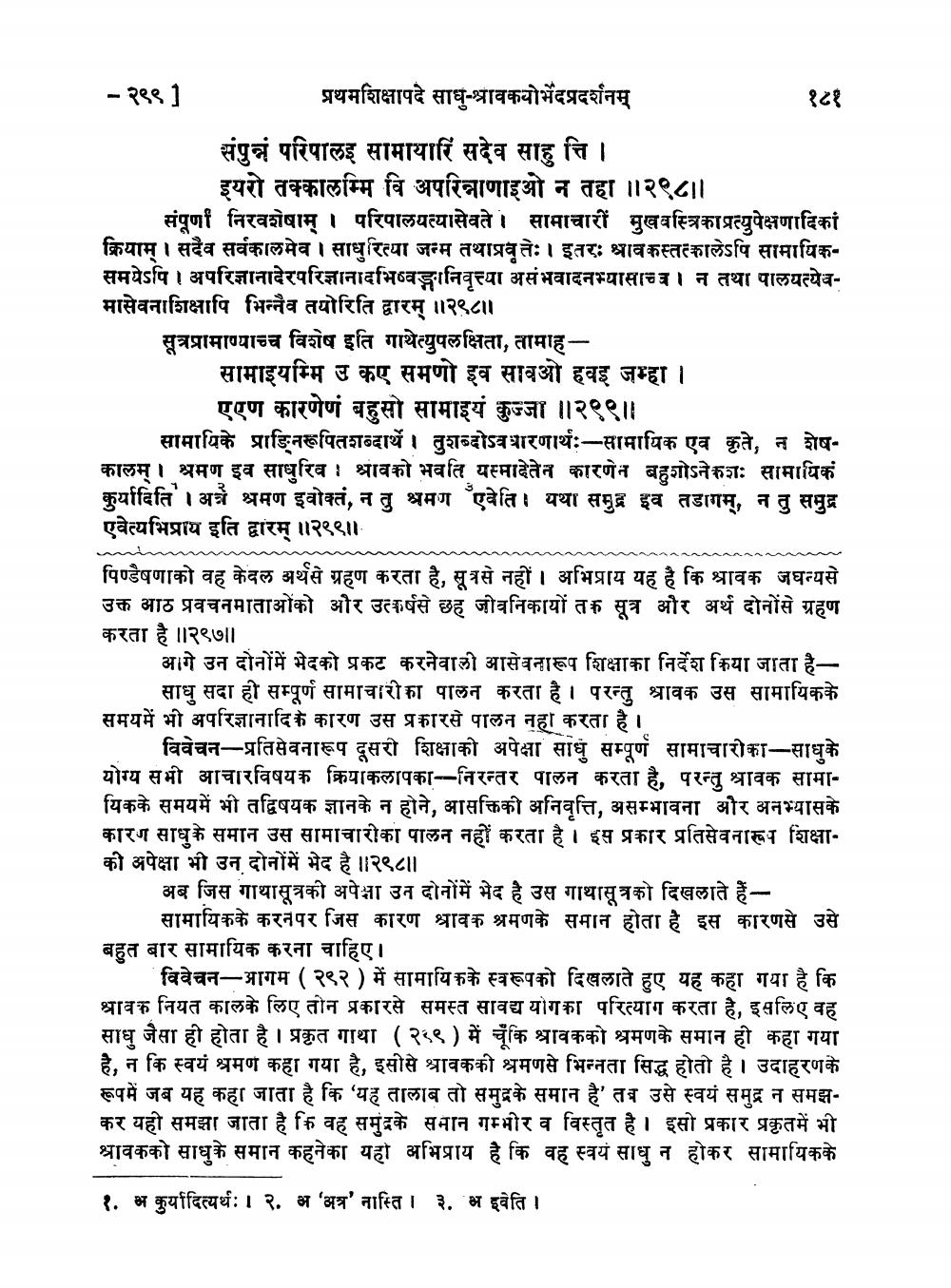________________
- २९९ ]
प्रथमशिक्षापदे साधु श्रावकयोर्भेदप्रदर्शनम्
संपुन परिपालइ सामायारिं सदेव साहु ति । saratoमिव अपरिन्नाणाइओ न तहा || २९८ ||
१८१
संपूर्णां निरवशेषाम् । परिपालयत्यासेवते । सामाचारों मुखवस्त्रिका प्रत्युपेक्षणादिकां क्रियाम् । सदैव सर्वकालमेव । साधुरित्या जन्म तथाप्रवृत्तेः । इतरः श्रावकस्तत्कालेऽपि सामायिकसमयेऽपि । अपरिज्ञानादेरपरिज्ञानादभिष्वङ्गानिवृत्त्या असंभवादनभ्यासाच्च । न तथा पालयत्येवमासेवनाशिक्षापि भिन्नैव तयोरिति द्वारम् ॥ २९८ ॥
सूत्रप्रामाण्याच्च विशेष इति गाथेत्युपलक्षिता, तामाह
सामाइयम्म उकए समणो इव सावओ हवइ जम्हा । एएण कारणं बहुसो सामाइयं कुज्जा ॥ २९९ ॥
सामायिके प्रानिरूपितशब्दार्थे । तुशब्दोऽवधारणार्थ:- सामायिक एव कृते, न शेषकालम् । श्रमण इव साधुरिव । श्रावको भवति यस्मादेतेन कारणेन बहुशोऽनेकशः सामायिक कुर्यादिति । अत्रे श्रमण इवोक्तं, न तु श्रमण एवेति । यथा समुद्र इव तडागम्, न तु समुद्र एवेत्यभिप्राय इति द्वारम् ॥ २९९ ॥
पिण्डैषणाको वह केवल अर्थ से ग्रहण करता है, सूत्र से नहीं । अभिप्राय यह है कि श्रावक जघन्यसे उक्त आठ प्रवचनमाताओंको और उत्कर्षसे छह जीवनिकायों तक सूत्र और अर्थ दोनोंसे ग्रहण करता है ||२९७||
आगे उन दोनों में भेदको प्रकट करनेवाली आसेवनारूप शिक्षाका निर्देश किया जाता हैसाधु सदा ही सम्पूर्ण सामाचारीका पालन करता है । परन्तु श्रावक उस सामायिक के समय में भी अपरिज्ञानादिके कारण उस प्रकारसे पालन नहीं करता है ।
विवेचन – प्रतिसेवनारूप दूसरी शिक्षाको अपेक्षा साधु सम्पूर्ण सामाचारीका - साधुके योग्य सभी आचारविषयक क्रियाकलापका - निरन्तर पालन करता है, परन्तु श्रावक सामाकिके समय में भी तद्विषयक ज्ञानके न होने, आसक्तिकी अनिवृत्ति, असम्भावना और अनभ्यासके कारण साधु के समान उस सामाचारीका पालन नहीं करता है। इस प्रकार प्रतिसेवनारूप शिक्षाकी अपेक्षा भी उन दोनों में भेद है || २९८ ॥
अब जिस गाथासूत्रकी अपेक्षा उन दोनों में भेद है उस गाथासूत्र को दिखलाते हैं
सामायिक करने पर जिस कारण श्रावक श्रमणके समान होता है इस कारण से उसे बहुत बार सामायिक करना चाहिए।
विवेचन - आगम (२९२ ) में सामायिक के स्वरूपको दिखलाते हुए यह कहा गया है कि श्रावक नियत कालके लिए तीन प्रकारसे समस्त सावद्य योगका परित्याग करता है, इसलिए वह साधु जैसा ही होता है । प्रकृत गाथा ( २९९ ) में चूँकि श्रावकको श्रमणके समान ही कहा गया है, न कि स्वयं श्रमण कहा गया है, इसीसे श्रावककी श्रमणसे भिन्नता सिद्ध होती है । उदाहरण के रूप में जब यह कहा जाता है कि 'यह तालाब तो समुद्र के समान है' तत्र उसे स्वयं समुद्र न समझकर यही समझा जाता है कि वह समुद्रके समान गम्भीर व विस्तृत है । इसी प्रकार प्रकृतमें भी श्रावकको साधु के समान कहने का यहो अभिप्राय है कि वह स्वयं साधु न होकर सामायिक के
१. अ कुर्यादित्यर्थः । २ अ 'अत्र' नास्ति । ३. अ इवेति ।