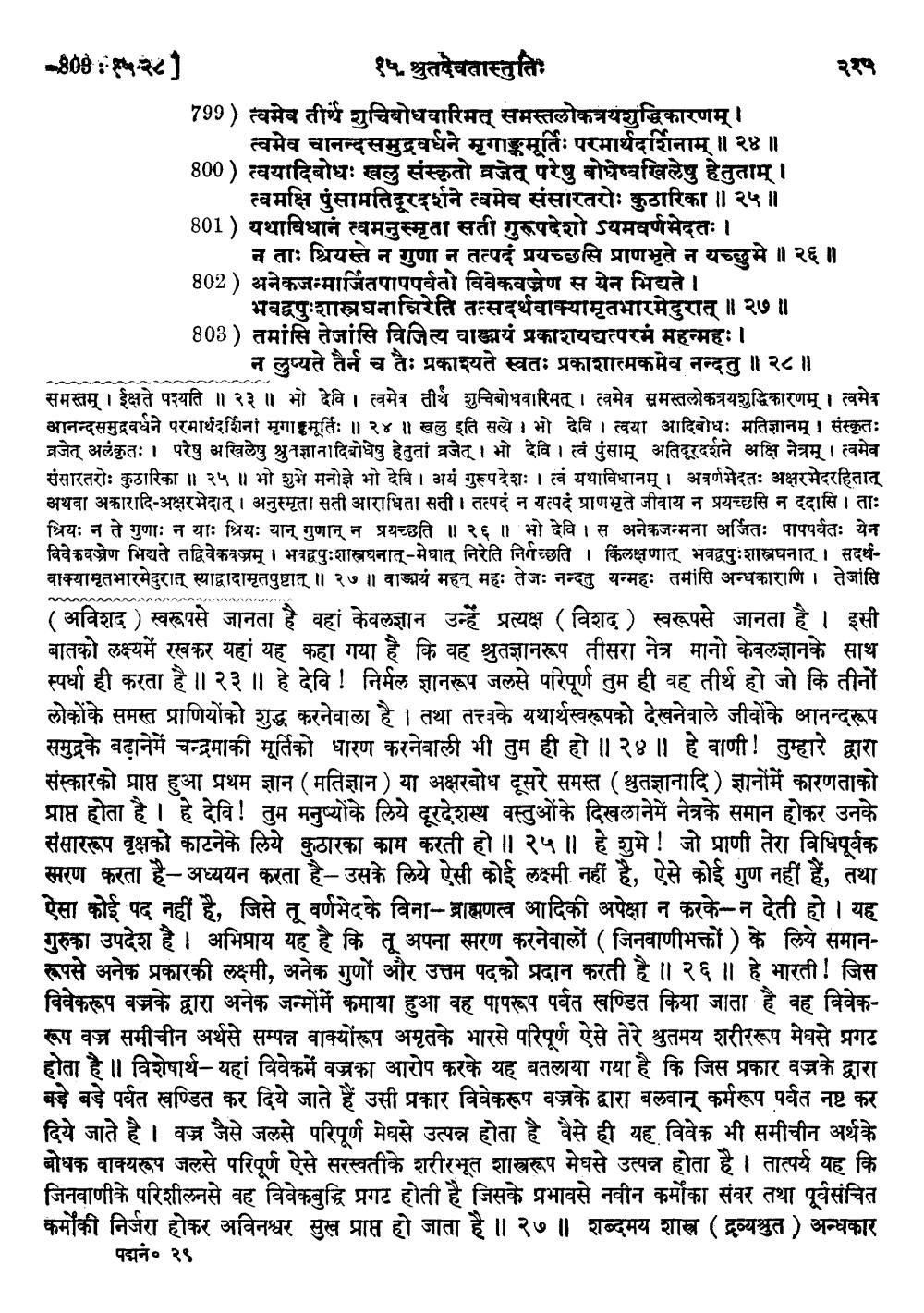________________
२५५
-808:१५२८]
१५. श्रुतदेवतास्तुतिः 799 ) त्वमेव तीर्थ शुचियोधवारिमत् समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम् ।
त्वमेव चानन्दसमुद्रवर्धने मृगाङ्कमूर्तिः परमार्थदर्शिनाम् ॥ २४ ॥ 800 ) त्वयादिवोधः खलु संस्कृतो व्रजेत् परेषु बोधेवखिलेषु हेतुताम् ।
त्वमक्षि पुंसामतिदूरदर्शने त्वमेव संसारतरोः कुठारिका ॥२५॥ 801) यथाविधानं त्वमनुस्मृता सती गुरूपदेशो ऽयमवर्णमेदतः।
न ताः श्रियस्ते न गुणा न तत्पदं प्रयच्छसि प्राणभृते न यच्छुभे ॥ २६ ॥ 802) अनेकजन्मार्जितपापपर्वतो विवेकवज्रेण स येन भिद्यते।
भवद्वपुःशास्त्रघनान्निरेति तत्सदर्थवाक्यामृतभारमेदुरात् ॥ २७॥ 803) तमांसि तेजांसि विजित्य वाडमयं प्रकाशयद्यत्परमं महन्महः।
न लुप्यते तैर्न च तैः प्रकाश्यते स्वतः प्रकाशात्मकमेव नन्दतु ॥२८॥ समस्तम् । ईक्षते पश्यति ॥ २३ ॥ भो देवि । त्वमेव तीर्थ शुचिबोधवारिमत् । त्वमेव समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम् । त्वमेव आनन्दसमुद्रवर्धने परमार्थदर्शिनां मृगामूर्तिः ॥ २४ ॥ खलु इति सत्ये। भो देवि । त्वया आदिबोधः मतिज्ञानम्। संस्कृतः व्रजेत् अलंकृतः। परेषु अखिलेषु श्रुतज्ञानादिबोधेषु हेतुतां व्रजेत् । भो देवि । त्वं पुंसाम् अतिदूरदर्शने अक्षि नेत्रम् । त्वमेव संसारतरोः कुठारिका ॥ २५ ॥ भो शुभे मनोज्ञे भो देवि। अयं गुरूपदेशः । त्वं यथाविधानम् । अवर्णभेदतः अक्षरभेदरहितात् अथवा अकारादि-अक्षरभेदात् । अनुस्मृता सती आराधिता सती। तत्पदं न यत्पदं प्राणभृते जीवाय न प्रयच्छसि न ददासि । ताः श्रियः न ते गुणाः न याः श्रियः यान् गुणान् न प्रयच्छति ॥ २६ ॥ भो देवि । स अनेकजन्मना अर्जितः पापपर्वतः येन विवेकवज्रेण भिद्यते तद्विवेकवज्रम् । भवद्वपुःशास्त्रघनात्-मेघात् निरेति निर्गच्छति । किंलक्षणात् भवद्वपुःशास्त्रघनात् । सदर्थवाक्यामृतभारमेदुरात् स्याद्वादामृतपुष्टात् ॥ २७ ॥ वाङ्मयं महत् महः तेजः नन्दतु यन्महः तमांसि अन्धकाराणि । तेजासि ( अविशद ) स्वरूपसे जानता है वहां केवलज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष (विशद ) स्वरूपसे जानता है । इसी बातको लक्ष्यमें रखकर यहां यह कहा गया है कि वह श्रुतज्ञानरूप तीसरा नेत्र मानो केवलज्ञानके साथ स्पर्धा ही करता है ॥ २३ ॥ हे देवि ! निर्मल ज्ञानरूप जलसे परिपूर्ण तुम ही वह तीर्थ हो जो कि तीनों लोकोंके समस्त प्राणियोंको शुद्ध करनेवाला है । तथा तत्त्वके यथार्थस्वरूपको देखनेवाले जीवोंके आनन्दरूप समुद्रके बढ़ानेमें चन्द्रमाकी मूर्तिको धारण करनेवाली भी तुम ही हो ॥ २४ ॥ हे वाणी! तुम्हारे द्वारा संस्कारको प्राप्त हुआ प्रथम ज्ञान ( मतिज्ञान) या अक्षरबोध दूसरे समस्त (श्रुतज्ञानादि) ज्ञानोंमें कारणताको प्राप्त होता है । हे देवि! तुम मनुष्योंके लिये दूरदेशस्थ वस्तुओंके दिखलानेमें नेत्रके समान होकर उनके संसाररूप वृक्षको काटनेके लिये कुठारका काम करती हो ॥ २५॥ हे शुभे ! जो प्राणी तेरा विधिपूर्वक स्मरण करता है- अध्ययन करता है- उसके लिये ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं है, ऐसे कोई गुण नहीं हैं, तथा ऐसा कोई पद नहीं है, जिसे तू वर्णभेदके विना-ब्राह्मणत्व आदिकी अपेक्षा न करके-न देती हो । यह गुरुका उपदेश है। अभिप्राय यह है कि तू अपना स्मरण करनेवालों (जिनवाणीभक्तों) के लिये समानरूपसे अनेक प्रकारकी लक्ष्मी, अनेक गुणों और उत्तम पदको प्रदान करती है ॥ २६ ॥ हे भारती! जिस विवेकरूप वज्रके द्वारा अनेक जन्मोंमें कमाया हुआ वह पापरूप पर्वत खण्डित किया जाता है वह विवेकरूप वज्र समीचीन अर्थसे सम्पन्न वाक्योंरूप अमृतके भारसे परिपूर्ण ऐसे तेरे श्रुतमय शरीररूप मेघसे प्रगट होता है। विशेषार्थ- यहां विवेकमें वज्रका आरोप करके यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार वज्रके द्वारा बड़े बड़े पर्वत खण्डित कर दिये जाते हैं उसी प्रकार विवेकरूप वज्रके द्वारा बलवान् कर्मरूप पर्वत नष्ट कर दिये जाते है। वज्र जैसे जलसे परिपूर्ण मेघसे उत्पन्न होता है वैसे ही यह विवेक भी समीचीन अर्थके बोधक वाक्यरूप जलसे परिपूर्ण ऐसे सरस्वतीके शरीरभूत शास्त्ररूप मेघसे उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह कि जिनवाणीके परिशीलनसे वह विवेकबुद्धि प्रगट होती है जिसके प्रभावसे नवीन कर्मोंका संवर तथा पूर्वसंचित कर्मोंकी निर्जरा होकर अविनश्वर सुख प्राप्त हो जाता है ॥ २७ ॥ शब्दमय शास्त्र (द्रव्यश्रुत) अन्धकार
पद्मनं. २९