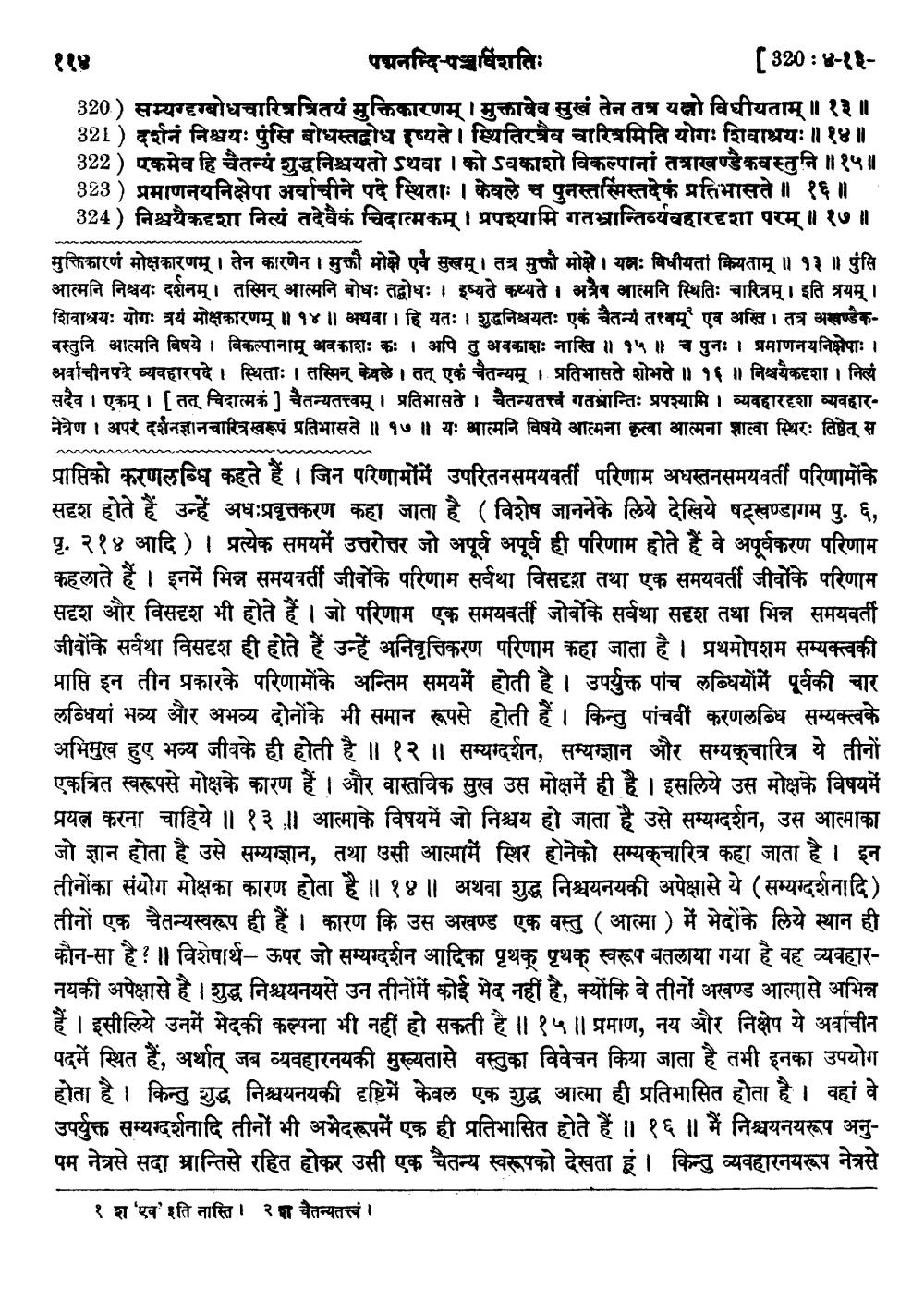________________
१९५ पभनन्दि-पञ्चविंशतिः
[320 : ४-१६ 320) सम्यग्दृग्बोधचारित्रत्रितयं मुक्तिकारणम् । मुक्तावेव सुखं तेन तत्र यनो विधीयताम् ॥ १३ ॥ 321 ) दर्शनं निश्चयः पुंसि बोधस्तद्वोध इष्यते । स्थितिरत्रैव चारित्रमिति योगः शिवाश्रयः ॥१४॥ 322) एकमेव हि चैतन्यं शुद्धनिश्चयतोऽथवा । कोऽवकाशो विकल्पानां तत्राखण्डैकवस्तुनि ॥१५॥ 323) प्रमाणनयनिक्षेपा अर्वाचीने पदे स्थिताः । केवले च पुनस्तस्मिंस्तदेकं प्रतिभासते ॥ १६॥
324) निश्चयैकदशा नित्यं तदेवैकं चिदात्मकम् । प्रपश्यामि गतभ्रान्तिर्व्यवहारदृशा परम् ॥ १७ ॥ मुक्तिकारणं मोक्षकारणम् । तेन कारणेन । मुक्ती मोक्षे एवं सुखम्। तत्र मुचौ मोक्षे। यमः विधीयतां क्रियताम् ॥ १३ ॥ पुंसि आत्मनि निश्चयः दर्शनम्। तस्मिन् आत्मनि बोधः तद्बोधः । इष्यते कथ्यते। अत्रैव आत्मनि स्थितिः चारित्रम् । इति त्रयम् । शिवाश्रयः योगः त्रयं मोक्षकारणम् ॥ १४॥ अथवा । हि यतः । शुद्धनिश्चयतः एकं चैतन्य तत्वम् एव अस्ति । तत्र अखण्डेकवस्तुनि आत्मनि विषये। विकल्पानाम् अवकाशः कः । अपि तु अवकाशः नाति ॥१५॥ च पुनः। प्रमाणनयनि अर्वाचीनपदे व्यवहारपदे। स्थिताः । तस्मिन् केवले। तत् एकं चैतन्यम् । प्रतिभासते शोभते ॥१६॥ निश्चयकरशा। नित्यं सदैव । एकम् । [तत् चिदात्मकं] चैतन्यतत्त्वम् । प्रतिभासते। चैतन्यतत्त्वं गतम्रान्तिः प्रपश्यामि । व्यवहारदृशा व्यवहारनेत्रेण । अपरं दर्शनज्ञानचारित्रखरूपं प्रतिभासते ॥ १७ ॥ यः भात्मनि विषये आत्मना कृत्वा आत्मना ज्ञात्वा स्थिरः तिष्ठेत् स प्राप्तिको करणलब्धि कहते हैं । जिन परिणामोंमें उपरितनसमयवर्ती परिणाम अधस्तनसमयवर्ती परिणामोंके सदृश होते हैं उन्हें अधःप्रवृत्तकरण कहा जाता है (विशेष जाननेके लिये देखिये षट्खण्डागम पु. ६, पृ. २१४ आदि) । प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर जो अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होते हैं वे अपूर्वकरण परिणाम कहलाते हैं। इनमें भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम सर्वथा विसदृश तथा एक समयवर्ती जीवोंके परिणाम सदृश और विसदृश भी होते हैं । जो परिणाम एक समयवर्ती जोवोंके सर्वथा सदृश तथा भिन्न समयवर्ती जीवोंके सर्वथा विसदृश ही होते हैं उन्हें अनिवृत्तिकरण परिणाम कहा जाता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति इन तीन प्रकारके परिणामोंके अन्तिम समयमें होती है। उपर्युक्त पांच लब्धियोंमें पूर्वकी चार लब्धियां भव्य और अभव्य दोनोंके भी समान रूपसे होती हैं। किन्तु पांचवीं करणलब्धि सम्यक्त्वके अभिमुख हुए भव्य जीवके ही होती है ॥ १२॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों एकत्रित स्वरूपसे मोक्षके कारण हैं । और वास्तविक सुख उस मोक्षमें ही है। इसलिये उस मोक्षके विषयमें प्रयत्न करना चाहिये ॥ १३ ॥ आत्माके विषयमें जो निश्चय हो जाता है उसे सम्यग्दर्शन, उस आत्माका जो ज्ञान होता है उसे सम्यग्ज्ञान, तथा उसी आत्मामें स्थिर होनेको सम्यक्चारित्र कहा जाता है। इन तीनोंका संयोग मोक्षका कारण होता है ॥ १४ ॥ अथवा शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे ये (सम्यग्दर्शनादि) तीनों एक चैतन्यस्वरूप ही हैं। कारण कि उस अखण्ड एक वस्तु ( आत्मा ) में भेदोंके लिये स्थान ही कौन-सा है ? ॥ विशेषार्थ- ऊपर जो सम्यग्दर्शन आदिका पृथक पृथक् स्वरूप बतलाया गया है वह व्यवहारनयकी अपेक्षासे है। शुद्ध निश्चयनयसे उन तीनोंमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि वे तीनों अखण्ड आत्मासे अभिन्न हैं । इसीलिये उनमें भेदकी कल्पना भी नहीं हो सकती है ।। १५॥ प्रमाण, नय और निक्षेप ये अर्वाचीन पदमें स्थित हैं, अर्थात् जब व्यवहारनयकी मुख्यतासे वस्तुका विवेचन किया जाता है तभी इनका उपयोग होता है। किन्तु शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिमें केवल एक शुद्ध आत्मा ही प्रतिभासित होता है। वहां वे उपर्युक्त सम्यग्दर्शनादि तीनों भी अभेदरूपमें एक ही प्रतिभासित होते हैं ॥ १६ ॥ मैं निश्चयनयरूप अनुपम नेत्रसे सदा प्रान्तिसे रहित होकर उसी एक चैतन्य स्वरूपको देखता हूं। किन्तु व्यवहारनयरूप नेत्रसे
१ श एव' इति नास्ति । २श चैतन्यतत्त्वं ।