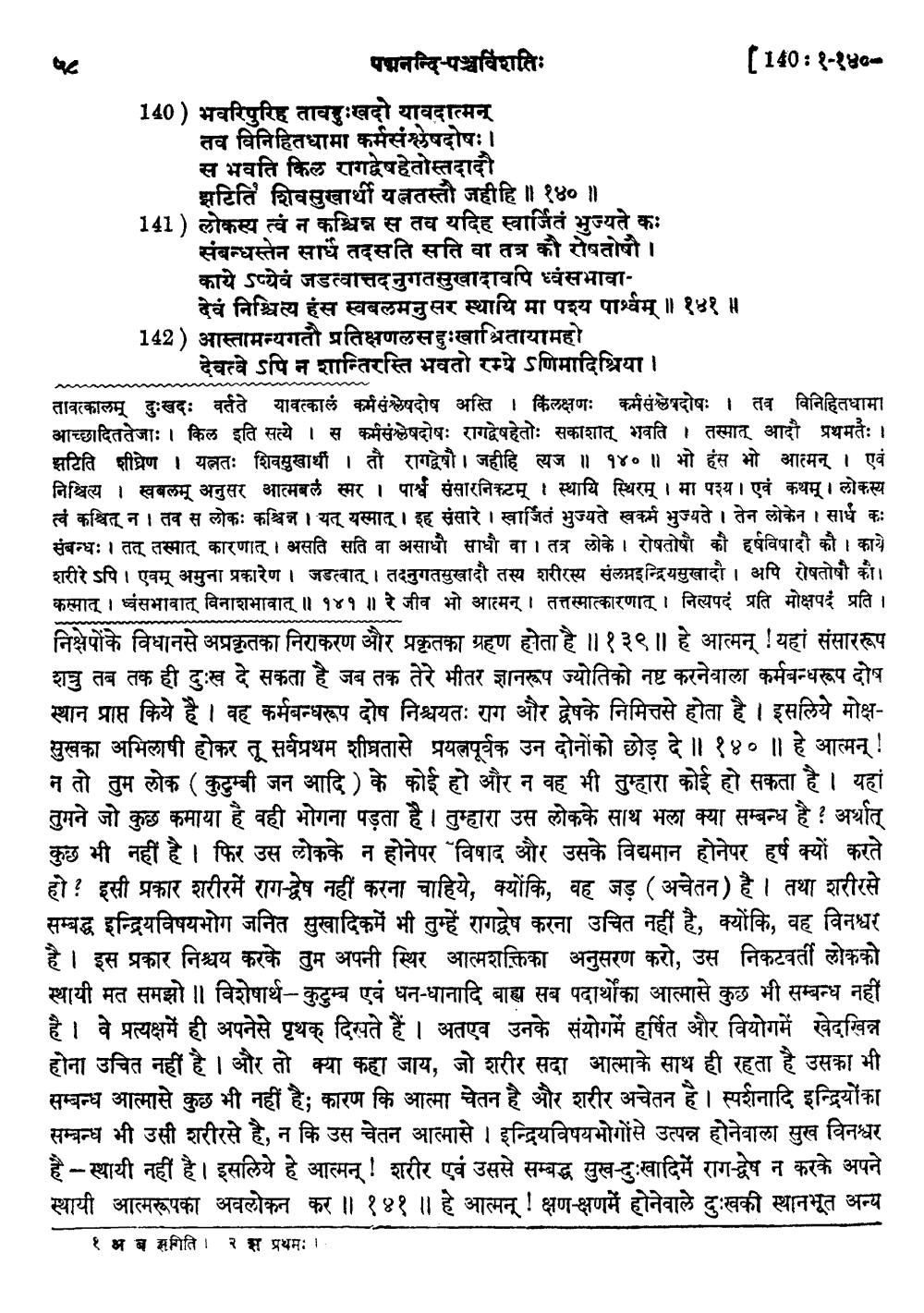________________
पननन्दि-पञ्चविंशतिः
[140:१-२४०140) भवरिपुरिह तावहुःखदो यावदात्मन्
तव विनिहितधामा कर्मसंश्लेषदोषः। स भवति किल रागद्वेषहेतोस्तदादौ
झटिति शिवसुखार्थी यत्नतस्तौ जहीहि ॥ १४० ॥ 141) लोकस्य त्वं न कश्चिन्न स तव यदिह स्वार्जितं भुज्यते कः
संबन्धस्तेन साधं तदसति सति वा तत्र को रोषतोषौ । काये ऽप्येवं जडत्वात्तदनुगतसुखादावपि ध्वसभावा
देवं निश्चित्य हंस स्वबलमनुसर स्थायि मा पश्य पार्श्वम् ॥ १४१ ।। 142) आस्तामन्यगतौ प्रतिक्षणलसदुःखाश्रितायामहो
देवत्वे ऽपि न शान्तिरस्ति भवतो रम्ये ऽणिमादिश्रिया। तावत्कालम् दुःखदः वर्तते यावत्कालं कर्मसंश्लेषदोष अस्ति । किलक्षणः कर्मसंश्लेषदोषः । तव विनिहितधामा आच्छादिततेजाः। किल इति सत्ये । स कर्मसंश्लेषदोषः रागद्वेषहेतोः सकाशात् भवति । तस्मात् आदी प्रथमतः । झटिति शीघ्रण । यत्नतः शिवमुखार्थी । तौ रागद्वेषौ । जहीहि त्यज ॥ १४० ॥ भो हंस भो आत्मन् । एवं निश्चित्य । खबलम् अनुसर आत्मबलं स्मर । पार्श्व संसारनिकटम् । स्थायि स्थिरम् । मा पश्य । एवं कथम् । लोकस्य त्वं कश्चित् न । तव स लोकः कश्चिन्न । यत् यस्मात् । इह संसारे । वार्जितं भुज्यते स्वकर्म भुज्यते। तेन लोकेन । सार्ध कः संबन्धः । तत् तस्मात् कारणात् । असति सति वा असाधौ साधौ वा। तत्र लोके । रोषतोषौ को हर्षविषादौ कौ । काये शरीरे ऽपि । एवम् अमुना प्रकारेण । जडत्वात् । तदनुगतसुखादौ तस्य शरीरस्य संलमइन्द्रियसुखादौ । अपि रोषतोषी को। कस्मात् । ध्वंसभावात् विनाशभावात् ॥ १४१ ॥ रे जीव भो आत्मन् । तत्तस्मात्कारणात् । नित्यपदं प्रति मोक्षपदं प्रति । निक्षेपोंके विधानसे अप्रकृतका निराकरण और प्रकृतका ग्रहण होता है ॥१३९॥ हे आत्मन् ! यहां संसाररूप शत्रु तब तक ही दुःख दे सकता है जब तक तेरे भीतर ज्ञानरूप ज्योतिको नष्ट करनेवाला कर्मबन्धरूप दोष स्थान प्राप्त किये है । वह कर्मबन्धरूप दोष निश्चयतः राग और द्वेषके निमित्तसे होता है । इसलिये मोक्षसुखका अभिलाषी होकर तू सर्वप्रथम शीघ्रतासे प्रयत्नपूर्वक उन दोनोंको छोड़ दे ॥ १४० ॥ हे आत्मन् ! न तो तुम लोक ( कुटुम्बी जन आदि) के कोई हो और न वह भी तुम्हारा कोई हो सकता है। यहां तुमने जो कुछ कमाया है वही भोगना पड़ता है । तुम्हारा उस लोकके साथ भला क्या सम्बन्ध है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है। फिर उस लोकके न होनेपर विषाद और उसके विद्यमान होनेपर हर्ष क्यों करते हो ? इसी प्रकार शरीरमें राग-द्वेष नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह जड़ (अचेतन) है । तथा शरीरसे सम्बद्ध इन्द्रियविषयभोग जनित सुखादिकमें भी तुम्हें रागद्वेष करना उचित नहीं है, क्योंकि, वह विनश्वर है। इस प्रकार निश्चय करके तुम अपनी स्थिर आत्मशक्तिका अनुसरण करो, उस निकटवर्ती लोकको स्थायी मत समझो ॥ विशेषार्थ-कुटुम्ब एवं धन-धानादि बाह्य सब पदार्थों का आत्मासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। वे प्रत्यक्षमें ही अपनेसे पृथक् दिखते हैं । अतएव उनके संयोगमें हर्षित और वियोगमें खेदखिन्न होना उचित नहीं है । और तो क्या कहा जाय, जो शरीर सदा आत्माके साथ ही रहता है उसका भी सम्बन्ध आत्मासे कुछ भी नहीं है; कारण कि आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन है। स्पर्शनादि इन्द्रियोंका सम्बन्ध भी उसी शरीरसे है, न कि उस चेतन आत्मासे । इन्द्रियविषयभोगोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख विनश्वर है - स्थायी नहीं है। इसलिये हे आत्मन् ! शरीर एवं उससे सम्बद्ध सुख-दुःखादिमें राग-द्वेष न करके अपने स्थायी आत्मरूपका अवलोकन कर ॥ १४१ ॥ हे आत्मन् ! क्षण-क्षणमें होनेवाले दुःखकी स्थानभूत अन्य
१ अब झगिति। २ श प्रथमः ।