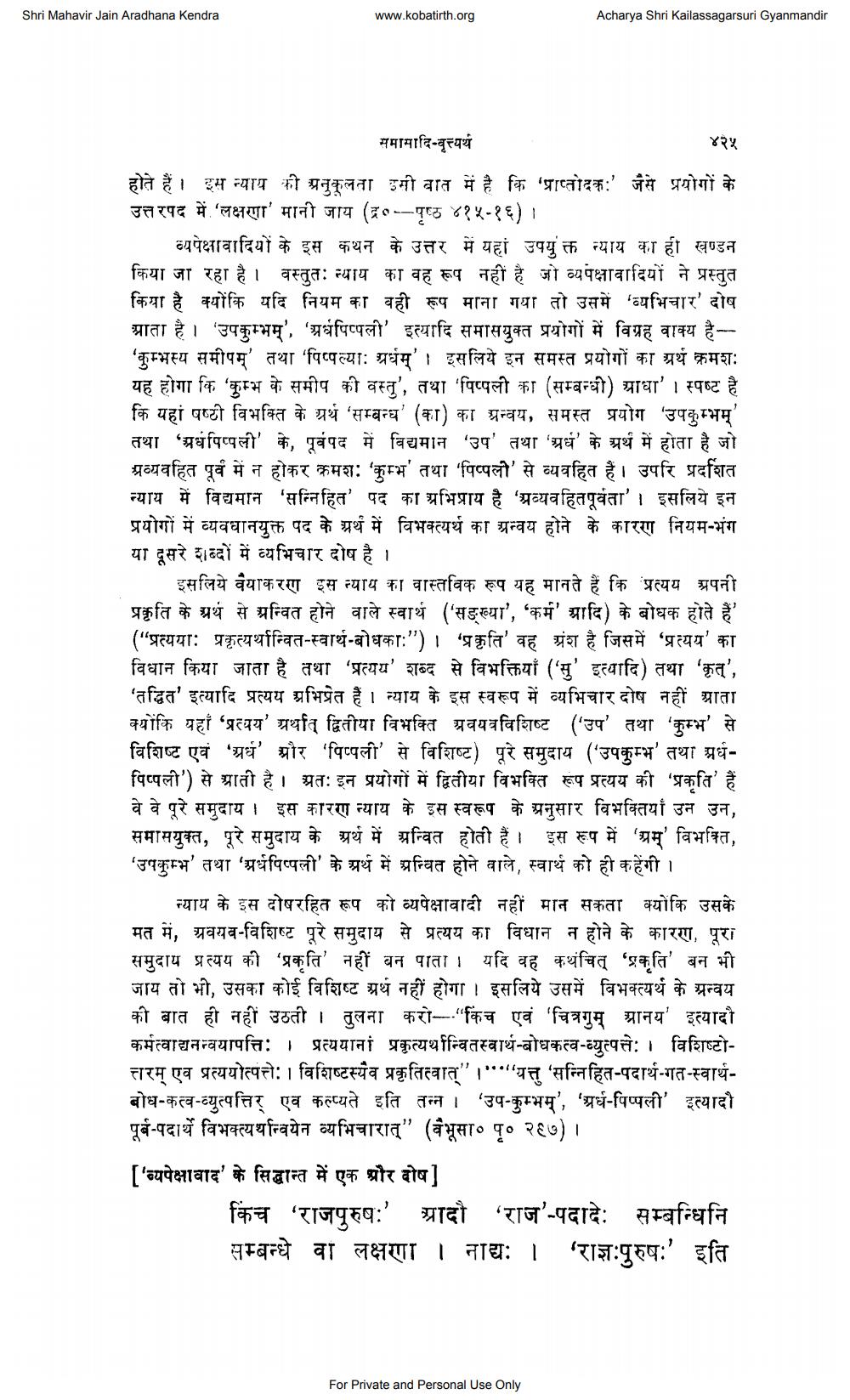________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
समामादि-वृत्त्यर्थ
४२५
होते हैं। इस न्याय की अनुकूलता इसी बात में है कि 'प्राप्तोदकः' जैसे प्रयोगों के उत्तरपद में लक्षरणा' मानी जाय (द्र० --पृष्ठ ४१५-१६) ।
व्यपेक्षावादियों के इस कथन के उत्तर में यहां उपयुक्त न्याय का ही खण्डन किया जा रहा है। वस्तुतः न्याय का वह रूप नहीं है जो व्यपेक्षावादियों ने प्रस्तुत किया है क्योंकि यदि नियम का बही रूप माना गया तो उसमें 'व्यभिचार' दोष
आता है। 'उपकुम्भम्', 'अर्धपिप्पली' इत्यादि समासयुक्त प्रयोगों में विग्रह वाक्य है-- 'कुम्भस्य समीपम्' तथा 'पिप्पल्या: अर्धम्'। इसलिये इन समस्त प्रयोगों का अर्थ क्रमशः यह होगा कि 'कुम्भ के समीप की वस्तु', तथा 'पिप्पली का (सम्बन्धी) प्राधा' । स्पष्ट है कि यहां षष्ठी विभक्ति के अर्थ 'सम्बन्ध' (का) का अन्वय, समस्त प्रयोग 'उपकुम्भम्' तथा 'अर्धपिप्पली' के, पूर्वपद में विद्यमान 'उप' तथा 'अर्ध' के अर्थ में होता है जो अव्यवहित पूर्व में न होकर क्रमश: 'कुम्भ' तथा 'पिप्पली' से व्यवहित हैं। उपरि प्रदर्शित न्याय में विद्यमान 'सन्निहित' पद का अभिप्राय है 'अव्यवहितपूर्वता'। इसलिये इन प्रयोगों में व्यवधानयुक्त पद के अर्थ में विभक्त्यर्थ का अन्वय होने के कारण नियम-भंग या दूसरे शब्दों में व्यभिचार दोष है ।
इसलिये वैयाकरण इस न्याय का वास्तविक रूप यह मानते हैं कि प्रत्यय अपनी प्रकृति के प्रथं से अन्वित होने वाले स्वार्थ ('सङ्ख्या ', 'कर्म' आदि) के बोधक होते हैं' ("प्रत्यया: प्रकृत्यर्थान्वित-स्वार्थ-बोधकाः")। 'प्रकृति' वह अंश है जिसमें 'प्रत्यय' का विधान किया जाता है तथा 'प्रत्यय' शब्द से विभक्तियाँ ('सु' इत्यादि) तथा 'कृत्', 'तद्धित' इत्यादि प्रत्यय अभिप्रेत हैं । न्याय के इस स्वरूप में व्यभिचार दोष नहीं आता क्योंकि यहाँ 'प्रत्यय' अर्थात् द्वितीया विभक्ति अवयव विशिष्ट ('उप' तथा 'कुम्भ' से विशिष्ट एवं 'अर्ध' और 'पिप्पली' से विशिष्ट) पूरे समुदाय ('उपकुम्भ' तथा अर्धपिप्पली') से आती है। अतः इन प्रयोगों में द्वितीया विभक्ति रूप प्रत्यय की 'प्रकृति' हैं वे वे पूरे समुदाय । इस कारण न्याय के इस स्वरूप के अनुसार विभक्तियाँ उन उन, समासयुक्त, पूरे समुदाय के अर्थ में अन्वित होती हैं। इस रूप में 'अम्' विभक्ति, 'उपकुम्भ' तथा 'अर्धपिप्पली' के अर्थ में अन्वित होने वाले, स्वार्थ को ही कहेंगी।
___ न्याय के इस दोषरहित रूप को व्यपेक्षावादी नहीं मान सकता क्योंकि उसके मत में, अवयव-विशिष्ट पूरे समुदाय से प्रत्यय का विधान न होने के कारण, पूरा समुदाय प्रत्यय की 'प्रकृति' नहीं बन पाता। यदि वह कथंचित् 'प्रकृति' बन भी जाय तो भी, उसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होगा। इसलिये उसमें विभक्त्यर्थ के अन्वय की बात ही नहीं उठती । तुलना करो-."किंच एवं 'चित्रगुम् अानय' इत्यादौ कर्मत्वाद्यनन्वयापत्तिः । प्रत्ययानां प्रकृत्यान्वितस्वार्थ-बोधकत्व-व्युत्पत्तेः। विशिष्टोत्तरम् एव प्रत्ययोत्पत्तेः । विशिष्टस्यैव प्रकृतित्वात्"।""यत्तु 'सन्निहित-पदार्थ-गत-स्वार्थबोध-कत्व-व्युत्पत्तिर् एव कल्प्यते इति तन्न । 'उप-कुम्भम्', 'अर्ध-पिप्पली' इत्यादौ पूर्व-पदार्थे विभक्त्यर्थान्वयेन व्यभिचारात्" (वैभूसा० पृ० २६७) । ['व्यपेक्षावाद' के सिद्धान्त में एक और दोष]
किंच 'राजपूरुषः' प्रादौ 'राज'-पदादेः सम्बन्धिनि सम्बन्धे वा लक्षणा । नाद्यः । 'राज्ञःपुरुषः' इति
For Private and Personal Use Only