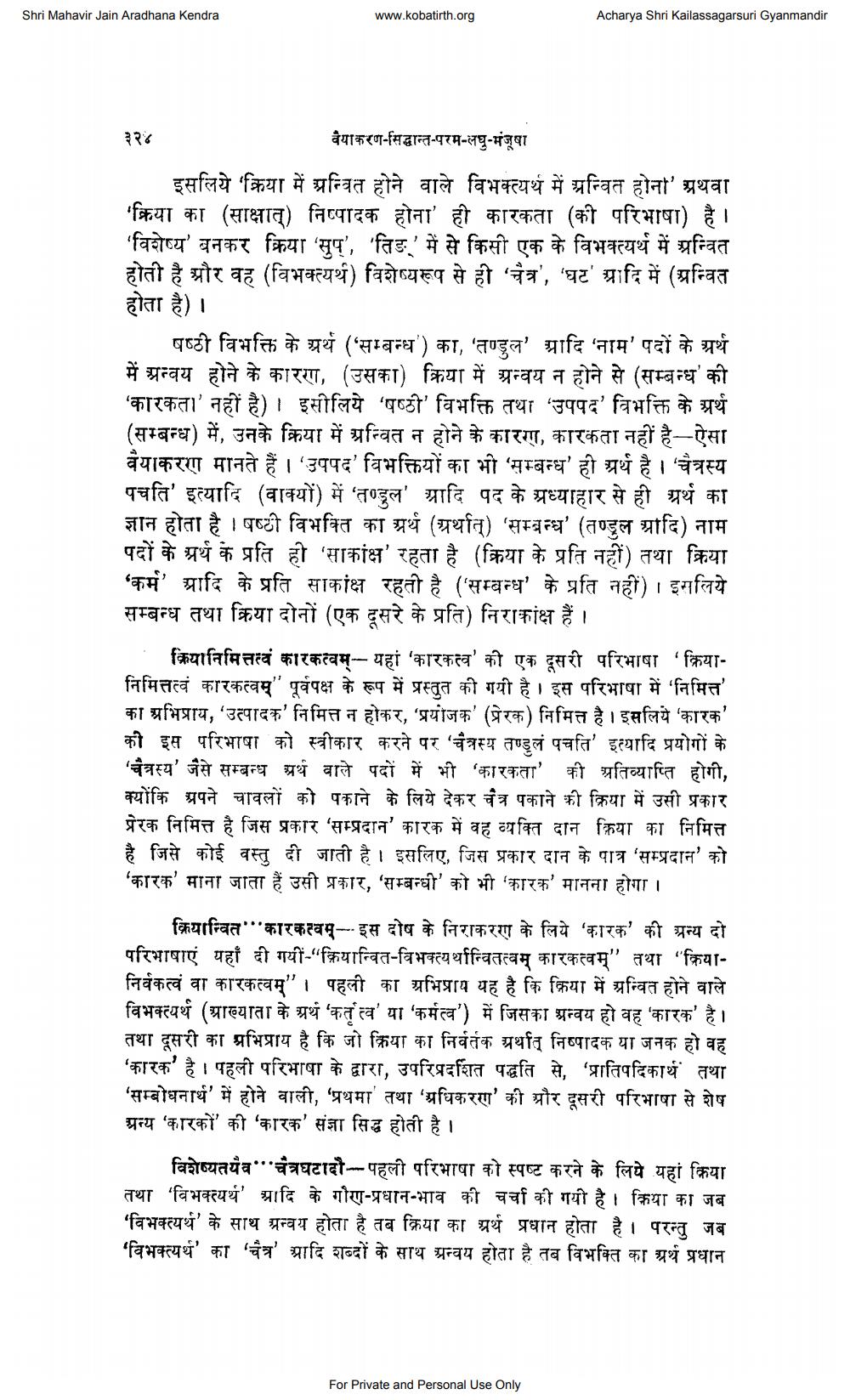________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
३२४
वैयाकरण-सिद्धान्त-परम-लघु-मंजूषा इसलिये 'क्रिया में अन्वित होने वाले विभक्त्यर्थ में अन्वित होना' अथवा 'क्रिया का (साक्षात्) निष्पादक होना' ही कारकता (की परिभाषा) है। 'विशेष्य' बनकर क्रिया ‘सुप्', 'तिङ' में से किसी एक के विभक्त्यर्थ में अन्वित होती है और वह (विभक्त्यर्थ) विशेष्यरूप से ही 'चैत्र', 'घट' आदि में (अन्वित होता है)।
षष्ठी विभक्ति के अर्थ ('सम्बन्ध) का, 'तण्डुल' अादि 'नाम' पदों के अर्थ में अन्वय होने के कारण, (उसका) क्रिया में अन्वय न होने से (सम्बन्ध' की 'कारकता' नहीं है)। इसीलिये 'षष्ठी' विभक्ति तथा 'उपपद' विभक्ति के अर्थ (सम्बन्ध) में, उनके क्रिया में अन्वित न होने के कारण, कारकता नहीं है-ऐसा वैयाकरण मानते हैं । 'उपपद' विभक्तियों का भी 'सम्बन्ध' ही अर्थ है । 'चैत्रस्य पचति' इत्यादि (वाक्यों) में 'तण्डुल' आदि पद के अध्याहार से ही अर्थ का ज्ञान होता है । षष्ठी विभक्ति का अर्थ (अर्थात्) 'सम्बन्ध' (तण्डुल आदि) नाम पदों के अर्थ के प्रति ही 'साकांक्ष' रहता है (क्रिया के प्रति नहीं) तथा क्रिया 'कर्म' आदि के प्रति साकांक्ष रहती है ('सम्बन्ध' के प्रति नहीं) । इसलिये सम्बन्ध तथा क्रिया दोनों (एक दूसरे के प्रति) निराकांक्ष हैं।
- क्रियानिमित्तत्वं कारकत्वम्- यहां 'कारकत्व' की एक दूसरी परिभाषा ‘क्रियानिमित्तत्वं कारकत्वम्" पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत की गयी है। इस परिभाषा में 'निमित्त' का अभिप्राय, 'उत्पादक' निमित्त न होकर, 'प्रयोजक' (प्रेरक) निमित्त है। इसलिये 'कारक' की इस परिभाषा को स्वीकार करने पर 'चैत्रस्य तण्डुलं पचति' इत्यादि प्रयोगों के 'चैत्रस्य' जैसे सम्बन्ध अर्थ वाले पदों में भी 'कारकता' की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि अपने चावलों को पकाने के लिये देकर चैत्र पकाने की क्रिया में उसी प्रकार प्रेरक निमित्त है जिस प्रकार 'सम्प्रदान' कारक में वह व्यक्ति दान क्रिया का निमित्त है जिसे कोई वस्तु दी जाती है। इसलिए, जिस प्रकार दान के पात्र 'सम्प्रदान' को 'कारक' माना जाता हैं उसी प्रकार, 'सम्बन्धी' को भी 'कारक' मानना होगा।
क्रियान्वित'''कारकत्वम्-- इस दोष के निराकरण के लिये 'कारक' की अन्य दो परिभाषाएं यहाँ दी गयीं-"क्रियान्वित-विभक्त्यान्वितत्वम् कारकत्वम्" तथा "कियानिर्वकत्वं वा कारकत्वम्"। पहली का अभिप्राय यह है कि क्रिया में अन्वित होने वाले विभक्त्यर्थ (अाख्याता के अर्थ 'कर्तृत्व' या 'कर्मत्व') में जिसका अन्वय हो वह 'कारक' है। तथा दूसरी का अभिप्राय है कि जो क्रिया का निर्वर्तक अर्थात् निष्पादक या जनक हो वह 'कारक' है। पहली परिभाषा के द्वारा, उपरिप्रदर्शित पद्धति से, 'प्रातिपदिकार्थ तथा 'सम्बोधनार्थ' में होने वाली, 'प्रथमा' तथा 'अधिकरण' की और दूसरी परिभाषा से शेष अन्य 'कारकों' की 'कारक' संज्ञा सिद्ध होती है ।
विशेष्यतयैव "चैत्रघटादौ--पहली परिभाषा को स्पष्ट करने के लिये यहां किया तथा 'विभक्त्यर्थ' आदि के गौण-प्रधान-भाव की चर्चा की गयी है। किया का जब 'विभक्त्यर्थ' के साथ अन्वय होता है तब क्रिया का अर्थ प्रधान होता है। परन्तु जब 'विभक्त्यर्थ' का 'चैत्र' आदि शब्दों के साथ अन्वय होता है तब विभक्ति का अर्थ प्रधान
For Private and Personal Use Only