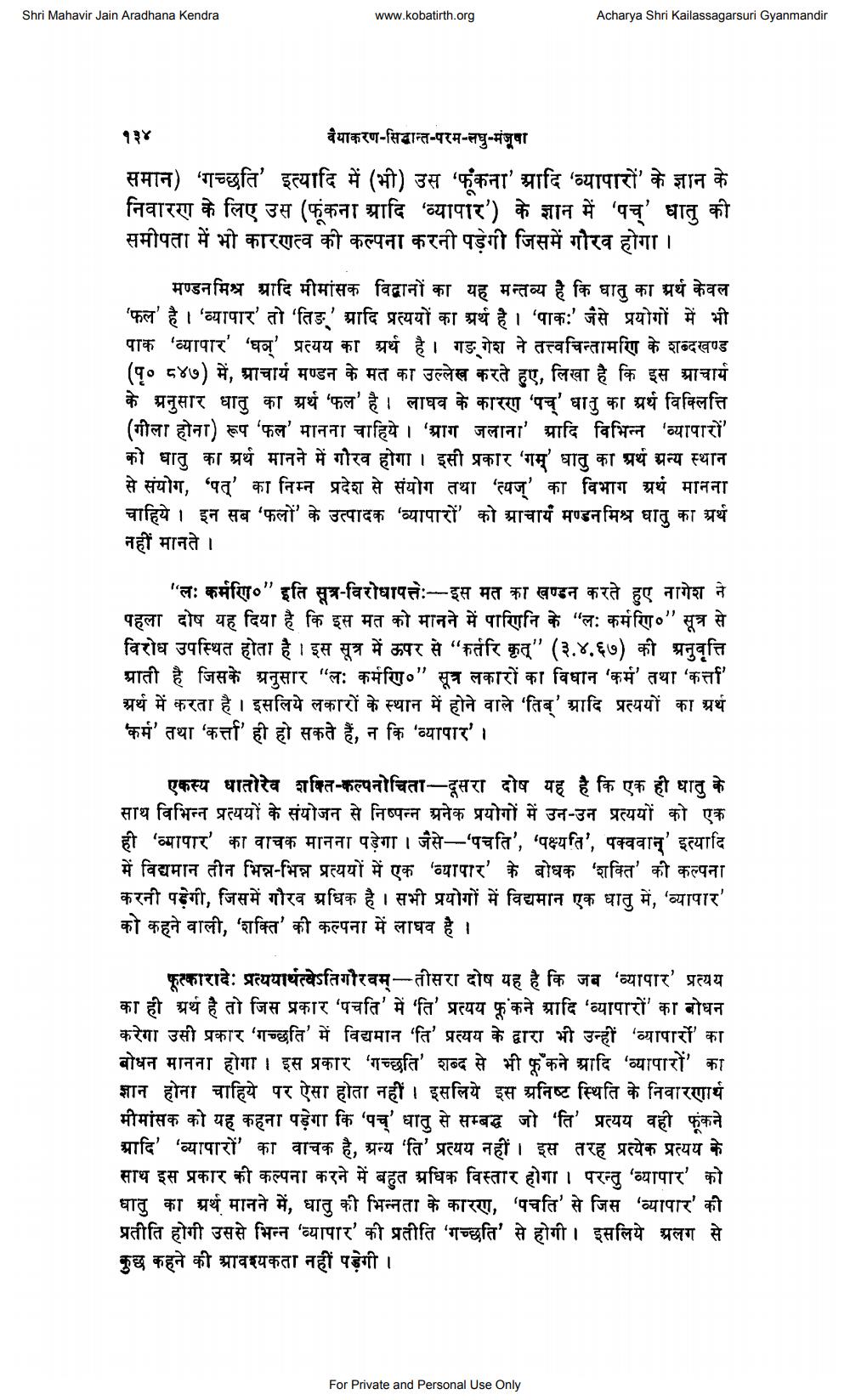________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
१३४
वैयाकरण - सिद्धान्त-परम- लघु-मंजूषा
समान) 'गच्छति' इत्यादि में (भी) उस 'फूंकना ' आदि 'व्यापारों' के ज्ञान के निवारण के लिए उस ( फूंकना आदि 'व्यापार' ) के ज्ञान में 'पच्' धातु की समीपता में भी कारणत्व की कल्पना करनी पड़ेगी जिसमें गौरव होगा ।
मण्डन मिश्र श्रादि मीमांसक विद्वानों का यह मन्तव्य है कि धातु का अर्थ केवल 'फल' है । 'व्यापार' तो 'तिङ' आदि प्रत्ययों का अर्थ है । 'पाक' जैसे प्रयोगों में भी पाक 'व्यापार' 'घन्' प्रत्यय का अर्थ है । गङ्गेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शब्दखण्ड ( पृ० ८४७ ) में, प्राचार्य मण्डन के मत का उल्लेख करते हुए, लिखा है कि इस आचार्य के अनुसार धातु का अर्थ 'फल' है । लाघव के कारण 'पच्' धातु का अर्थ विक्लित्ति ( गीला होना) रूप 'फल' मानना चाहिये । 'आग जलाना' आदि विभिन्न 'व्यापारों' को धातु का अर्थ मानने में गौरव होगा । इसी प्रकार 'गम्' धातु का अर्थ अन्य स्थान से संयोग, 'पत्' का निम्न प्रदेश से संयोग तथा 'त्यज्' का विभाग ग्रथं मानना चाहिये । इन सब 'फलों' के उत्पादक 'व्यापारों को प्राचार्य मण्डन मिश्र धातु का अर्थ नहीं मानते ।
" लः कर्मणि० " इति सूत्र - विरोधापत्तेः - इस मत का खण्डन करते हुए नागेश ने पहला दोष यह दिया है कि इस मत को मानने में पाणिनि के "लः कर्मरिण ०" सूत्र विरोध उपस्थित होता है । इस सूत्र में ऊपर से "कर्तरि कृत्" (३.४.६७) की अनुवृत्ति श्राती है जिसके अनुसार "लः कर्मणि० " सूत्र लकारों का विधान 'कर्म' तथा 'कर्त्ता' अर्थ में करता है । इसलिये लकारों के स्थान में होने वाले 'तिब्' आदि प्रत्ययों का अर्थ 'कर्म' तथा 'कर्ता' ही हो सकते हैं, न कि 'व्यापार' ।
एकस्य धातोरेव शक्ति-कल्पनोचिता- दूसरा दोष यह है कि एक ही धातु के साथ विभिन्न प्रत्ययों के संयोजन से निष्पन्न अनेक प्रयोगों में उन-उन प्रत्ययों को एक ही 'व्यापार' का वाचक मानना पड़ेगा । जैसे— 'पचति', 'पक्ष्यति', पक्ववान्' इत्यादि में विद्यमान तीन भिन्न भिन्न प्रत्ययों में एक 'व्यापार' के बोधक 'शक्ति' की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसमें गौरव अधिक है। सभी प्रयोगों में विद्यमान एक धातु में, 'व्यापार' को कहने वाली, 'शक्ति' की कल्पना में लाघव है ।
फूत्कारादेः प्रत्ययार्थत्वेऽतिगौरवम् - तीसरा दोष यह है कि जब 'व्यापार' प्रत्यय काही अर्थ है तो जिस प्रकार 'पचति' में 'ति' प्रत्यय फूंकने आदि 'व्यापारों' का बोधन करेगा उसी प्रकार 'गच्छति' में विद्यमान 'ति' प्रत्यय के द्वारा भी उन्हीं 'व्यापारों' का बोधन मानना होगा । इस प्रकार 'गच्छति' शब्द से भी फूंकने आदि 'व्यापारों' का ज्ञान होना चाहिये पर ऐसा होता नहीं । इसलिये इस अनिष्ट स्थिति के निवारणार्थ मीमांसक को यह कहना पड़ेगा कि 'पच्' धातु से सम्बद्ध जो 'ति' प्रत्यय वही फूंकने आदि' 'व्यापारों' का वाचक है, अन्य 'ति' प्रत्यय नहीं । इस तरह प्रत्येक प्रत्यय के साथ इस प्रकार की कल्पना करने में बहुत अधिक विस्तार होगा । परन्तु 'व्यापार' को धातु का अर्थ मानने में, धातु की भिन्नता के कारण, 'पचति' से जिस 'व्यापार' की प्रतीति होगी उससे भिन्न 'व्यापार' की प्रतीति 'गच्छति' से होगी । इसलिये अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।
For Private and Personal Use Only