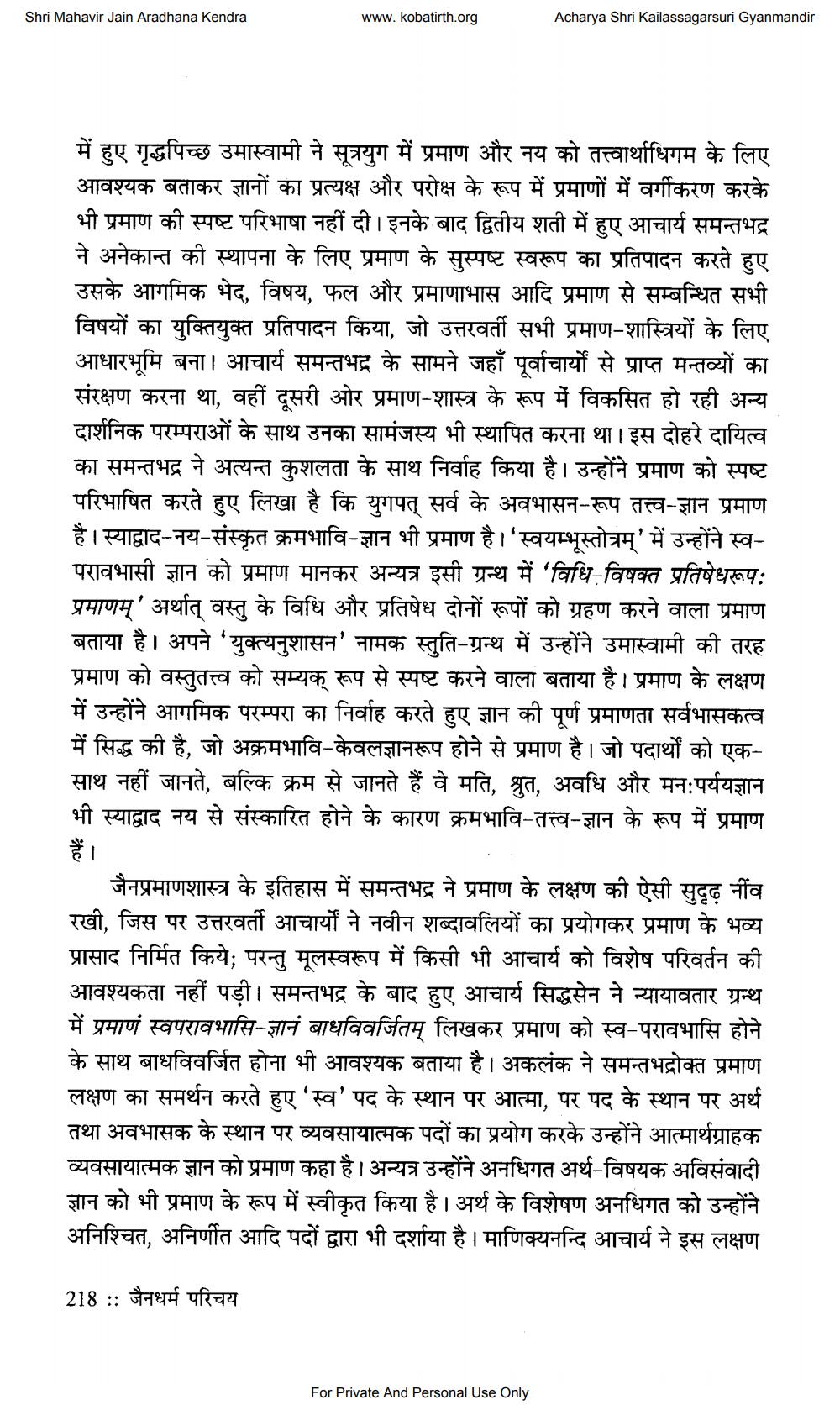________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
में हुए गृद्धपिच्छ उमास्वामी ने सूत्रयुग में प्रमाण और नय को तत्त्वार्थाधिगम के लिए आवश्यक बताकर ज्ञानों का प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में प्रमाणों में वर्गीकरण करके भी प्रमाण की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। इनके बाद द्वितीय शती में हुए आचार्य समन्तभद्र ने अनेकान्त की स्थापना के लिए प्रमाण के सुस्पष्ट स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए उसके आगमिक भेद, विषय, फल और प्रमाणाभास आदि प्रमाण से सम्बन्धित सभी विषयों का युक्तियुक्त प्रतिपादन किया, जो उत्तरवर्ती सभी प्रमाण-शास्त्रियों के लिए आधारभूमि बना। आचार्य समन्तभद्र के सामने जहाँ पूर्वाचार्यों से प्राप्त मन्तव्यों का संरक्षण करना था, वहीं दूसरी ओर प्रमाण-शास्त्र के रूप में विकसित हो रही अन्य दार्शनिक परम्पराओं के साथ उनका सामंजस्य भी स्थापित करना था। इस दोहरे दायित्व का समन्तभद्र ने अत्यन्त कुशलता के साथ निर्वाह किया है। उन्होंने प्रमाण को स्पष्ट परिभाषित करते हुए लिखा है कि युगपत् सर्व के अवभासन-रूप तत्त्व-ज्ञान प्रमाण है। स्याद्वाद-नय-संस्कृत क्रमभावि-ज्ञान भी प्रमाण है। 'स्वयम्भूस्तोत्रम्' में उन्होंने स्वपरावभासी ज्ञान को प्रमाण मानकर अन्यत्र इसी ग्रन्थ में 'विधि-विषक्त प्रतिषेधरूपः प्रमाणम्' अर्थात् वस्तु के विधि और प्रतिषेध दोनों रूपों को ग्रहण करने वाला प्रमाण बताया है। अपने ‘युक्त्यनुशासन' नामक स्तुति-ग्रन्थ में उन्होंने उमास्वामी की तरह प्रमाण को वस्तुतत्त्व को सम्यक् रूप से स्पष्ट करने वाला बताया है। प्रमाण के लक्षण में उन्होंने आगमिक परम्परा का निर्वाह करते हुए ज्ञान की पूर्ण प्रमाणता सर्वभासकत्व में सिद्ध की है, जो अक्रमभावि-केवलज्ञानरूप होने से प्रमाण है। जो पदार्थों को एकसाथ नहीं जानते, बल्कि क्रम से जानते हैं वे मति, श्रुत, अवधि और मन:पर्ययज्ञान भी स्याद्वाद नय से संस्कारित होने के कारण क्रमभावि-तत्त्व-ज्ञान के रूप में प्रमाण
__ जैनप्रमाणशास्त्र के इतिहास में समन्तभद्र ने प्रमाण के लक्षण की ऐसी सुदृढ़ नींव रखी, जिस पर उत्तरवर्ती आचार्यों ने नवीन शब्दावलियों का प्रयोगकर प्रमाण के भव्य प्रासाद निर्मित किये; परन्तु मूलस्वरूप में किसी भी आचार्य को विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। समन्तभद्र के बाद हुए आचार्य सिद्धसेन ने न्यायावतार ग्रन्थ में प्रमाणं स्वपरावभासि-ज्ञानं बाधविवर्जितम् लिखकर प्रमाण को स्व-परावभासि होने के साथ बाधविवर्जित होना भी आवश्यक बताया है। अकलंक ने समन्तभद्रोक्त प्रमाण लक्षण का समर्थन करते हुए 'स्व' पद के स्थान पर आत्मा, पर पद के स्थान पर अर्थ तथा अवभासक के स्थान पर व्यवसायात्मक पदों का प्रयोग करके उन्होंने आत्मार्थग्राहक व्यवसायात्मक ज्ञान को प्रमाण कहा है। अन्यत्र उन्होंने अनधिगत अर्थ-विषयक अविसंवादी ज्ञान को भी प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया है। अर्थ के विशेषण अनधिगत को उन्होंने अनिश्चित, अनिर्णीत आदि पदों द्वारा भी दर्शाया है। माणिक्यनन्दि आचार्य ने इस लक्षण
218 :: जैनधर्म परिचय
For Private And Personal Use Only